भास का अनुकीर्तन: कावालम नारायण पणिक्कर से संगीता गुन्देचा की बातचीत
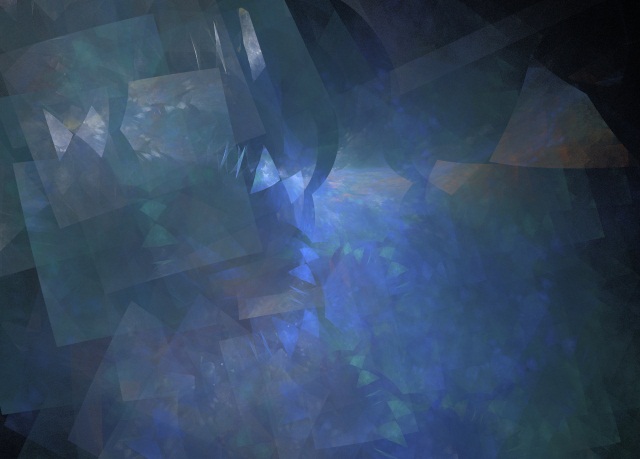
केरल के सुविख्यात रंगनिर्देशक कावालम नारायण पणिक्कर संस्कृत के शास्त्रीय रंगमंच पर वर्षों से एक केन्द्रीय उपस्थिति रहे हैं. श्री पणिक्कर की अधिकांश रंगशिक्षा केरल के पारम्परिक परिवेश और वहाँ की कुडियाट्टम् जैसी पारम्परिक रंगशैलियों के मध्य हुई. पणिक्कर की नाट प्रस्तुतियों में संस्कृत रंगमंच की सदियों पुरानी परम्परा मानो हम तक अटूट चली आयी हो. वे भास के रूपकों के मंचन के लिए विख्यात हैं. यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि समकालीन विश्व में भास के रूपकों को पुर्नप्रतिष्ठित करने में पणिक्कर ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है. वे केरल के तिरूवनन्तपुरम् में स्थित ‘सोपानम् रंगमण्डली के निर्देशक हैं और विभिन्न भारतीय तथा विदेशी नाटकों का संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेज़ी तथा मलयाली भाषा में मंचन करने में सिद्धहस्त हैं. पणिक्कर मलयालम् भाषा के जाने माने कवि और नाट लेखक भी हैं और पारम्परिक नाटकलाओं के मशहूर गुरू भी . यह संवाद भास-रंगकर्म विशेषज्ञ पणिक्कर से यह जानने-समझने के लिए किया गया कि आदि-नाटकार भास को एक पारम्परिक रंगकर्मी किन रंगयुक्तियों, रंगकल्पनाओं के सहारे बीसवीं सदी में अपने रंगकर्म में सम्भव करता है.
संगीता गुन्देचा
आपने नाटक के क्षेत्र में निश्चय ही अनेक नवाचार किये हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ में आप पारम्परिक नाटकर्मी हैं. महाकवि भास, कालिदास आदि के नाटकों के प्रदर्शन के लिए आपने पारम्परिक नाटशैली का ही चुनाव क्यों किया? आपने इसके लिए मसलन तथाकथित यथार्थवादी शैली को क्यों नहीं चुना?
पणिक्कर
यह बेहद महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि आखिर कार कोई भी अपनी परम्परा से कैसे भाग सकता है, न सिर्फ़ भास या कालिदस जैसे नाटकारों के नाटकों को करने के सन्दर्भ में बल्कि रोज़मर्रा के जीवन में भी. जैसे ही आप अपने आप से या अपने परिवेश, अपनी अन्तश्चेतना से पराये हो जाते हैं, आप अपने साथ न्याय नहीं कर पाते, आप अपने को समझा नहीं पाते, अपनी व्याख्या नहीं कर पाते. भास या कालिदास जैसे महान् नाटकार आपको अपनी परम्परा को समझने व अपने समय के अनुरूप उसकी पुनर्व्याख्या करने का अवसर देते हैं. हमें यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि हम परम्परा को जड़ वस्तु या अचल नहीं कह सकते. आज परम्परा वही नहीं है जो दो हज़ार साल पहले या सौ बरस पहले न सिर्फ़ थी बल्कि उपयुक्त थी. आप परम्परा को इस तरह सीमित नहीं कर सकते इसीलिए वह परम्परा है. परम्परा शब्द में ही एक नैरन्तर्य का आशय है. बीते हुए कल की विरासत को हम आज परम्परा के नैरन्तर्य के रूप में पाते हैं क्योंकि काल एक निरन्तर प्रवाह है. आप बता रही थीं कि आधुनिक नृत्यकार सुश्री चन्द्रलेखा ने ‘आदिशेष’ नृत्य संयोजन तैयार किया है, उस अवधारणा में ही एक किस्म के नैरन्तर्य का आशय है. संस्कृति इसके अलावा हो ही नहीं सकती, आप समूची संस्कृति की किसी एक जगह पर इतिश्री कर बिल्कुल नयी शुरूआत करने की सोच भी नहीं सकते. कोई देश या कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? यह एक अलग बात है कि यथार्थवादी शैली हमारी अपनी नहीं है. हमारा यथार्थवाद भी पश्चिम के यथार्थवाद से भिन्न है, जीवन अलग है, जीवन के प्रति हमारा रूख अलग है इसलिए हर जगह हमें यह फ़र्क दर्शाना ही होगा. यही नहीं व्यापक भारतीय परिवेश के भीतर भी केरलीय परिवेश या मालवी परिवेश में अन्तर है, एक ही सांस्कृतिक इकाई के अन्दर भी अलग-अलग जगहों में अन्तर मौजूद है. जैसे भाषा में फ़र्क है और यही नहीं जीवन के लगभग सभी पहलुओं में यह फ़र्क मौजूद है. आप उस तरह से हिन्दी नही बोलतीं जैसे मसलन कोई लखनवी व्यक्ति बोलेगा. यह फ़र्क दरअसल जीवन का वैविध्य है.
संगीता गुन्देचा
क्या आपको पश्चिमी यथार्थवाद किन्ही मायनों में सीमित नज़र आता है?
पणिक्कर
पश्चिमी यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के बीच अन्तर सम्बन्ध है. हमें प्रकृति की नकल करने की हद तक नहीं जाना चहिए, पश्चिम की नकल का तो सवाल ही नहीं उठता, भले ही वह यथार्थवाद या प्रकृतिवाद के नाम पर क्यूँ नहीं की जाये. हमारी सृजनात्मकता में ईश्वर तक की नकल नहीं की जाती. ईश्वर की सृष्टि पहले से ही हमारी आँखों के सामने है, हमें उसकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है. आप पर्वत की नकल कर भी कैसे सकते हैं? अपनी सम्पूर्णता में और अपने सारे गुणों के साथ एक पर्वत आप बना ही कैसे सकते हैं? इसलिए अगर एक कलाकार पर्वत का सृजन करना भी चाहे तो वह कैसे करेगा? क्या यह यथार्थवाद के सहारे मुमकिन है?
संगीता गुन्देचा
यहाँ मुझे महान् कुडियाट्टम् नर्तक इट्टियम्मां चाक्यार के जीवन की एक घटना याद आ रही है. वे एक सुबह घूमने निकले. सामने से एक अंग्रेज़़ अफ़सर अपना कुत्ता लिए चला आ रहा था. इट्टियम्मां चाक्यार को देखते ही वह कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा, इस पर उन्होंने उसकी ओर एक पत्थर फेंका जिससे कुत्ता गिर पड़ा. जब अंग्रेज़ ने इस पर नाराज़गी ज़ाहिर की, इट्टियम्मां चाक्यार बोले कि उन्होंने पत्थर नहीं मारा, पत्थर मारने का अभिनय भर किया था, फिर उन्होंने वैसा ही एक पत्थर अंग्रेज़ की ओर फेंका और उसे चौंकता देख बोले कि मैं पहाड़ भी उठा सकता हूँ और उन्होंने पहाड़ उठाने का ऐसा अभिनय किया कि अंग्रेज़ को लगा यह पहाड़ कहीं उस पर न गिर पड़े और वह भाग गया.
पणिक्कर
यह अच्छा दृष्टान्त है और मेरी समझ में यह यथार्थ के प्रति हम भारतीयों के दृष्टिकोण की अच्छी व्याख्या है. यह कुडियाट्टम् के लिए ही नहीं किसी भी ऐसे भारतीय कलारूप के लिए सही है जो नाट्यधर्मी है. और जहाँ तक लोकधर्मी और नाट्यधर्मी का प्रश्न है, उनमें डिग्री का फ़र्क है, लोकधर्मी में भी नाट्यधर्मी के गुण होते हैं और नाट्यधर्मी में लोकधर्मी के. मैं आपको बता रहा था कि यथार्थवाद भ्रम पैदा करता है. यथार्थवाद में आप कला को यथार्थ की तरह निर्मित करने की कोशिश करते हैं. यह करने के अपने प्रयास में आपको ठीक-ठीक पता होता है कि आप जिस यथार्थ की नकल करने की कोशिश में लगे हैं वैसा कुछ आप कर ही नहीं सकते इसलिए आप जिन लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपने यथार्थ जैसा कुछ निर्मित कर दिया है, उनके सामने आप भ्रम खड़ा करते हैं. आप यथार्थ की नकल करते हुए यह जानते हैं कि यह कोशिश अनिवार्यतः विफल होने वाली है. यथार्थवाद में यह मुश्किल या विडम्बना अन्तर्भूत है. लेकिन अगर आप इस परम्परा में यथार्थ को ज्यूँ का त्यूँ नहीं दर्शाना चाहते तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आप अतियथार्थवादी हो जाएँ. इसलिए वे टेलीफ़ोन दिखाने के लिए एक सामान्य आकार के टेलिफ़ोन को दिखाने की जगह एक बहुत बड़ा टेलिफ़ोन रख देंगे. इसके बरक्स भारतीय नाट्यदृष्टि को स्पष्ट करने मैं एक बार फिर पहाड़ का उदाहरण दूँगा. अगर आप पश्चिम की यथार्थवादी शैली में पहाड़ का एक चित्र बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ बनाएँगे जो बिल्कुल पहाड़ जैसा लगता हो, भले ही वह उसका लघु रूप हो और यह प्रयास निश्चय ही विफल होने वाला है क्योंकि यथार्थवादी ढंग से एक पहाड़ की पुर्नरचना करने की कोशिश करते हुए आप उस पहाड़ के कुछ तत्वों को जैसे वे हैं ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे, भले ही संक्षिप्त रूप में. यानि आप ठीक उन्हीं अवयवों का उपयोग अपनी इस पुर्नरचना के लिए करेंगे जो पहाड़ में पहले से मौजूद हैं. लेकिन यदि आप गैर-यथार्थवादी ढंग से यह करने की कोशिश कर रहे हैं तब पहाड़ दर्शाने के लिए आप किन्हीं दूसरे ही तत्वों का उपयोग करेंगे, आप अपने शरीर का पहाड़ की तरह उपयोग करेंगे. आप पहाड़ की ओर देखते हुए-से दर्शकों को यह बता देंगे कि यह रहा पहाड़, आप पहाड़ के बारे में बताते हुए उसके आन्तरिक लक्षणों को व्यक्त कर पहाड़ को दर्शकों के सामने साकार कर देंगे. बल्कि इन आन्तरिक लक्षणों को दर्शाते हुए आप स्वयं उन्हें धारण कर लेंगे और खुद पहाड़ हो जाएँगे, क्योंकि आन्तरिक लक्षण ही अधिक महत्त्व के होते है. मसलन मैं आपको संगीता की तरह इसलिए पहचान लेता हूँ क्योंकि आपकी एक तरह की छाया है, आप अपने पिता की तरह लगती हों या कुछ और, यह सब तो है, लेकिन इसके परे आपका एक विशेष आध्यात्मिक आयाम है, जो आपके भीतर उपस्थित है. आपके गुण जैसे आपको लोगों से स्नेह है और इसी तरह के तमाम दूसरे गुण, ये सब मिलकर आपका एक आन्तरिक व्यक्तित्त्व बनाते हैं, उसे ही अवस्था कहा जाता है, वह संगीता अवस्था है और वह केवल बाहरी गुणों से निर्धारित नहीं होती. हर व्यक्ति बल्कि हर विचार का एक आन्तरिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है, यह निर्जीव वस्तुओं तक के लिए सही है. इसलिए पहाड़ का अनुकरण करते समय आप पहाड़ के बाहरी गुणों का अनुकरण नहीं करते, आप पहाड़ के आन्तरिक यथार्थ को जानने की कोशिश करते हैं. यह प्रक्रिया विशेषकर नृत्य और नाट में आपके शरीर के माध्यम से ही सम्पन्न होती है. यहाँ आपके शरीर के अलावा और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता. इसी के सहारे आप सबसे अधिक शिद्दत से पहाड़ के पहाड़पन को सम्प्रेषित कर सकते हैं, समुद्र के समुद्रपन को, किसी विचार के विचारपन को, इसे ही अवस्था कहते हैं.
संगीता गुन्देचा
शायद इसी अर्थ में शरीर अपने आप में समूचा ब्रह्माण्ड है ?
पणिक्कर
हाँ और इसी अर्थ में ‘अवस्थानुकृतिर्नाट्यम् एक गहन और विशिष्ट सूत्र है. यहाँ वस्तु की अनुकृति आशय नहीं है, वस्तु की अवस्था की अनुकृति आशय है.
संगीता गुन्देचा
अनुकृति या अनुकीर्तन?
पणिक्कर
अवस्थानुकृति विकसित होकर अवस्थानुकीर्तन को प्राप्त होती है. अनुकीर्तन अनुकृति के बाद होता है. अनुकृति महज अवस्था को दर्शाती है जिसमें आप वस्तु के आन्तरिक सत्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लोकधर्मी स्तर पर अवस्था का सृजन करने का. लेकिन जब आप इसका विस्तार करते हैं, जब आप अवस्था के विचार का उत्सव मनाते हैं, पहाड़ के सत्त्व को जानने की प्रक्रिया में डूबते है, उसका आनन्द लेते हैं, तब वहाँ एक नया नाट्यधर्मी आयाम प्रकट होता है, जिसे अनुकीर्तन के नाम से जाना जाता है.
संगीता गुन्देचा
आपने भास के कौन-कौन से नाटकों का मंचन किया है ?
पणिक्कर
मैंने उन तेरह नाटकों से, जो भास के बताये जाते हैं, सात का मंचन किया है, जिनमें सबसे बाद में प्रतिमानाटकम् किया है. हम यह ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि ये सारे नाटक भास के ही लिखे हैं, खासकर उन सात नाटकों के अलावा जो मैंने किये हैं.
संगीता गुन्देचा
ये सात नाटक कौन-से हैं?
पणिक्कर
मध्यमव्यायोग, उरूभंगम्, दूतवाक्यम, कर्णभारम्, स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिमानाटकम् और प्रतिज्ञायौगन्धरायण . भास के ये सभी नाटक मैंने किये हैं. अब हम पंचरात्रम् करने के बारे में सोच रहे हैं. इन सभी नाटकों को करते हुए मैंने यह पाया कि भास निश्चय ही भरत की कई अवधारणाओं को नकारते हैं लेकिन उन्होंने उस परम्परा को निश्चय ही समृद्ध किया है जो भरत से शुरू होकर आगे तक चली आती है. भरत के विषय में यह कहना मुश्किल है कि इस नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं. हो सकता है कि कई सारे भरत रहे हों. हो सकता है विभिन्न नटसूत्रों को कभी बाद में संकलित किया गया हो, जिसे आज हम नाट्यशास्त्र के रूप में जानते हैं. जहाँ तक भास का प्रश्न है, वे एक ऋषि हैं क्योंकि वे अपने नाटकों के माध्यम से स्वयं को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, कालिदास तक ने अपने नाटक के माध्यम से अपने नाम को प्रोजेक्ट किया है. आप उज्जैन जैसी जगह पर आकर कालिदास की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं. कल जब मैंने कालिदास समारोह में विक्रमोर्वशीयम् की अपनी प्रस्तुति में छह ऋतुओं को ऋतुसंहार के सहारे प्रस्तुत किया तो कृष्णकान्त चतुर्वेदी बोले कि ऋतुसंहार के बारे में अब तक निश्चित नहीं है कि वह कालिदास की कृति है. लेकिन उन्हें लगा कि मेरी इस प्रस्तुति के बाद अब यह संशय नहीं होना चाहिए. कालिदास की बात भास से भिन्न है. ये दो प्रमुख धाराएँ हैं, यह सच है कि हम इसमें विशाखदत्त के मुद्राराक्षस को भी शामिल कर सकते हैं.
संगीता गुन्देचा
क्या हम यह कह सकते है कि भरत के नाट्यशास्त्र के स्रोतों में भास के नाटक भी रहे होंगे ?
पणिक्कर
यह कहना मुश्किल है. मुझे यह लगता ज़रूर है कि भास, भरत के पहले रहे होंगे. इसका कारण मेरा यह विश्वास है जो मुझे उनके नाटकों को पढ़ने के दौरान हुआ कि वे एक ऐसे युग के लेखक रहे हैं, जहाँ वे कर्ण जैसे आद्यरूपात्मक (आर्किटिपिकल) चरित्र को गढ़ सके. भास के चरित्र आद्यरूपात्मक ही नहीं लगभग आदिवासी हैं. यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनके नाटकों में घटोत्कच, हिडिम्बा जैसे चरित्र हैं बल्कि यह आद्यरूपात्मकता (आर्किटिपिकलनेस) उनके नाटकों की रंगसम्भावना के आधार पर लक्ष्य की जा सकती है. जैसे कर्णभारम् में कर्ण कवच और कुण्डल जैसी आवश्यक और प्रिय वस्तुएँ अपने शरीर से काटकर शत्रु को दे देता है. यहाँ इस समस्या को किसी भी यथार्थवादी ढंग से नहीं देखा गया है. ऐसा कोई भी नहीं करेगा, भले ही आप उसे दानवीर की उपाधि क्यूँ न दे दें. मैं सोचता हूँ कि इन चीज़ों को देने का निर्णय करने के लिए कर्ण एक ऊँचाई तक पहुँचता है, इस दृश्य को भास ने बहुत ही नाटकीय ढंग से रचा है. इसलिए दान के इस दृश्य को दिखाया ही नहीं जा सकता बगैर इसे ‘पजे़ज़्ड डांस’ से जोड़े, आदिवासियों के ‘पजे़ज़्ड’ डांस से जोड़े बगैर. यह मेरी विनम्र भावना है.
संगीता गुन्देचा
आदिवासियों के इस नृत्य में क्या होता है ?
पणिक्कर
आप पर होल आता है. जैसे आप में प्रेतात्मा का प्रवेश हो गया हो. जैसे आप पर कोई काबिज़ हो गया हो. यह एक अनुष्ठान जैसा है लेकिन इसका अभिनय आप तभी कर सकते हैं जब आप उस अनुष्ठान पर आस्था रखते हों. मैंने ऐसा एक आदिवासी देखा है, उस पर कविता भी लिखी है. मैं उससे मिलने जंगल के भीतर गया था. वह आदिवासी इस तरह जीता था जैसे वह अपने इष्टदेवता का जीवन जी रहा हो, जैसे उसे उस इष्टदेव ने धारण कर रखा हो. वह अपने उस इष्टदेव को पंचरली कहता था. पंचरली भले ही उसका इष्टदेव हो लेकिन वह उसकी भूमिका में रहता था. उसे लगता कि वह खुद पंचरली है. यह सम्भव है कि वह दौड़कर पास की ताड़ी की दुकान से जाकर कुछ पी आता हो ताकि वह अपने अहंकार को पार्श्व में धकेलकर अपने इष्ट पंचरली को सामने आने दे सके. यह बिल्कुल सम्भव है कि उसके इस व्यवहार का एक सबब ताड़ी हो, लेकिन इसके साथ उसका अपना विश्वास भी इसका बड़ा कारण है. एक बार वह सुपारी काटते वक्त मुझसे बोला कि क्या मैं यह देखना चाहता हूँ कि उसका इष्टदेव अनश्वर है, कि वह कभी नहीं मर सकता. उसने यह अपनी भाषा में कहा, जो तुलु और मलयालम् का एक क़िस्म का सम्मिश्रण है. मुझे यह दिखाने की कोशिश में वह अपना गला काटने ही वाला था कि तभी हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे वासुदेवन ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि तब कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस आदिवासी को इसकी परवाह नहीं थी. आखिर वह निरक्षर था, प्राकृत था, जैसा कि हमारे आलोचकों में से एक की मेरे बारे में राय है: यह प्राकृत है. क्योंकि मैं इस किस्म के आद्यरूपात्मक चरित्रों को अपने रंगकर्म में ला रहा था. इसी सन्दर्भ में मैं आपसे कर्ण के ‘पजे़ज़्ड डांस’ की बात कर रहा था जिसमें अभिनेता को इतना ‘पजे़ज़्ड’ हो सकना चाहिए कि वह स्वयं को भूल जाये. ऐसा करना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि वह अपने जीवनदान के लिए तैयार हो जाये जैसा कर्णभारम् में कर्ण होता है. कर्ण वेदव्यास का चरित्र है लेकिन भास ने इसी चरित्र का उपयोग एक खास तरह से किया है. वे उसे इस तरह निर्मित करते हैं जहाँ वह एक के बाद एक इतना सब दान करने के लिए तैयार हो जाता है. इसे केवल ‘पजे़ज़्ड’ होकर ही किया जा सकता है और यह अत्यन्त आद्यरूपात्मक है, बल्कि आदिवासियों का-सा है. यह करना अभिनेता के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे इस तरह ‘पजे़ज़्ड’ नहीं होना है जैसा आदिवासी अनुष्ठानों में होता है. मेरे एक अभिनेता ने यह करने का प्रतिरोध किया था क्योंकि उसे लगा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है. उसे यह लगा कि वह एक आदिवासी की तरह किसी प्रेत को खुद में कैसे प्रवेश दे सकता है क्योंकि वह तो आदिवासी है नहीं. दरअसल वह गलत समझ रहा था. इस नाटक के मंचन में कर्ण की भूमिका निभाते हुए ‘पजे़ज़्ड’ होना एक रंगयुक्ति है, मंचन की युक्ति, जिसे अभिनेता को महसूस करते हुए, उस पर भरोसा करना होता है. उसे अपनी मानसिकता में स्थान देना होता है. अपनी मानसिकता में इस तरह की युक्ति को स्थान देने का प्रयत्न करना ही अभिनेता के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए मेरा वह अभिनेता ‘पजे़ज़्ड’ होकर कर्ण का अभिनय करने से कतरा रहा था. ऐसा करने के लिए अभिनेता का स्वयं अपनी तमाम संवेदनाओं पर नियन्त्रण होना आवश्यक है. ऐसा अभिनय वही कर सकता है, जो इस सब को ग्रहण कर उसे व्यक्त कर सके. इसलिए जिस अभिनेता ने ‘पजे़ज़्ड’ होकर अभिनय करने से इन्कार किया था, शायद उसके पुराने अनुभव ऐसे रहे हों जिनके कारण वह न इसे अनुभव कर पा रहा था और न इस पर भरोसा. मैंने उससे कहा कि भास कर्ण की व्याख्या करते हुए उसे एक ऐसी क्रमिक अवस्था तक ले जाते हैं जहाँ वह पूरी तरह ‘पजे़ज़्ड होकर एक झटके से अपने कवच कुण्डल काटकर ब्राह्मण का रूप धरे इन्द्र को दान कर देता है. भास ने कर्ण के चरित्र को इसी तरह गढ़ा है.
संगीता गुन्देचा
आपकी विशेषताओं में भास के नाटकों के मंचन का विषेष उल्लेख होता है. आप ने दूसरे नाटक भी किये हैं लेकिन जब भी भास के नाटकों के मंचन की बात होती है तो कावलम नारायण पणिक्कर का नाम आता है. आपकी रंगशिक्षा में ऐसे कौन-से तत्व रहे हैं जिनके कारण आप भास के नाटकों के मंचन की ओर मुड़ सके ?
पणिक्कर
ऐसी कोई रंगशिक्षा हुई ही नहीं. शिक्षा के नाम पर सिर्फ़ इतना हुआ कि मैं संगीत का अभ्यास करता था, कविताएँ लिखता था और गाँव में रहता था. हमारे गुरू खेतों में काम करते थे, गाते थे. वे सभी निरक्षर थे. कम से कम पश्चिमी शिक्षा की दृष्टि से. वे निरक्षर भले ही रहे हों पर थे सुसंस्कृत. शुरूआत में मैं इन्हीं लोगों से सीखता रहा फिर धीरे-धीरे मैं रंगमंच की ओर मुड़ा. वे सारी छवियाँ, वे सारे अनुभव मेरे साथ थे, जो मुझे गाँव में रहते हुए हासिल हुए थे. मैं रंगमंच के क्षेत्र में देर से आया, जिसका आशय यह है कि साठ के दशक में मैंने रंगमंच में काम करना शुरू किया. एक तरह से मेरी शिक्षा लोकसंगीत में हुई, जो मैंने सीखा नहीं, जो खुद मुझ तक आया, क्योंकि वह मेरे चारों तरफ था, खेतों में तरह-तरह के काम करते लोगों के गानों में और इसी तरह दूसरे ग्रामीण कार्यकलापों में.
संगीता गुन्देचा
क्या उन दिनों आपने भास के नाटक पढ़े थे ?
पणिक्कर
नहीं. यह बहुत बाद में हुआ. हमारी संस्कृत शिक्षा कुछ अलग क़िस्म की हुई है. उन दिनों गाँव के ज्योतिषी संस्कृत पढ़ाया करते थे. वे कणियन् जाति के होते थे. यह जाति वर्ण व्यवस्था में अपेक्षाकृत निचली जाति की होती है. ये लोग संस्कृत के अध्येता होते थे. वे नक्षत्रों को पढ़ सकते थे और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, गायक भी होते थे. मेरे गुरू उसी समुदाय के थे. उन्होंने ही मुझे संस्कृत के आरम्भिक ग्रन्थों का ज्ञान कराया. उन दिनों शिक्षा का अर्थ ही अंग्रेज़ी शिक्षा होता था, इसलिए हमारे अभिभावकों ने हमें ऐसे स्कूलों में भेजा जहाँ केवल अंग्रेज़ी शिक्षा होती थी, जहाँ मलयालम् भी दूसरी भाषा थी. सारा कुछ अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ाया जाता था.
संगीता गुन्देचा
आप अपनी आरम्भिक रंगशिक्षा से जुड़ी कोई महत्त्वपूर्ण घटना याद करना चाहेंगे ?
पणिक्कर
हमारे घर के पास धान की खेती होती थी. हमारा घर ऐसी जगह था जहाँ पानी भरा रहता था. हम वहीं खेती किया करते थे और कई बार कुछ हवा में तैरता हुआ-सा करीब आता था. एक बार मैं इस संगीत के स्रोत की खोज में निकल पड़ा और मैंने पाया कि एक झोपड़ी में एक व्यक्ति बाँसुरी बजा रहा है. वह खेतिहर मज़दूर था. मैंने उन्हे अपना गुरू बना लिया और उन्होंने मुझे एक बाँसुरी दी और वह भी मुफ़्त में. उन्होंने ही मुझे यह सिखाया कि बाँसुरी पर अँगुलियाँ कहाँ रखी जाती हैं और इस तरह मेरा सीखना शुरू हुआ.
संगीता गुन्देचा
आपने भास के नाटक प्रतिमानाटकम् नाटक को करते हुए प्रतिमा शब्द में एक नया आशय देखा है. क्या आप उस बारे में कुछ बताएँगे ?
पणिक्कर
प्रतिमानाटकम् मैंने अभी हाल ही में किया है. यह नाटक मेरे मन में बहुत दिनों से था. सोचता यह भी रहा हूँ कि भास ने यह नाम क्यों दिया है! मैंने इसे रंगमंच से जोड़कर समझने की कोशिश की. उस एक वाक्य ने मुझे बहुत बेचैन किया, जिसका भास ने अपने इस नाटक में उपयोग किया है, वह वाक्य हैः ‘कंचुकीयो यवनिकास्तरणं करोति’ जिसका अर्थ है: कंचुकी का मृतक के चेहरे पर आवरण डालना. मैं इस अर्थ की उपेक्षा करना चाहता था क्योंकि मुझे मृतक के चेहरे को ढँकने का विचार पसन्द नहीं आया, जो खासा यथार्थवादी विचार है. मैं इस वाक्य के यथार्थवादी आशय से अधिक जानना चाह रहा था. मैं इसे दशरथ के यवनिका में गायब हो जाने की तरह व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा था. किसी ने कहा आप ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि ‘अस्तरणं’ का अर्थ विशेषरूप से मृतक के चेहरे को ढँकने के लिए ही है. मैंने कहा क्यूँ नहीं, इसका अर्थ पर्दा क्यूँ नहीं हो सकता! मैंने सोचा कि पण्डित लोग जो भी कहें मैं पर्दे का इस्तेमाल इस तरह करूँगा कि उसमें दशरथ गायब हो सकें और इस तरह उनकी मृत्यु मंचित हो. यह मेरा, इस नाटक की रंगयोजना के सन्दर्भ में, पहला निर्णय था.
जब मैंने दोबारा भास के इस नाटक में प्रवेश किया तो मेरा फिर एक नये विचार से सामना हुआ. यह विचार इस नाटक में ‘प्रतिमा’ का है. मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं था कि भास ने इस नाटक का नाम प्रतिमानाटकम् सिर्फ़ इसलिए रखा होगा कि इसमें जिस जगह भरत अपने ननिहाल से वापस अपने पिता के घर लौट रहे हैं, वे एक ऐसे प्रतिमागृह में अपने पिता दशरथ की प्रतिमा देखते हैं जहाँ सिर्फ़ मृतकों की प्रतिमाएँ ही प्रदर्शित की गयी हैं. मेरी समझ में प्रतिमानाटक में प्रतिमा का सिर्फ़ इतना-सा अर्थ होना मुमकिन नहीं था. भास के प्रति मेरी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए यह काफ़ी नहीं था. इस नाटक में प्रतिमा के विचार के आशयों को टटोलते हुए मुझे लगा कि नाटक में जिस जगह भरत राम की पादुकाएँ लेकर वापस लौटते हैं, वहाँ से मुझे इस नाटक का साथ छोड़ देना चाहिए. यह नहीं कि मैंने ऐसा कोई निष्कर्ष निकाल लिया था कि नाटक में बाद का यह हिस्सा किसी और ने, मसलन चाक्यारों ने, जोड़ा हो. मैंने यह तय किया कि मैं इस नाटक में प्रतिमा के बिम्ब को अपने मंचन के केन्द्र में रखकर नाटक की परिकल्पना करूँगा और मुझे लगा कि स्वयं भास इसकी इजाज़त देते हैं. इसके लिए मुझे एक पाठेतर-पाठ की आवश्यकता थी, जो मेरी इस विचार -प्रक्रिया को उसकी परिणति तक पहुँचा सके. ऐसा पाठेतर-पाठ मुझे तुरन्त मूल रामायण में मिल गया, जिससे मुझे भास की नाटक की परिकल्पना और योजना को ज़रा भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी. यह सब कैसे हो सका, मैं आपको बताता हूँ. दशरथ की मृत्यु के पहले राम, लक्ष्मण और सीता शोकमग्न दशरथ की अनुमति लिए बगैर वनगमन करते हैं, भास ने ऐसा प्रतिमानाटकम् में लिखा है. दूसरे अंक में एक अद्भुत दृश्य है, जहाँ दशरथ उस ओर देखकर, जहाँ से राम, लक्ष्मण और सीता वन गये हैं, विलाप करते हैः
सूर्य इव गतो रामः, सूर्य दिवस इस लक्ष्मणोह्ढनुगतः ।
सूर्यदिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता॥
इसका मंचन करते हुए मैंने इन तीनों को जंगल में जाते हुए दिखाया, दर्शकों की ओर जाते हुए, वे तीनों रंगमंच पार कर रहे हैं और धूलधूसरित दशरथ उन्हें पुकार रहे हैं. दशरथ पुकारते-पुकारते गिर जाते हैं. इस क्षण के बाद वे स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं. इस वक्त मैंने यह दिखाया कि सूर्यवंश के तीन महापुरूष दिलीप, अज और रघु बारी-बारी से मंच पर आते हैं, वे दशरथ को पुकारते हैं, उन्हें अपने में शामिल होने का न्यौता देते हैं. अपने पूर्वजों से घुलने-मिलने की प्रक्रिया में दशरथ भी प्रतिमा में रूपान्तरित हो जाते हैं. मंच पर जैसे वे सभी मिलकर एक आकृति बन गये हों. और तब इन प्रतिमाओं से सज्जित प्रतिमागृह में भरत प्रवेश करते हैं. वे पूजा करना चाहते हैं. प्रतिमागृह का पालक देवकुलिक उन्हें कहता है कि यह न करें, यह देवालय नहीं, यह वह स्थान है, जहाँ इक्ष्वाकु कुल रहता है. इस पर भरत कहते हैं कि मुझे बताइए यहाँ किन किन लोगों की प्रतिमाएँ हैं. वे यह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिमागृह नया बना है यानि भरत के ननिहाल जाने के बाद बना है इसलिए भरत को उसके बारे में पता नहीं है, उन्हें तो यह भी पता नहीं है कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है. अयोध्या में प्रवेश करने के लिए कृत्तिका नक्षत्र के बीतने का इन्तज़ार करते हुए भरत संयोग से इस नये बने प्रतिमागृह में आ गये हैं. प्रतिमापालक देवकुलिक हरेक प्रतिमा के बारे में भरत को बताता जाता हैः ‘ये राजा दिलीप हैं, इन्होंने ये ये किया था आदि’ मैंने सारे पूर्वजों को मुखौटा पहने दिखाया है, उन्हें देखकर भरत और देवकुलिक गोल घेरे में घूमते हैं. ये राजा अज हैं इन्होंने ये ये किया है. भरत भी अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, अच्छा ये वही राजा अज हैं जिन्होंने ऐसा-ऐसा किया है वगैरह. और तब वे देवकुलिक से पूछते हैं, ये कौन हैं? उन्हें खुद अपने पिता की प्रतिमा पर शक होता है. ‘क्या इस प्रतिमागृह में जीवितों की प्रतिमाएँ भी रखी गयी हैं?’ देवकुलिक कहता है नहीं, केवल उन्हीं की जो जा चुके हैं अतिक्रान्तानामेव. इस तरह भरत को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलती है और वे वहीं मूर्छित हो जाते हैं. तभी संयोग से सुमन्त्र के साथ कौशल्या, कैकयी और सुमित्रा प्रतिमागृह में आती हैं और देखती हैं कि भरत वहाँ गिरे पड़े हैं. भरत सुमन्त्र से कहते हैं, ‘मैं माताओं को प्रणाम करने का क्रम जानना चाहता हूँ, आप मेरा इनसे परिचय कराइए. पहले कौशल्या का परिचय कराया जाता है, ‘ये राम की माँ हैं’. फिर सुमित्रा का, ‘ये लक्ष्मण की माँ हैं’ और कैकयी के लिए कहा जाता है कि ‘ये आपकी माँ हैं.’ भरत प्रणाम किये बगैर क्रोधित होकर कहते हैं, ‘आः पापे, तुम मेरी इन माताओं के बीच ऐसी लग रही हो जैसे गंगा और जमुना के बीच प्रविष्ट हुई कोई कुनदी.’ भरत कैकेयी को खूब कोसते हैं तभी वशिष्ठ और वामदेव भरत को यह सन्देश भेजते हैं, ‘जैसे गोपाल के बिना गायें वैसे ही राजा के बिना प्रजा भी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए आपका राज्याभिषेक हो. इस पर भरत कहते है कि राम के बिना अयोध्या में रहने का अर्थ ही क्या है ? राम के बिना अयोध्या, अयोध्या नहीं है. अयोध्या वहीं है जहाँ राम हैं.
नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः
यह कहकर भरत वहाँ से सीधे वन चले जाते हैं. इस नाटक के मेरे मंचन में भरत वन जाकर अपने बड़े भाई से पादुका और उनके नाम पर राज्य चलाने की अनुमति लेकर लौट आते हैं. उनके अयोध्या लौटने से पहले राम उन्हें सलाह देते हैं. यहीं मैंने पाठेतर-पाठ (ध्वनि पाठ) का उपयोग किया है, ‘मातरं रक्ष कैकयीं मा रोषं कुरू तां प्रति’ तुम्हें अपनी माँ के प्रति कोई रोष नहीं होना चाहिए, यह सलाह राम भरत को देते हैं, जिसे मैंने सीधे वाल्मीकि रामायण से लिया. वन से लौटते समय यह सलाह भरत के कानों में लगातार गूँजती है. वन जाते समय भरत ने अपनी माँ से झगड़ा किया था, अब वे उसी रास्ते से लौट रहे हैं यानि वे उसी रास्ते से लौट रह हैं जहाँ प्रतिमागृह है. बल्कि प्रतिमाएँ उनके रास्ते में आ जाती हैं, उन संयुक्त प्रतिमाओं के सामने जिसमें उनके पिता की प्रतिमा भी शामिल है, वह सिर पर पादुका रखे-रखे अपनी माँ कैकेयी से मिलता है. इस समय तक भी उसके कानों में ‘मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरू तां प्रति’ गूँज रहा है. यह उसकी स्मृति में गूँज रहा है और इसे ही उसके मृत पूर्वज अंगीकार कर लेते हैं. वे भी वही कहना शुरू कर देते हैं. वे भी राम के उस उपदेश गान को दोहराने लगते हैं. फिर मैं दोबारा भास के लिखित पाठ पर लौट आता हूँ, जहाँ कैकेयी भरत को बताती हैं कि उसे यह सब क्यूँ करना पड़ा. इसे मैंने बहुत संक्षेप में मंचित किया है. भरत समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी माँ के प्रति रोष नहीं रखना चाहिए और वे प्रतिमाओं की यानि पूर्वजों की उपस्थिति में कैकेयी के चरणों पर गिर पड़ते हैं. यही मैंने इस नाटक को समाप्त किया है जिससे मैं इस नाटक को प्रतिमा और ‘प्रति मा’ भी कहने का साहस जुटा सका. इसी तरह उसके नाम का, मेरी समझ में, औचित्य सिद्ध हो सका है.
संगीता गुन्देचा
आपने प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् और स्वप्नवासवदत्तम् को एक साथ किया है, क्या उनके बारे में कुछ बताएँगे?
पणिक्कर
मैंने ऐसा हिन्दी में करने की कोशिश की थी. भारतरत्न भार्गव ने इसका अनुवाद किया था. मैंने इन नाटकों को संस्कृत में करते समय जिन विचारों के सहारे जो ध्वनि पाठ (सबटेक्ट्स) विकसित किये थे, उन तमाम विचारों का उपयोग करते हुए श्री भार्गव ने यह अनुवाद किया था, जिसमें मुझे एक ऐसा ध्वनि पाठ मिल सका जो कहीं अधिक समृद्ध था, प्रदर्शन की सम्भावना की दृष्टि से. इससे मुझे मंचन की सम्भावनाएँ मिल सकीं. यह एक राजनैतिक नाटक है और मैंने इसे इसी तरह किया भी. स्वप्नवासवदत्ता में भास का एक आयाम उनका स्पेस (रंगाकाश) का उपयोग है. उनका कक्ष्या विभाजन का विचार महत्त्वपूर्ण है. वे कक्ष्या को स्वप्नकक्ष्य और तथ्यकक्ष्य में विभाजित करते हैं. यह विभाजन उदयन के स्वप्न दृश्य में पूरी तरह उपस्थित है. मैंने यह सारा कुछ नाटक की अपनी व्याख्या में शामिल किया है. इसलिए इसके मंचन के दौरान मुझे जब भी ज़रूरत महसूस हुई, मैने मंच पर कक्ष्याएँ तैयार कर ली.
संगीता गुन्देचा
आपने अपनी एक नयी रंगशैली ईजाद की है. उसमें किन-किन चीज़ों का योगदान है ?
पणिक्कर
मैंने अपने नाटकों का मंचन करते हुए अधिकतर लोकतत्त्वों का उपयोग किया है. विक्रमोर्वशीयम् नाटक में उर्वशी जिस लता में बदल जाती है, वह लता सुपारी के पेड़ से बनायी. कल कालिदास समारोह में इस नाटक को करते हुए मैंने वह लता बाँस की कोमल छाल यानि रस्सी से बनायी थी, आपने देखी होगी. यह मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ़ समय-समय पर सलाह दी हैं, उन्हें जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जो सर्जक हैं. यह प्रयोग जी. अरविन्दन ने शुरू किया था, प्रसिद्ध फ़िल्मकार अरविन्दन ने. हमें उनका नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से तत्त्व लेने की प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली है. उदाहरण के लिए, मध्यमव्यायोग में नारियल आदि की पत्तियों का उपयोग. कोलकाता में पहली बार मध्यमव्यायोग का मंचन देखकर शम्भू मित्र इतने उद्वेलित हो गये कि उन्होंने मंच पर आकर सारी नेपथ्य सामग्री पास से देखी. घटोत्कच की वेशभूषा के लिए इस्तेमाल किया गया सूखी घास का वक्षपट, नारियल के कोमल पत्तों से बनाये गये उसके आभूषण, भीम की वेशभूषा में वक्षपट और आभूषण के लिए प्रयुक्त ताड़पत्र और हिडिम्बा का सूखे नारियल के पत्तों से सजा अंगवस्त्र वगैरह देखकर वे जानने को उत्सुक थे कि यह सब कैसे हुआ. मैंने कहा, अरविन्दन हमारे साथ काम कर रहे हैं, यह सब उन्हीं ने किया है. इस अर्थ में अरविन्दन बहुत नवाचारी थे. अभी हाल में जब हबीब तनवीर एक नाट्य समारोह में केरल आये थे, जिसमें हमारा एक नाटक करिंगुटी भी शामिल था, तो स्थानीय रंगसमीक्षकों ने हबीब साहब की बहुत प्रशंसा की और उन्हीं रंग समीक्षकों ने करिंगुटी की पर्याप्त निन्दा की. उन्होंने यहाँ तक लिखा कि यदि देखना है तो हबीब तनवीर का नाटक देखना चाहिए, केरल में कुछ नहीं है. केरलवासियों को यह समझना चाहिए कि उनके पास एक गहरी लोक परम्परा है. उन्हें इसका बोध ही नहीं है और अगर है तो वे यह समझना नहीं चाहते कि इस परम्परा का नैरन्तर्य आधुनिक रंगमंच के लिए अपरिहार्य है. आधुनिक रंगमंच को किसी भी हाल में केरल की सांस्कृतिक अन्तश्चेतना से संबंधित होना ही होगा, क्योंकि जब तक देशी रंगमंच नहीं होगा, मार्गी रंगमंच नहीं हो सकता. हबीब साहब की लोक प्रेरणा बिल्कुल भिन्न है, उनके नाटकों की अन्तश्चेतना भी. जो भारतीय मार्गी रंगमंच के लिए निश्चय ही अत्यन्त प्रासंगिक है. इसे हमारे लोग समझते नहीं है हालाँकि केरल के बाहर इसे समझने वाले बहुत हैं. मैने करिंगुटी के अपने इस मंचन में अपने गाँव कावालम की लगभग सभी लोकधुनों का प्रयोग किया है. कावालम एक शुद्ध कृषि प्रधान गाँव है, मेरी जड़े वहीं हैं बल्कि यह कहें कि मैं कावालम का ही हूँ. लेकिन मैं समूचे केरल का भी हूँ और केरल ही क्यूँ, पूरे भारत का हूँ. इसी तरह तो राष्ट्रीय थिएटर की धारणा विकसित हो सकती है, जब आप बिल्कुल निचले स्तर से शुरू करें. इसे आप छोटा रंगमंच और अन्यों को बड़ा रंगमंच नहीं कह सकते. ऐसे ही अनेक छोटे रंगमंच मिलकर राष्ट्रीय रंगमंच की सम्भावना चरितार्थ करते हैं. मेरा कावालम का अनुभव मेरी अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त है, न सिर्फ़ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी. लोकधुन जैसे तत्त्व जो मैंने कावालम में रहते हुए अन्तस्थ किये हैं अगर वे सम्प्रेषण के लिए पर्याप्त हैं तो मेरे लिए यह बहुत है. करिंगुटी में मैंने इन्ही लोकधुनों का सृजनात्मक प्रयोग किया है. मैंने उस समूची सांगीतिक व्यवस्था को इस नाटक के सन्दर्भ में पुनराविष्कृत करने का प्रयत्न किया है. इसमें इस बात से भी मदद मिली कि यहाँ नाटक का लेखक और रंगनिर्देशक एक ही व्यक्ति है. कई बार इनके एक होने से मदद नहीं भी मिल सकती है, लेकिन इस बार यह मददगार साबित हुआ क्योंकि हम एक रंगभाषा विकसित करने के प्रयास में थे. वह नाटक एक ही था लेकिन केरल में उसे एक ढंग से देखा गया और कोलकाता में किसी और ढंग से. स्वयं हबीब तनवीर ने जब यह नाटक देखा तो उन्हें यह इतना पसन्द आया कि उन्होंने अपने अभिनेताओं से आग्रह किया कि वे न सिर्फ़ यह नाटक देखें बल्कि मुझसे मिलकर यह समझने की कोशिश करें कि मैंने इस नाटक में लोकतत्त्वों का किस तरह समावेश किया है. एक और तरह के देशी रंगमंच को देखना हबीब साहब के लिए आह्लादकारी रहा होगा जो उनके रंगमंच से नितान्त भिन्न था लेकिन तब भी जिसमें ऐसे अनेक तत्त्व थे जिनका उनके रंगमंच के कई तत्त्वों से साझा था. यही मैंने न सिर्फ़ अपने लिखे नाटकों में किया है बल्कि संस्कृत के नाटकों में भी इसके अलावा कुछ नहीं किया. मैंने चाक्यारों का अनुकरण नहीं किया है. अगर हम चारी करते हैं तो नाट्यपाठ की अपेक्षा से ही. आगे चलकर जब हम पाते हैं कि इन नाट्य प्रयोगों का नाट्यशास्त्र में उल्लेख है, तो प्रसन्नता होती है. कुछ नाटप्रयोगों का नाट्यशास्त्र में उल्लेख नहीं भी है. नाट्शास्त्र कभी भी नाट्यधर्मी और लोकधर्मी की सारी सम्भावनाओं को पूरी तरह निःशेष नहीं करता बल्कि चारी और करणों के प्रयोग की सम्भावना को वह इंगित भर करता है. किसी एक भंगिमा से शास्त्रोल्लिखित अर्थ के अलावा भी अनेकार्थ सम्प्रेषित किये जा सकते हैं. इस भंगिमा में बहुत महीन परिवर्तन करके किन्हीं अधिक सूक्ष्म अर्थों को भी सम्प्रेषित किया जा सकता है. नाट्यशास्त्र को याद करके उगला नहीं जाता, वह नाटकृति की अपेक्षा के अनुरूप स्वयं प्रकट होता है. भरत ने अपने अनुभव के आधार पर नाट्यशास्त्र की रचना की और इसकी रचना के लगभग नौ सौ साल बाद अभिनव गुप्त आकर उसे पुनराविष्कृत करते हैं. इस बीच अनेक व्याख्याकार आये होंगे लेकिन इसके बाद भी दसवीं शताब्दी के अन्त में अभिनव गुप्त को यह आवश्यकता महसूस हुई कि वह एक बार फिर उसकी व्याख्या करें. अठारहवीं शताब्दी में आकर एक मलयाली विद्वान बालवर्धन को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वह भरत के नाट्यशास्त्र की देशी व्याख्या करें. उन्होंने इस पर पूरी पुस्तक लिखी है जो मुख्यतः उपांग अभिनय की चर्चा करती है. इस पुनर्व्याख्या की सम्भावना भरत के नाट्यशास्त्र में पहले ही उपस्थित है इसलिए यह बिल्कुल सम्भव है कि भास भरत के बाद होने पर (अगर हम ऐसा मान लें) यह कह सकते है कि मृत्यु मंचित हो सकती हैं जैसा उन्होंने पूरी खूबसूरती से दशरथ की मृत्यु, दुर्योधन की मृत्यु को मंचित करके दर्शाया है.
संगीता गुन्देचा
विक्रमोर्वशीयम् में द्विपदिका प्रयोग क्या है ?
पणिक्कर
विक्रमोर्वशीयम् नाटक में कोयल से नाटक के राजहंस तक जाने में एक अन्तराल है, इस अन्तराल के बीच में द्विपदिका है, ‘अनन्तरे द्विपदिकया ऐसा कालिदास ने निर्देश किया है. पुरूरवा कोयल के निकट पहुँचता हैं, उसका वर्णन करता है, उससे अपनी प्रिया के बारे में बात करता है. यह एक संचारी भाव है, जो स्थायी भाव को अलंकृत करता है. इसके बाद उसे राजहंस के पास जाना है. लेकिन इन दोनों घटनाओं की बीच एक वक्रता होनी चाहिए. जब हम एक संचारी भाव से दूसरे संचारी भाव की ओर जा रहे हों, तो इस अन्तराल में अनिवार्यतः एक वक्रता होनी चाहिए जिसके लिए द्विपदिका का प्रयोग होता है. यह एक विशुद्ध नृत्य है, जो अभिनेता को चरित्र से खुद को अलग करने का अवसर देता है, साथ ही एक क़िस्म के विश्राम का भी. ताकि अभिनेता अगले संचारी को व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाए. कालिदास ने अपने नाटकों में यह लिखा है, भास ने नहीं लिखा. भास के नाटकों में नाटनिर्देश वाचिक में अन्तर्भूत हैं, इसलिए आप इस वाचिक की अनेक तरह से व्याख्या कर सकते हैं, यह सम्भावना वहाँ मौजूद है.
संगीता गुन्देचा
केरल के गाँवों में थय्यम् होते हैं, वे भी एक तरह से लोकधर्मी नाटरूप हैं. आपके रंगमंच में थय्यम् का भी यत्किंचित् योगदान है ही, आप थय्यम् के बारे में कुछ बताएँ ?
पणिक्कर
थय्यम् अनेक हैं. कहा जाता है कि केरल में लगभग सात सौ थय्यम् हैं, जो पैंतीस प्रकार के हैं. ये थय्यम् सात सौ (या अधिक) कैसे हो जाते हैं? अगर किसी गाँव में कोई घटना हो जाती है और उसमें कोई वीरतापूर्वक शामिल होता है तो इसका थय्यम् बना दिया जाता है. ये एक तरह के थय्यम् हैं. दूसरी तरह के थय्यम् प्रेतात्माओं को लेकर बनाये जाते हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव की खातिर जान दे देता है, इसका भी थय्यम् बनाया जाता है. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी. गाँव में एक रईस आदमी है जिसकी एक बेटी है. बेटी का दोस्त अपेक्षाकृत गरीब आदमी का बेटा है. यह लड़का जब आम के पेड़ पर बैठा पके आम खा रहा था, नीचे खड़ी लड़की उससे आम माँगती है और वह उसे देता नहीं है. या तो उसने सुना नहीं है या सुनना नहीं चाहता और इस तरह वह लड़की के लिए फल नहीं फेंक रहा. इसकी जगह वह आम खाकर उसकी गुँठलिया लड़की की ओर फेंकता है. लड़की आकर अपने पिता से शिकायत करती है. रईस पिता इस बात को गम्भीरता से लेता है और उस लड़के से बदला लेने उसकी खोज में निकल पड़ता है. जब लड़के को यह बात पता चलती है, वह घबराकर गाँव से भाग जाता है. वह गाँव के बाहर एक बूढ़ी औरत के साथ रहने लगता है. वह बूढ़ी औरत विष्णुमूर्ति की पूजक है. वह लड़के से दूध मँगवाकर गरम कर उसे पीने के लिए देती है और हमेशा उससे पूछती है, ‘पालण दाई कण्णा’ यानि दूध कैसा है कण्णा, कण्णा यानि कृष्ण. यह प्यार का नाम है. उस लड़के का नाम पालण दाई कण्णा ही पड़ जाता है. एक दिन वह लड़का उस बूढ़ी औरत से अपने गाँव जाने की अनुमति लेता है और गाँव जाकर लोगों के हालचाल पूछता है. लेकिन उसके आने की खबर उस लड़की के पिता को हो जाती है. वह अब भी उससे बदला लेना चाहता है इसलिए वह उसे मारकर तालाब में फेंक देता है. मृत्यु को प्राप्त यह लड़का थय्यम् हो जाता है, जिसका नाम पालण दाई कण्णन् है लेकिन अन्ततः पालण दाई कण्णन् विष्णुमूर्ति में अन्तर्भूत हो जाता है. इस तरह यह विष्णुमूर्ति थय्यम् का एक प्रकार हो जाती है. विष्णुमूर्ति थय्यम् के अनेक प्रकार हैं. इस तरह विष्णु के अलग-अलग जगहों अलग-अलग आयाम हो जाते हैं जिनका सम्बन्ध स्थानीय कथाओं से होता है. एक तरह से थय्यम् मृतात्माओं की लोक प्रतिष्ठा है. थय्यम् में अनेक तरह की वेशभूषाएँ होती हैं. जैसे कई तरह के शिरस्त्राण होते हैं, गोल शिरस्त्राण, तिकोने और बहुत बड़े आकार के शिरस्त्राण.
संगीता गुन्देचा
क्या भास के नाटकों का मंचन करते हुए आपने थय्यम् का प्रयोग किया है ?
पणिक्कर
हाँ, उरूभंगम् में.
संगीता गुन्देचा
आपने उरूभंगम् के किस हिस्से में यह किया है?
पणिक्कर
मैंने थय्यम् का उपयोग उरूभंगम् में एक ध्वनि पाठ (सबटेक्ट्स) की तरह किया है. इस एकांकी के अन्त में दुर्योधन के भूमि पर गिरने के बाद मैंने एक और दुर्योधन की कल्पना की, जो उसका आत्मन् है और जो थय्यम् की तरह उसके सामने खड़ा है. यह थय्यम् उस बुरे व्यक्ति दुर्योधन को वह सब बताता है जो अच्छा है. यह मैंने भास के ही शब्दों का उपयोग करते हुए किया है. उसमें मैंने कोई छूट नहीं ली है. जैसे-जैसे दुर्योधन गिरता है वैसे-वैसे उसका थय्यम् खड़ा होता जाता है. दुर्योधन अपनी देह छोड़ते हुए कहता है, ‘मां नेतुं वीरवाही विमानः कालेन प्रेषित’: वीरों को ले जाने वाला, काल के द्वारा भेजा हुआ यह विमान मुझे लेने आ गया है. विमान के लिए मैंने दो छड़ियों का प्रयोग किया है, जो दुर्योधन के हाथ में रहती हैं. थय्यम् ही दुर्योधन को सारी सुखकर और सारी भयावह चीज़ें दिखाता है. अन्त में भूलुण्ठित दुर्योधन जब मरता है, मंच पर आप उसे अपने थय्यम् से एक होता हुआ देखते हैं.
संगीता गुन्देचा
आप भरत के रंगमंच का भास के साथ क्या सम्बन्ध देखते हैं ?
पणिक्कर
भौतिक स्तर पर भरत ने जिन प्रेक्षागृहों के बारें में लिखा है उनमें चतुर्भुजाकार, चतुरस्र्र, वर्गाकार विकृस्र और त्रिभुजाकार त्र्यस्र प्रेक्षागृह हैं, लेकिन अण्डाकार प्रेक्षागृह का विचार भी केरल में है. इस प्रेक्षागृह के केरल में अब सिर्फ अवशेष हैं. वह लगभग दौ सो साल पहले जल गया था. मत्तवारिणी भी एक भौतिक तत्त्व है. पण्डितों में यह बहस रही है कि मत्तवारिणी कहाँ हो, और कैसी हो? हमें किसी भी नाटक की संरचना और उसकी प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुति के सन्दर्भ में सोचना चाहिए. मत्तवारिणी की संरचना, रंगमंच का क्षेत्र, उसमें अभिनय का क्षेत्र, रंगशीर्ष, रंगपीठ को ध्यान में रखकर हम कक्ष्या–विभाजन या रंगाकाश का विभाजन करते हैं. रंगाकाश के विभाजन से भी हमें नाटक की संरचना के बारे में महत्त्वपूर्ण दृष्टि मिलती है. इसमें पटी और अपटी भी शामिल है, जो हमें रंगदृश्य प्रदान करती है. कक्ष्या के बारे में हमें भरत के कथनों से बहुत मदद नहीं मिलती. संस्कृत नाटकों में रंगमंच पर किसी अभिनेता का प्रवेश या निष्क्रमण बहुत महत्त्व का है. उसमें एक रेखीय क़िस्म का प्रवेश नहीं होता जैसा कि यथार्थवादी रंगकर्म में होता है. वह अनिवार्यतः एक वक्रता के विचार को चरितार्थ करता है, वहाँ कोई पात्र ऐसे ही टहलते हुए रंगमंच पर नहीं आ सकता, वह घूमकर आता है और इस घुमाव की उस नाटक की संरचना से संगति होती है. भास के नाटकों में एक पात्र कैसे रंगमंच पर प्रवेश करेगा, वह कैसा दिखायी देता है, यह उन नाटकों के श्लोंको में है. ‘मध्यमव्यायोग’ में आप घटोत्कच के लिए यह लिखा हुआ पायेगीं:
सिंहास्य, सिंहदंष्ट्रो, मधुनिभनयनः स्निग्धगम्भीरकण्ठो, ब्रभ्रुभूः श्येननासो आदि.
चरित्र कोष्ठक में लिखे इन निर्देशों के अनुसार ही प्रविष्ट नहीं होता, वह मुद्राओं के साथ प्रवेश करता है या उस पात्र से दर्शकों का परिचय कोई और पात्र कराता है. जैसे उरूभंगम् में जब दुर्योधन बलराम को पुकारता है, बलराम आते हैं और वे टूटी हुई जंघा वाले दुर्योधन के रंगमंच पर आने का वर्णन करते हैं:
भूसंसर्पणरेणुपाटल भुजो बालवृतम् ग्राहितः
वह ज़मीन पर सरकने के कारण धूलधूसरित भुजाओं वाले बालक की तरह लड़खड़ाते हुए आ रहा है, युद्ध के बाद वह उसी तरह थका हुआ है जैसे अमृत मन्थन के बाद खोला गया नागराज वासुकी. यहाँ समूचे रंगमंच और विभिन्न गतियों की परिकल्पना एक-दूसरे से जोड़कर ही करनी होगी क्योंकि ये अन्तर्सम्बन्धित हैं. पात्र परिक्रमा यानि कौन पात्र रंगमंच पर कहाँ और कैसे आएगा इस सबकी परिकल्पना आपको करनी होगी.
संगीता गुन्देचा
दूतवाक्यम की आपके मन में क्या व्याख्या है. मेरा आशय उस व्याख्या से है, जिसे आपने मंचित किया है? जैसे आपने प्रतिमानाटकम् करते हुए ‘प्रतिमा’ की एक नयी व्याख्या अपने मंचन में प्रस्तावित की थी ?
पणिक्कर
इस नाटक की शुरूआत में सिर्फ़ एक पात्र है दुर्योधन. वैसे भी इस नाटक में कुल मिलाकर दो पात्र ही हैं कृष्ण और दुर्योधन यदि आप कंचुकी आदि को छोड़ दें तो. मैंने यह नाटक उज्जैन में किया था और चित्रपट दर्शन वाले दृश्य को बहुत विस्तार से किया था.
संगीता गुन्देचा
आपने कृष्ण के विराट रूप का मंचन कैसे किया था ?
पणिक्कर
जब हमने शुरू में दूतवाक्यम् किया था तो मंच पर एक साथ तीन-चार कृष्ण प्रकट होते थे और उज्जैन के मंचन में वही कृष्ण मंच पर कई जगह दिखायी दिये हैं. यह दृश्य हमने प्रकाश की मदद से किया था.
संगीता गुन्देचा
इस बार कर्णभारम् के प्रदर्शन में क्या आपने कुछ परिवर्तन किये हैं ?
पणिक्कर
अभिनेता के बदलने से कुछ परिवर्तन करने ही होते हैं. प्रश्न यह नहीं है कि इस बार कर्ण की भूमिका अभिनेता मोहनलाल कर रहे हैं इसलिए परिवर्तन किये गये. कर्णभारम् में ही नहीं मध्यमव्यायोग में भी ऐसा ही हुआ था. पहले जगन्नाथन् घटोत्कच की भूमिका निभाते थे, फिर शिवन् ने जब यह भूमिका की तो कई छोटे-छोटे परिवर्तन उस पात्र में आये.
संगीता गुन्देचा
मध्यमव्यायोग में अभिनेता के बदलने पर कौन से परिवर्तन घटोत्कच के चरित्र में आये?
पणिक्कर
जब शिवन् ने घटोत्कच की भूमिका निभायी तब घटोत्कच में काफी लड़कपन है. मैंने शिवन् के अभिनय वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर यह किया था. वैसे भी घटोत्कच बहुत युवा है. जब वह अपने पिता भीम से युद्ध करता है तब भी वह बहुत युवा है. मैंने मध्यमव्यायोग में घटोत्कच की ऐसी मुद्राएँ प्रदर्शित की जिसमें वह शरारती युवक जान पड़े. जब अभिनेता बदलता है तब नाटकृति की निर्देशकीय व्याख्या की सम्भावनाएँ भी बदल जाती हैं. कई बार ये सूक्ष्म हो सकती हैं कई बार बिल्कुल स्पष्ट.