निर्मल वर्मा की चिट्ठियों के वे दिन: ज्योत्स्ना मिलन
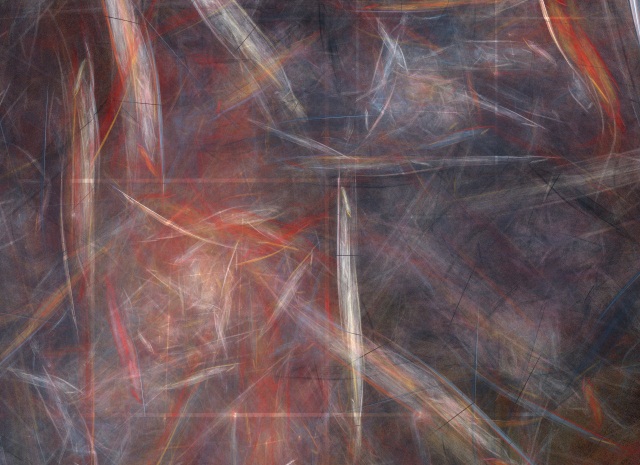
कितना अच्छा था कि निर्मलजी से परिचय और दोस्ती के वे दिन अभी चिट्ठियाँ लिखने के दिन थे. चिट्ठी यानी हाथ की लिखी, असलीवाली चिट्ठी, ई-मेल वाली बिना किसी पहचान की, वर्च्युअल चिट्ठी नहीं. हाथ की लिखी हर चिट्ठी की अपनी एक अलग पहचान होती है. उसी उसी ककहरे और बाराखड़ी से बनी होती है हर लिखावट, तब भी होती है कितनी अलग एक-दूसरी से. हर लिखावट एक अलग हाथ का अलग विस्तार, जो हाथ से अलग हो जाती है फिर भी बची रहती है हाथ की पहचान, उसमें.
लिखावट बड़ी-छोटी हो सकती है, टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है, सुंदर-असुंदर हो सकती है, स्पष्ट-अस्पष्ट हो सकती है, एक सी भर नहीं हो सकती. हर किसी ने अ को अलग ढंग से लिखा, मगर मज़ा यह कि जितना भी अलग लिखा हो अ को, वह कुछ और नहीं हुआ, रहा आया अ का अ ही . चाहे उसे मैंने, तुमने, मन्नाजी ने, भँवरीबाई ने, निर्मलजी ने, किसी ने भी लिखा हो, वह हर बार, हर किसी का एक अलग अ हुआ.
लिखावट से क्या किसी व्यक्ति की अलग पहचान की जा सकती है? क्या उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है? क्या उसे जाना जा सकता है कि वह कैसा होगा या हो सकता है अपनी कद-काठी में, बनक में, मुद्रा में, रहन-सहन में? क्या लिखनेवाले के स्वभाव को उसमें पढ़ा जा सकता है? उसकी भीतरी दुनिया की झलक मिल सकती है? क्या उसकी आवाज़ को सुना-परखा जा सकता है ? जाने क्यों यह विश्वास करने को मन करता है कि ऐसा ज़रूर संभव हो सकता होगा और इसकी कोई विधि भी ज़रूर होगी.
निर्मलजी के छोटे-छोटे अक्षरों से बने शब्द और वाक्य एक-दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं. दो शब्दों के बीच पूरा एक शब्द भर दूरी. हर शब्द के इर्द-गिर्द काफी सारी खाली जगह होती है. अपने होने और साँस लेने के लिए ज़रूरी अवकाश को लेकर ही प्रकट होते हैं उनके शब्द. उनकी सम्मोहक भाषा का रहस्य और तिलिस्म जैसे शब्दों के गिर्द के इसी अवकाश से पैदा होता है. उनके लिखे एक एक शब्द और वाक्य ने अपने बनने में जो समय लिया वह भी खाली जगहों में मौजूद है. उनके लेखन की प्रक्रिया में समय और स्थान का अनुपात ही बदल जाता है. शब्द कम, चुप्पियाँ ज़्यादा. अपनी ही आभा में दमकते पारदर्शी शब्द, जिनमें जो है उसके साथ साथ जो है नहीं वह भी कौंध जाता है. मुझे नहीं लगता निर्मलजी की लिखावट जैसी वह है उसके वैसा होने में उनकी कोई सजग भूमिका रही होगी.
१९५८-५९ में निर्मलजी को पहले-पहल पढ़ने का जादू आज भी बना हुआ है यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं. पहली बार में ही वे मुझे अपने लिए एक ज़रूरी लेखक के रूप में मिले. मुंबईवासी मैंने दिल्लीवासी निर्मलजी से मुलाकात का सपना देखने का साहस भी नहीं किया था. मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी जितनी थी उससे कई गुना भीतर थी, जैसे दिल्ली कोई दूसरी दुनिया हो. उस समय अगर कोई यह भविष्यवाणी कर भी देता कि निर्मलजी और हम मुहल्ले के पड़ोसी होंगे तो मुझे ज़रा भी विश्वास न होता. भोपाल आ जाने के बाद मुंबई के मुकाबले दिल्ली से दूरी कम तो हुई थी, फिर भी एक दिन अचानक उसके घटकर एक मुहल्ले के पड़ोसियों के बीच की दूरी में बदल जाने की घटना तो किसी चमत्कार से सूत भर भी कम न थी. इतनी अविश्वसनीय कि अपने को भरोसा दिलाने हम हर दूसरे-तीसरे दिन पहुँच जाते निराला सृजनपीठ कि निर्मलजी सच में वहाँ हैं, लगभग पड़ोस में.
मुहल्ले के मुहल्ले में उनके चिटनुमा पत्र लेकर उन दिनों छोटेलाल अक्सर प्रकट हो जाता था–ज्योत्स्नाजी/कुछ अस्वस्थ सा अनुभव कर रहा हूँ, आसपास कोई अच्छे डॉक्टर हों तो उनका नाम-पता भिजवा दीजिएगा.” या
“छोटेलाल के हाथ कुँवरनारायण का लेख भिजवा दें और छतरी–यदि उसकी ज़रूरत न हो.” या “वीरेन्द्रजी का पता भिजवा दीजिए, उन्हें आज ‘कला का जोखिम’ भेज रहा हूँ.”
पत्र लिखना उनके लिए इतना सहज था कि जिस संदेश को छोटेलाल मुँह-ज़बानी पहुँचा सकता था उसे वे एक पुर्जे पर लिख भेजते थे. वे जानते थे कि अपनी लिखावट में, शब्दों में लिखनेवाला कुछ न कुछ तो शामिल हो ही जाता है. उसकी आवाज़ उन्हीं में दुबकी सुनाई दे जाती है. इन लघुकाय पत्रों को पढ़ते हुए भी सामने खड़ा छोटेलाल भूल जा सकता था और निर्मलजी के वहीं कहीं होने का एहसास घिर आ सकता था. छोटेलाल को अक्सर अपने वहाँ खड़े होने की याद दिलानी पड़ जाती थी फिर मैं अचानक हड़बड़ाकर अपना संदेश लिख कर छोटेलाल को थमा देती थी.
मोहल्ले का यह पत्र व्यवहार अपनी तरह का अनोखा पत्र व्यवहार था, अपने कामकाजी चरित्र के बावजूद. ये छोटे छोटे चिट पत्र उनके पत्रों के हिस्से की तरह उनमें दुबके आए हाथ. मुझे अचरज हुआ कि वे अभी तक थे और बाकायदा थे पत्रों के बीच, पत्रों की तरह.
पिछले दिनों उनके पत्रों को देखने-पढ़ने का अनुभव उनके होने से घिर जाने का अनुभव था. पत्रों में उनका होना उनकी रचना जितना ही सघन और बेलौस होता है. जितना और जिस तरह वे अपने को रचना को देते हैं उससे जरा भी कम पत्र में नहीं देते थे. हम चारों में से हर एक के साथ उनका संबंध एक अलग संबंध था. संबंधों का यह अलगपन हर के साथ के उनके मिलने-जुलने में, बातचीत में, पत्र-लेखन में एकदम नज़र आता है. और यह भी कि दूसरे में उनकी कितनी गहरी दिलचस्पी है. आप किसी भी तरह के संकट से गुज़र रहे हों — रचना के पारिवारिक या सामाजिक जीवन के, स्वयं जीवन के या होने मात्र के संकट से गुज़र रहे हों और आप उनकी साझेदारी चुनें तो यह असंभव है कि वे भी उस संकट से रुबरू न हों. अपने जीवन की उनसे मिलती-जुलती स्थितियों को विस्मृति के निविड़ से निकालकर चकित उन्हें देखते हैं कि इनसे वे कैसे निपटे थे? उन स्थितियों के दूसरे पहलू का पता कैसे लगाया था? इसकी पड़ताल वे करेंगे, जैसे पहली बार कर रहे हों और इस प्रक्रिया में आपको भी अपनी स्थिति का दूसरा पहलू दिखने लग जा सकता है, जिसके बूते आप उस संकट से निकल आ सकते हैं.
पत्रों में बात चाहे निजी संदर्भ से उपजे, चाहे हमारे, चाहे उनके, चाहे किसी रचना के संदर्भ से या किसी यात्रा के संदर्भ से वे उसे ‘घनी झाड़ी में छिपे पक्षी को बिना आहत किये समूचा और साबुत निकाल लाने की तरह संदर्भ से बाहर खुले अवकाश में निकाल लाते थे. वह बात अपने में इतनी स्वायत्त, इतनी पूरमपूर होती कि खुद-ब-खुद साँस लेने लगती और इस प्रक्रिया में वह पारदर्शी होती जाती थी.’
एक पत्र का संदर्भ निर्मलजी की कोई रचना थी जिसे पढ़कर उससे उद्धरण देते हुए मैंने उन्हें लिखा था. यों भी उनके लेखन ने सच बोलकर उन्हें प्रसन्न करने के कई अवसर दिए थे. चकित हूँ कि एक लेखक और एक पाठक के बीच या एक लेखक और दूसरे लेखक के बीच इतना खुला, इतना पारदर्शी नाता हो सकता है. निर्मलजी के पत्रों जैसे पत्र किसी भी समय में कम ही लिखे जा सकते हैं, पढ़े मगर ऐसे पत्र कई कई बार जाते हैं अलग अलग स्थल और काल में. उसे पढ़ने की पहले की स्मृति को चकमा देते हुए हर बार वह एक अलग पत्र निकल आता. इस तरह उनका एक पत्र अनेक पत्रों में बदल जाता. इन पत्रों में लिखनेवाले का अपना जीवन और भीतर की आँच बची रहती है, अपनी समूची आभा के साथ.–
हम जिस ज़माने में रहते हैं उसमें ऐसे पत्र दुर्लभ हो गए हैं! इसीलिए इसे बार बार पढ़ने का लोभ संवरण न कर सका. एक तरफ अपने को बहुत ‘फ्लैटर्ड’ सा महसूस करता हूँ, दूसरी तरफ मन में छिपा चोर यह भी कहता है कि आपने जो जो मेरे लेखन के बारे में लिखा है उसके काबिल बनने के लिए मुझे बरसों मेहनत करनी पड़ेगी.
यहाँ लेखक-पाठक संबंध से परे वे एक ऐसे बिंदु पर खड़े मिलते हैं जब उनके भीतर कहीं एक गहृवर सा खुल जाता है–
इसे झूठी विनम्रता मत समझिए. मैं जिस उम्र में हूँ, उसमें पिछले वर्षों का सहज विश्वास डगमगाने सा लगता है. यह भूलभुलैया की वह जगह है, जहाँ अँधेरा सबसे घना होता है, क्योंकि जिस दरवाज़े से मैं साहित्य में दाखिल हुआ था वह पीछे छूट जाता है और जिस द्वार से मुक्ति मिलने की उम्मीद है, वह कहीं दिखाई नहीं देता. शायद इसीलिए ऐसी मनःस्थिति को कुछ संत कवियों ने- dark nights of the soul- की संज्ञा दी थी.
जब हम अलग अलग शहरों में होते थे तब कभी कभी होनेवाली सामूहिक मुलाकातों के अलावा हमारे बीच होते थे पत्रों के सूत्र. समय के लंबे या छोटे अंतरालों से संबंध की निरन्तरता अबाधित बनी रहती. पत्रों में निर्मलजी संपूर्ण और निबिड़ एकांत की रचना कर पाते थे जिसमें संवाद संभव हो पाता है,एक ऐसा संवाद जो दूसरे के साथ जितना होता है उससे जरा भी कम अपने साथ नहीं होता. ÷शंपा’-मेरी कहानी के निमित्त लिखी गई बात एक साथ अपने और दूसरे के साथ संवाद जैसी है-
मैं हमेशा यह समझता रहा हूँ कि नारी का अपनी देह से रिश्ता, संपूर्ण रिश्ता होता है, जो पुरुष को अपने शरीर से महसूस नहीं होता है, पुरुष अंततः अपनी देह का अतिक्रमण करके किसी ऊपर की अशरीरी चीज़ (आत्मा ? ईश्वर ?) पाना चाहता है, जबकि स्त्री की आत्मा स्वयं उसकी देह में पगती है, बसती है-वह स्वयं ईश्वर या आत्मा को अपनी देह से अलग नहीं कर सकती. पुरुष शरीर को divine के रास्ते पर सबसे बड़ी बाधा मानता है, स्त्री की कपअपदपजल स्वयं उसकी देह की सुंदरता में वास करती है. ‘शंपा’ में आपने बहुत ही गहनता से इस रहस्यमय रिश्ते की परतों को खोला है.
ऐसे पत्रों की एक अलग ही फितरत होती है. वे बीच बीच में उचककर अमरता को छू लेने के कारण भीतर तक जगमगा जाते हैं इसीलिए यह चमत्कार घटित होता है कि जब पत्र लिखनेवाला चला जाता है जब पाने वाला चला जाता है तब भी वे रहे आते हैं, निजी संदर्भों से विलग किन्हीं दूसरों तक यात्रा करते.