एडीटिंग मशीन की संतानें: विनीत कुमार
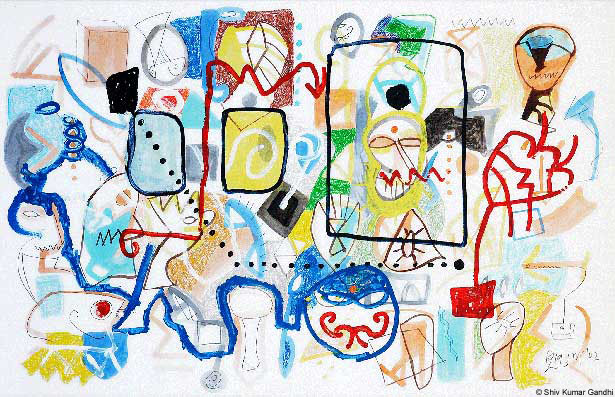
वर्चुअल टेरॅ्, टीआरपी और आतंक की आदत
हिंदुस्तान का कोई भी टीवी पत्रकार इस वक्त तालिबान के इलाके में नही है. लेकिन हर दिन तालिबान पर रिपोर्टिंग हो रही है. चेहरे पर नकाब हाथों में बंदूक लिए आगे और पीछे की उजाड़ वादी यह तालिबान है. सब कुछ फिल्मी स्टाइल में दिखाया जा रहा है. कुछ इस तरह से कि शो में केवल गोली – बंदूक की तस्वीर दिखे. आपको लगे कि वाह क्या देख रहे हैं हिन्दी के टीवी रिपोर्टर सीधा तालिबान के गढ़ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं.
कभी आपने सोचा है कि तालिबान फार्मूला क्यों बन गया है. दरअसल टीआरपी की दौड़ में टीवी चैनलों पर इस तरह की ख़बरों का दौर आता है एक समय भूत-प्रेत चला तो उसके बाद पौराणिक नायकों के ससुराल से लाकर रसोई तक,पलंग तक ढूंढा गया. आप दर्शकों के लिए जब भी ऐसा दौर होता है तो आप हैरान होकर देखते हैं. इससे पहले कि आप चट जाते हैं. तब लगता है कि ये तो बेकार की न्यूज़ देखते रहे तब तक टीवी का काम हो जाता है. टीवी चैनल वाले भी नए फार्मूले की तरफ़ बढ़ जाते हैं. तालिबान एक नया फार्मूला है. 26 नवम्बर को मुम्बई पर हमला क्या हुआ कि टीवी को फार्मूला मिल गया.[i]
आमतौर पर टेलीविजन में काम करनेवाले लोगों के मुताबिक, टेलीविजन- समीक्षा के नाम पर हिन्दी मीडिया आलोचकों के पास टीआरीपी हासिल करने की कवायद में जुटे चैनलों और पत्रकारों को कोसने के अलावा कोई गंभीर समझ नहीं है। आजकल टेलीविजन न्यूज चैनलों की आलोचना करने की परंपरा सी बन गयी है।[ii] कार्यक्रम चाहे जो भी हों, सबके लिए विज्ञापन और टीआरपी से जोड़कर देखने की एक परंपरा-सी विकसित हो गयी, टेलीविजन समीक्षा के नाम पर एक मुहावरा चल निकला- टीआरपी के लिए टेलीविजन वाले जो न करें। ये धारणा इतनी मजबूत और प्रचलित हो चली है कि कोई व्यक्ति टेलीविजन की आलोचना कर्म में अकादमिक या लेखन के स्तर पर सीधे-सीधे न भी जुड़ा हो तो भी बड़ी आसानी से टेलीविजन को टीआरपी का दास साबित कर सकता है। मीडिया आलोचकों ने विश्लेषण के नाम पर टेलीविजन को टीआरपी की देहरी पर ला पटका है। मीडिया आलोचना का यह रवैया न तो टेलीविजन के लोगों के गले उतरता है और न ही इसमें तटस्थ और सकारात्मक समझ का विकास ही हो पाता है।
लेकिन आज, इसी पैटर्न पर, न्यूज चैनलों की आलोचना कोई मीडिया आलोचक न करके स्वयं एक चैनल कर रहा है। यानि एक खबरिया चैनल ऐसा करके अपने ही उपर कोड़े बरसाने का काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल कॉन्फेशन के दौर से गुजर रहा है। एनडीटीवी द्वारा 27 जनवरी 08 को आंतकवाद की खबरों के पीछे के खेल की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की गयी कि सहयोगी न्यूज चैनल टीआरपी की खातिर क्या-क्या नहीं करते हैं। खबर के नाम पर कूड़ा-कचरा प्रसारित किए जा रहे हैं। आतंकवाद के नाम पर ऐसी खबरों का प्रसारण, जिसका दर्शकों से कोई सरोकार नहीं है,जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं, वो फील्ड की रिपोर्टिंग नहीं है। पत्रकार यूट्यूब की खानों में खो चुके हैं, एडिटिंग मशीन के बूते ऐसी खबरों को गढ़ा जाता है और धमारेदार आवाज और चौंका देनेवाले लेबलों के साथ खबरों को परोसा जाता है।[iii]
एनडीटीवी की इस खबर पर गौर करें तो दो बातें स्पष्ट हो जाती है, एक तो यह कि न्यूज चैनल इस तरह की खबरों का प्रसारण इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि देश की ऑडिएंस 26 नबम्बर 08 के मुंबई आतंकवादी हमले से, उसके भय और असुरक्षा से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। यानि आतंकवाद से जुड़ी खबरें अभी भी उनके लिए प्रासंगिक है और दूसरा यह कि ये खबरें फील्ड की रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं बल्कि एडिटिंग मशीन की संतान है, जो कि मैनिपुलेटेड है, अविश्वसनीय है। आतंकवाद की यह वास्तविक छवि नहीं है। इस लिहाज से अगर हम रोज शाम प्राइम टाइम पर प्रसारित होनेवाले आतंकवादी खबरों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि चैनलों का इरादा हमारे बीच, देर तक ख़ौफ के बने रहने, असुरक्षा के साथ जीने और असंभावित घटनाओं से घिरे रहने का महौल पैदा करना है।
ऐसा करने से न्यूज चैनलों के प्रति लोगों का रुझान लंबे समय तक बना रह सकता है। क्योंकि ज्योतिष की तरह टेलीविजन खबरों के साथ भी लोग तभी तक ज्यादा समय तक जुड़े रह सकते हैं, जब तक उस पर हमेशा असंभावित होने का खतरा पैदा देने वाली खबरें हो, भीतर एक बेचैनी बनी रहे कि आगे क्या होगा। कोई जरुरी नहीं कि ये बेचैनी सिर्फ़ किसी एक घटना या हादसे को लेकर हो। बेचैनी की यह मनोवृति स्थायी तौर पर उनके भीतर जम जाए और वो हर बात के लिए बेचैन हो जाएं। ये काफी कुछ सिनेमाई अंदाज में होता है। सिनेमा दर्शकों के सामने एक ऐसी स्थिति या छवि प्रस्तुत करता है जहां वे खुद को ख़ौफ और भय से भरी दुनिया से रु-ब-रु पाते हैं.[iv]
आतंकवाद से जुड़ी खबरों के प्रसारित किए जाने की स्ट्रैटजी की व्याख्या जिस रुप में की जा रही है,आतंकवाद के नाम पर न्यूज चैनलों में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, उसे काफी हद तक खबरों के बदलने का एक पैटर्न भर माना जा सकता है। लेकिन एक स्थिति यह भी है कि रोजमर्रा के तौर पर आतंकवाद की खींची गयी छवि हमें किसी भी हद तक आतंकित नहीं करती,बेचैन नहीं करती। बल्कि एक आदत पैदा करती है, आतंकवाद को लेकर फेमिलियर बनाती है, हमें इस बात के लिए अभ्यस्त करती है कि हम आतंकवादी घटनाओं को किसी भी समय, किसी भी मनस्थिति में देखने के लिए तैयार हो सकें। इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए सूसन सोंटाग का मानना है कि- ये सब कैमरे से उतारी गयी छवियाँ हैं। वे इतनी ज्यादा प्रतिदिन दिखती है कि वे औसत यथार्थ में बदल गयी है। इन छवियों का जिन ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में जन्म हुआ, ये अपने उन मूल अभिप्रायों को खो देती हैं और स्वायत्त छवियां बन जाती है। इसलिए इन छवियों के प्रति हमारा विवेकशील और आलोचनात्मक रवैया नहीं,बल्कि उनसे सम्मोहित हो जानेवाला एक रिश्ता बन गया है। छवियां आज वास्तविकता की सिर्फ नकल नहीं है। वे वास्तविकता से ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी हैं। वे वास्तविकता को नष्ट कर देना चाहती हैं और हम निरंतर उन छवियों के संसार में रह रहे हैं। या सच तो यह है कि हम छवियों के शिकार हैं।[v] यानि हम जिसे सच मान कर देख रहे होते हैं, वो छवियों के अंबार से भरा एक पैकेज भर होता है।
अब, एनडीटीवी की इस खबर, सूसन सोंटाग की इस मान्यता और टीआरपी के खेल के आधार पर चैनलों की आलोचना से अलग एक स्थिति है जिस पर गौर किया जाना जरुरी है। न्यूज चैनलों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को दिखाए जाने के पीछे जागरुकता, सामाजिक सच,यथार्थ को उसके वास्तविक रुप में लाने की कोशिश की बात की जाती है। सामाजिक जागरुकता की बात करते हुए आतंकवाद से जुड़ी जो तस्वीरे और खबरें दिखायी जाती है, उससे आतंकवाद की छवि किस तरह की बनती है, इसे समझना जरुरी है।
फिलहाल, मुंबई आतंकवाद के संदर्भ में बात करें तो आतंकवाद और उससे पैदा होनेवाली भयावह स्थिति को दिखाने के लिए कुछ विजुअल्स स्टैब्लिश किए गए जिसे कि लगभग सभी चैनलों ने खबरों के पीछे का बैग्ग्राउंड( क्रोमा) के तौर पर इस्तेमाल किया।
1. होटल ताज की बिल्डिंग से उठती आग की लपटें,
2. हथियारों से लैस,चेहरा ढंके आतंकियों की तस्वीरें
3. चिखती हुई स्त्रियां और ऑडिएंस की तरफ ताकता मासूम
4. बिना जोड़ी के बिखरी चप्पलें
5. खून से लथ-पथ जमीन
6. भयभित,असहाय और इधर-उधर भागते लोग।
7. मरे हुए पक्षी, बेचैन उड़ते हुए पक्षी
8. दो आंखे जिनमें एक ही साथ दर्द, बेचैनी और असहाय हो जाने के कई मिलते-जुलते भाव मौजूद होते हैं।
9. घटना स्थल पर लगातार आग फैलने और धमाके के होने के विजुअल्स
अगर होटल ताज, नरीमन हाउस और होटल ऑबराय को छोड़ दे तो बाकी के विजुअल्स आपको किसी भी आतंकवादी घटना के होने पर मामूली हेर-फेर के साथ दिखायी देंगे। आतंकवादी घटनाओं के विजुअल्स देखते हुए कोई भी आसानी से बता सकता है कि चाहे स्थिति कितनी भी भयावह हो, कुछ भी कवर करने की स्थिति न बनने पाती हो लेकिन आतंकवाद के महौल को स्टैब्लिश करने के लिए इतना सब कुछ दिखाना अनिवार्य है। यानि आतंकवाद की छवि को स्थापित करने के लिए चैनलों के भीतर एक शास्त्र निर्मित है। इस तरह की घटनाओं में विजुअल्स की कमी की वजह से एक ही तस्वीर बार-बार दिखाई जाती है और इससे एक स्थायी छवि निर्मित होती है। इन विजुअल्स के साथ जिन शब्दों का जिसे कि एस्टर्न और स्लग कहते हैं वह भी लगभग निर्धारित होता है। भाषा साफ-साफ दो स्तरों पर बंट जाती है। एक स्तर वो जिसमें आतंकवाद, उसकी स्थिति,उससे बनने वाले हालात को अधिक से अधिक असरदार तरीके से दिखाए जा सकें। बाद में इसमें सरकार की नाकामी, राजनीतिक पेंच, संबद्ध लोगों की बाइट आदि आ जाते हैं, फिलहाल हम उस दिशा में न जाएं तो भी।
और दूसरा स्तर जिसके जरिए जज्बात,भावना,राष्ट्रीयता और इंडियननेस होने के सबूत को प्रस्तुत किए जाएं। शब्दों का इन दो रुपों में प्रयोग मुंबई आतंकवादी घटनाओं में भी किया गया। आतंकवादी घटना के पहले और दूसरे दिनों तक कुछ चैनलों( स्टार न्यूज, इंडिया टीवी) ने इसे अधिक से अधिक भयावह बताने के लिए 9/11 की तर्ज पर 26/11 का प्रयोग किया। इसके पीछे की रणनीति सिर्फ इतनी कि ऑडिएंस पेंटागन के मंजर और उसके अनुभव से इसे जोड़कर देखे। 9/11 आतंकवाद की एक स्थापित छवि है जिसमें किसी एक विजुअल्स के बिना पूरा का पूरा आतंकवादी दृश्य अपने आप उभरकर सामने आ जाता है। उसके बाद आतंक को घंटों में बताया जाना शुरु किया गया। आतंक के 18 घंटे[vi] या फिर आतंक के 37 घंटे[vii]। आतंक को घंटे में बताए जाने से आतंकवादियों की तैयारी और प्रशासन की असफलता की एक तस्वीर हमारे सामने उभरती है। हालांकि बाद में यह अवधि जितनी हो और बतायी जाए उससे जज्बात को उतना उपर तक उठाया जा सकता है कि देश ने आतंकवादियों का मुकाबला कितने घंटों तक किया। इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि शब्दों के जरिए टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रयुक्त छवि यूनीइमैजिनरी होते हैं जो दो विरोधी पक्षों और विपरीत दशा में एक ही साथ काम में लाए जा सकते हैं। राष्ट्रहित की बात करते हुए आतंकवाद की एक और छवि चैनल द्वारा बनाने की कोशिश की गयी। यह छवि यूट्यूब और एडिटिंग मशीन से बनी छवि से अलग है, यह छवि तस्वीर रहने के वाबजूद देश की सुरक्षा की खातिर नहीं दिखाने की छवि से अलग है। यह छवि बनती है आतंकवादी और एंकर के बीच के सीधे संवाद से।[viii] इस बातचीत का एक अंश है-
एंकर-
आपलोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारने से आपको क्या मिलेगा?होटल ताज में छिपा आतंकवादी-
जब लोग बाबरी मस्जिद गिरा रहे थे,उस समय लोगों को इस बात का खयाल क्यों नहीं आया।…. यहाँ हमारे भाई को परेशान किया जाता है, हमें सुकून से सोने नहीं दिया गया। हमारी मां-बहनों को कत्ल-ए-आम दिया गया।[ix]
आतंकवादियों की एक यह भी छवि है जिसे चैनल फोन पर( हालांकि इस फोन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए) हुई बातचीत के आधार पर निर्मित करता है।
एडीटिंग मशीन से पैदा की जानेवाली वर्चुअल टेर् को समझने के क्रम में सिल्वरस्टोन के टेलीविजन और तकनीक संबंधी विचार पर नजर डाल लेना दिलचस्प होगा। सिल्वरस्टोन का मानना है कि टेलीविजन अपने-आप में एक तकनीक है औऱ यह एक ऐसा तकनीक है जो कि दो प्रकार के अर्थों से जुड़ा हुआ है। इससे पैदा होनेवाले अर्थ एक तो निर्माता और उपभोक्ता के जरिए होता है और दूसरा स्वयं इस तकनीक के द्वारा जो कि प्रसारण और व्यवहार के दौरान पैदा होता है।[x] सिल्वरस्टोन की माने तो सूसन सोंटाग की कैमरे और तकनीक के आते ही घटना की वास्तविकता खत्म हो जाती है की मान्यता को बिल्कुल उसी रुप में मान लेना व्यावहारिक नहीं जान पड़ता। बिना तकनीक के टेलीविजन के होने की बात नहीं की जा सकती। तकनीक की अनिवार्यता ही टेलीविजन या फिर दूसरे संचार माध्यमों को संभव कर सकती है। दूसरी बात कि टेलीविजन से पैदा होनेवाले अर्थ सिर्फ उनके निर्माताओं की सक्रियता से नहीं होती बल्कि स्वयं उसका उपभोक्ता यानि ऑडिएंस भी अर्थ पैदा करने में सक्रिय होते हैं। यहां पर मार्शल मैक्लूहान की यह मान्यता खंडित होती है कि टेलीविजन कोल्ड माध्यम है क्योंकि यह उपभोक्ता को पैसिव बनाता है।[xi] मार्शल मैक्लूहान के बाद टेलीविजन विमर्श में एक अवधारणा तेजी से विकसित हुई जिसके अन्तर्गत ऑडिएंस को भी अर्थ पैदा करनेवाला यानि प्रोड्यूसर के तौर पर समझा गया।[xii]
ऑडिएंस के अर्थ ग्रहण करने और पैदा करने का ही परिणाम है कि उन खबरों की भी खपत होती है, उनकी भी टीआरपी बढ़ती है जिससे कि सीधा सरोकार बहुत ही कम लोगों का होता है या फिर कई बार नहीं भी होता है। सूसन सोंटाग की मान्यता के आधार पर जब लोग ड्राइंग रुम में बैठकर आतंकवाद की खबरें देख रहे होते हैं तो इत्मिनान होते हैं, उनके भीतर एक निश्चिंतता का बोध होता है कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या देश और दुनियाभर की ऑडिएंस टेलीविजन को इसी रुप में जानती-समझती है। तकनीकी रुप से सबों के टेलीविजन स्क्रीन एक ही तरह के होते हैं, संभव है एक ही खबर या प्रोग्राम को एक ही साथ लाखों लोग देख रहे हों, लेकिन क्या उनकी मान्यताएं, उनकी सामाजिक स्थिति और समझ एक होती है।[xiii] ऑडिएंस के बीच कई स्तरों की भिन्नता ही खबरों के अर्थ को बदलता है और साथ ही उसके बीच एक निजी संदर्भ पैदा करता है। तालिबान में होनेवाले हमले से हिन्दुस्तान के किसी गांव या कस्बे में बैठी ऑडिएंस को कोई खतरा नहीं है, मुंबई में होनेवाले आतंकी हमले से देश के दूसरे हिस्से में बैठी ऑडिएंस को तत्काल कोई नुकसान नहीं हो रहा,संभव है करोड़ों ऑडिएंस का आहत लोगों से कोई सीधा सरोकार नहीं हो लेकिन खबर तो सब देखते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि टेलीविजन अनिवार्यतः एक घरेलू माध्यम है और इसलिए ऑडिएंस उसकी खबरों औऱ कार्यक्रमों के बीच से अपने संदर्भ और अर्थ खोज लेती है.[xiv] यानी आतंकवादी खबरों से अधिक से अधिक लोगों के जुड़ने के पीछे सिर्फ उसके निश्चिंत महौल में खबर की तरह इन्ज्वॉय करना भर नहीं होता है बल्कि उस खबर में स्थानीय खौफ और आंतक के चिन्हों की तलाश करना भी होता है। तकनीक और एडिटिंग मशीन के इस्तेमाल होने से ऑडिएंस इसी संदर्भहीन आतंक के बीच से अधिक से अधिक स्थानीय संदर्भ खोजने की कोशिश करती है जिसे हम ऑडिएंस के बीच पैदा हुए अर्थ कह सकते हैं।
ऑडिएंस आतंकवाद की जिन खबरों में अपने एक निजी संदर्भ की तलाश करती है,उसे खबर प्रसारित करनेवालों के अनुसार अर्थ ग्रहण करें तो इसके दिखाए जाने के पीछे राष्ट्रचिंता और मानवता के स्वर छिपे हैं। नोम चॉमस्की ने ब्राजील तक दूसरे देशों का हवाला देते हुए जो लिखा है कि यहां संचार माध्यमों के बारे में मानकर चला जाता है कि वे सार्वजनिक हित की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है,[xv]कमोवेश वही स्थिति भारतीय संदर्भ में भी है। ऑडिएंस जिस स्तर पर खबरों से अर्थ ग्रहण करती है वो निजी होता है, खबरों के प्रसारण के पीछे भी यही रणनीति काम कर रही होती है कि हर खबर की प्रस्तुति कुछ इस तरीके से हो कि ऑडिएंस उसमें अपने मतलब की बात को खोज पाए लेकिन स्ट्रैटजी से अलग इनके तर्क बिल्कुल अलग हैं।
होटल ताज के सामने से कवर करते हुए हमलोग जो भी दिखा या कह रहे थे वह यथार्थ था उसमें कोई ड्रामा नहीं था। आतंकवादी गतिविधियों के शुरु होने के बाद से ही स्टार न्यूज का पूरा का पूरा दफ्तर और टॉप मैनेजमेंट लगातार साठ घंटे तक न्यूज रुम में मौजूद रहा और उस वक्त हममें से किसी के दिमाग में रेटिंग शब्द शायद ही कभी आया होगा।[xvi]
खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा की ।खातिर हम तस्वीरें लाइवें नहीं दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रियदर्शन लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं।[xvii]
ये खबर लाइव नहीं है। चैनल जो अपनी टीआरीपी के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइव करवेज के लिए परेशान रहते हैं, सरकार की ओर से मिले निर्देश के अनुसार अब लाइव प्रसारण नहीं कर रहे होते हैं। यही काम बाकी के चैनलों ने भी किया।
इस बयान के मुताबिक मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान जो कुछ भी दिखाया गया,वो टीआरपी का खेल नहीं था,उसमें राष्ट्रहित की भावना जुड़ी थी। देश और दुनिया के लोगों को यह बताने की कोशिश थी कि कुछ लोग मानवता के खिलाफ कितना गंदे से गंदा षडयंत्र कर सकते हैं। यानि आतंकवाद के मंजर को दिखाने के क्रम में न्यूज चैनलों के पास अपने-अपने दृष्टिकोण,समझ और व्यावहारिक प्रयोग है। यहां आकर आलोचना का यह आधार कि टीआरपी के लिए चैनल कुछ भी कर सकते हैं, टूटता नजर आता है, ऑडिएंस के निजी अर्थ और खबरों के प्रसारणकर्ता के तर्क से पैदा हुए अर्थ के बीच का एकहरापन टूटता है। यहां आकर ऐसा नहीं होता कि ऑडिएंस जिस स्तर पर अर्थ ग्रहण कर रही होती है पूरी तरह वही अर्थ संप्रेषण हो रहा होता है और ऐसा भी नहीं होता कि प्रसारणकर्ता जिसे राष्ट्रहित बता रहे होते हैं, आतंकवाद से जुड़ी खबरों को दिखाने के पीछे यही स्ट्रैटजी पूरी तरह काम कर रही होती है।
इस स्थिति में सिल्वरस्टोन की अर्थ पैदा होने के दूसरे आधार पर गौर करें तो यह भी समझना जरुरी होता है कि संचार से भी अर्थ बनते हैं जिसमें ऑडिएंस की कोई भूमिका नहीं होती। उपरी तौर पर प्रसारणकर्ता की भी कोई भूमिका नहीं होती। कैमरे का सच या फिर कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता का मुहावरे के प्रयोग के पीछे बार-बार यही साबित करने की कोशिश रहती है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसके प्रति प्रसारणकर्ता तटस्थ है। खबरों की प्रस्तुति में शामिल लोगों की तटस्थता को स्थापित किए जाने की स्थिति में प्रसारण औऱ तकनीक की भूमिका बढ़ जाती है और ऑडिएंस को बिना कोई मैनिपुलेशन के खबर प्रसारित होने का आभास होता है।
लेकिन यही आकर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि तकनीक का आधार लेकर अपने को तटस्थ बताने की रणनीति क्या तर्कसंगत है। आज एनडीटीवी ने आतंकवादी घटनाओं की खबरों को दिखाए जाने के पीछे जिस तरह से आपत्ति दर्ज की है, उसमें तकनीक पर सवार होकर अपने को तटस्थ बताए जाने का फार्मूला कितना विश्वसनीय है, इस पर विचार किए जाने चाहिए। क्या तकनीक और प्रसारण के बीच अपने अनुरुप खबरों का रुख करने की कोई गुंजाइश नहीं होती।
इस संदर्भ में पी.एन.बासंती का मानना है कि मुंबई आतंकवाद की खबरों को जिस तरह से टेलीविजन चैनलों ने दिखाया, खबर को जिस तरह से लोगों के बेडरुम तक पहुंचाया वो रियलिटी शो के रुप में था।[xviii] बासंती खबरों की प्रस्तुति के लिए रियलिटी शो का प्रयोग कर रही हैं, यानी पूरा विश्लेषण इस संदर्भ में है कि खबरों को जिस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं उससे खबरों के कंटेट से अलग अर्थ पैदा होते हैं। आतंकवादी घटना को देखने के बाद खौफ,असुरक्षा औऱ चिंता के भाव पैदा होने चाहिए लेकिन रोमांच औऱ कौतुहल पैदा होता है। शायद यही वजह है कि देश की ऑडिएंस आतंकवादी घटनाओं को किसी खबर के बजाय आदतन एक कार्यक्रम के तौर पर देखने की अभ्यस्त होती चली जाती है। हार्रर फिल्मों की तरह थोड़ी देर डरकर खुद का विरेचन करती है। संभवतः यही वजह है कि वो इस आदत के बीच डेस्कटॉप पर चले रहे यूट्यूब और चैनलों द्वारा फिर से कैमरे में कैद कर लिए जाने और उस पर कुछ चमकदार लेबल और स्लग लगा दिए जानेवाली खबरों को भी देखकर परेशान नहीं होती, आतंकवाद को खत्म करने के लिए बेचैन नहीं होती और चैनल जिस राष्ट्रीय चिंता का आधार तय करता है, उसे लेकर असहमत नहीं हो पाती।
भारतीय दर्शकों के बीच एक बड़ी सच्चाई ये है कि वो न्यूज चैनलों के जरिए प्रसारित होनेवाली खबरों औऱ घटनाओं को सच मानकर चलती है। इस लिहाज से प्रसारणकर्ता का ये फार्मूला कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता काम कर जाता है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता की समझ के नीचे विकसित होनेवाले दर्शकों के लिए ये समझना वाकई मुश्किल काम है कि कैमरे के पहले औऱ बाद भी किस तरह के तकनीकी प्रयोग किए जाते हैं औऱ उससे अर्थ( मतलब भी औऱ टीआरपी भी) पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। यहां पर डेविड मोर्ले की बात पर विचार करना जरुरी है कि ऑडिएंस टेलीविजन के अर्थ को किस रुप में ग्रहण करती है, इससे समझने के लिए उसके परिवेश और मान्यताओं को तो समझना जरुरी है ही इसके साथ ही ये भी समझना जरुरी है कि वो आसपास की तकनीक से किस रुप में जुड़ी हुई है।[xix]
नलिन मेहता ने कैमरे से बनी छवि और ऑडिएंस के उपर इसके असर को जब 2002 के गुजरात दंगे के संदर्भ में देखते हैं, तब इसी कैमरे और माइक के होने से डरे हुए लोग घर से बाहर निकलकर आए और दुनिया के सामने आकर अपनी बात रखी।[xx] इसी टेलीविजन और तकनीक के बीच से पैदा होनेवाली बेचैनी औऱ सवाल से जुड़कर मुंबई आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और टेलीविजन के फुटस्टेप को मानते हुए अपनी बात रखी। इसलिए तकनीक और संचार के बीच से पैदा होनेवाले अर्थ सिर्फ वर्चुअल स्पेस के भीतर भटकनेवाले शब्द भर नहीं होते, उसका रुपांतरण सामाजिक स्तर पर भी होता है। इसलिए एक स्थिति ये भी बनती है कि यह समाज को पहले से अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। एसएमएस और फोन कॉल के जरिए इन घटनाओं के विरोध में, लोगों के समर्थन में अपनी बात रखते हैं, वह भी लोकतंत्र का हिस्सा है, इसे चाहे तो टेली-डेमोक्रेसी कहा जा सकता है।
भारतीय दर्शकों के बीच टेलीविजन सहित मोबाइल, कैमरे, इंटरनेट और दूसरे संचार औऱ तकनीक माध्यमों का जितनी तेजी से प्रसार बढ़ रहा है उससे एक निष्कर्ष निकालना आसान हो गया है कि तकनीक को लेकर भारतीय समाज फैमिलियर होता जा रहा है। लेकिन इस तकनीक का उपयोग किस स्तर तक किया जाता है इससे विश्लेषित करना आसान नहीं है औऱ संभव है कि प्रसार को लेकर जो हम हुलस रहे हैं तकनीक आधारित जागरुकता के इस निष्कर्ष पर यह जानकर हम उदास हो जाएं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल महज एक उत्पाद के रुप में हो रहा है न कि एक संचार माध्यम के रुप में।
फिलहाल,मुंबई आतंकवाद द्वारा निर्मित छवियों का प्रभाव विश्लेषण करें तो इतना तो स्पष्ट है कि लोग इसे देखकर ठीक वैसे ही निश्चिंत नहीं हुए जिस तरह से निश्चिंत होने की बात सोंटाग करती है। कम से कम मुंबई की ऑडिएंस के संदर्भ में तो नहीं ही कहा जा सकता है। बाद में तो देश के अलग-अलग हिस्सों में भी सक्रियता बढ़ी। सोंटाग जिसे निष्क्रियता बता रही है, वो यहाँ ठीक उलट हाइपर डेमोक्रेसी के रुप में उभरकर सामने आता है। चैनलों को आतंकवाद से डरानेवाली स्ट्रैटजी के बजाय जज्बाती होनेवाली स्थिति की तरफ ले जाता है। इसलिए चैनलों द्वारा निर्मित इन छवियों को जल्दीबाजी में सिर्फ टीआरपी के फार्मूले, सोंटाग के ऑफ फोटोग्राफी के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषित करने के बजाय लोगों के बीच बननेवाले डेमोक्रेटिक-कल्चर को भी संदर्भ के तौर पर देखना अनिवार्य होगा। यह सिर्फ मीडिया विश्लेषण का हिस्सा नहीं बल्कि इसका संबंध समाज के बीच संरचनागत बदलावों, कई दूसरे दृष्टिकोणों, अनुभव और प्रभावों से है। इसलिए छवि निर्माण की प्रक्रिया पर बात करते हुए इन सबका शामिल किया जाना अनिवार्य है। लेकिन नलिन मेहता के कैमरे का असर और राजदीप सरदेसाई की टेलीडेमोक्रेसी की मान्यता को काफी हद तक मान लेने के बाद भी इस बात को समझना जरुरी है कि सारा काम कैमरे का नहीं है। तकनीक के नाम पर हमें कैमरे से आगे एडिटिंग रुम में होनेवाली गतिविधियों को भी समझना होगा। हिन्दी मीडिया में समाज, संरचना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव औऱ घरेलू परिवेश के आधार पर विश्लेषण करने की पद्धति एक आकार ले रही है, इसी क्रम में तकनीक, लोगों से उसके जुड़ाव औऱ जागरुकता के आधार पर विश्लेषण करने का दौर शुरु हो जाए तो संभव है कि साइट और यूट्यूब के भरोसे खबरें गढ़नेवाले न्यूज चैनलों को कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते का मुहावरा इस्तेमाल करने के पहले दस बार सोचने पड़ जाएं।…
संदर्भः-
[i] स्पेशल रिपोर्टः एनडीटीवी इंडिया,9.35 बजे रात, 27 जनवरी 08)।
[ii] सुप्रिया प्रसाद,न्यूज डॉयरेक्टर,न्यूज 24, मीडिया खबर डॉट कॉम
[iii] सावधान आ रहा है तालिबान…/आगे बढ़ रहा है तालिबान…तालिबान के बढ़ते कदम…/तालिबान से भारत को खतरा…हो रही है जंग की तैयारी…/तालिबान कर सकता है हमला…तालिबानी मानव बम का खतरा…/भारत का दुश्मन नंबर वन…। (स्पेशल रिपोर्टः एनडीटीवी इंडिया,9ः37 बजे रात, 27 जनवरी 08)।
[iv] रवि वासुदेवन, ख़ौफ़ का उन्मादः सिनेमा की शहरी बेचैनी, मीडियानगर-03 नेटवर्क-संस्कृति, पेज नं-02 2007,सराय सीएसडीएस,,दिल्ली-110054
[v] छवियां वास्तविकता को ख्तम कर देती है-सूसन सोंटाग, अंधेरे समय में विचार, बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध का वैचारिक परिदृश्य(विजय कुमार) पेज-207-08, संवाद प्रकाशन, मुंबई,मेरठ, 2006
[vi] आजतक, 5.07 बजे,27 नबंबर 08
[vii] स्टार न्यूज,4.45 बजे, 28 नबंबर,08
[viii] अपील का असर आतंकवादियों ने की इंडिया टीवी से बातचीत। (इंडिया टीवी,10.08 बजे सुबह,27 नबंबर 08)
[ix] वही
[x] आर सिल्वरस्टोन -लेख, टेलीविजन एंड एवरीडे लाइफः टूवर्ड्स एन एन्थ्रोपोलॉजी ऑफ दि टेलीविजन ऑडिएंस, पुस्तक- पब्लिक कम्युनिकेशनः दि न्यू इम्परेटिव्स, सं- एम फर्गसन, लंदनःसेज,1990
[xi] मार्शल मैक्लूहान(1965),अंडर्स्टैंडिंग मीडियाःदि एक्सटेंशन ऑफ मैन,अध्याय 2 न्यूयार्क, अमेरिकन लाइब्रेरी.
[xii] क्रिस बारकर(2003), दि एक्टिव ऑडिएंस, कल्चरल स्टडीज, पेज नं-325, सेज पब्लिकेशन इं. प्रा.लि.बी-42,पंचशील एन्क्लेव,नई दिल्ली 100017
[xiii] डेविड मोर्ले(2002), टेलीविजन ऑडिएंन्सेंज एंड कल्चरल स्टडीज,पेज नं-203, राउटलेज 11 न्यू फिटर लेन,लंदन
[xiv] नोम चॉमस्की (2006,हिन्दी संस्करण), जनमाध्यमों का माया लोक, अनुवादक-चंद्रभूषण ग्रंथशिल्पी(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,बी-7 लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली 110092
[xv] मीडिया मंत्र( जनवरी-फरवरी 08)सं- पुष्कर पुष्प,डायरी पेज- दीपक चौरसिया( एडीटर, नेशनल न्यूज, स्टार न्यूज)
[xvi] आजतक, 7 बजे सुबह, 29 नवंबर 08
[xvii] एनडीटीवी इंडियाःमुकाबला दिसंबर 12, 08 पी.एन.बासंती, डायरेक्टर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज
[xviii] डेविड मोर्ले(2002), टेलीविजन ऑडिएंन्सेंज एंड कल्चरल स्टडीज,पेज नं-204, राउटलेज 11 न्यू फिटर लेन,लंदन
[xix]नलिन मेहता(2008) इंडिया ऑन टेलीविजन, पेज नं-294,हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली
[xx] वही पेज नं- 257, राजदीप सरदेसाई का मत
मैं भी दिल्ली पहुँचने से पहले तक ‘कैमरा झूठ नहीं बोलता’ मुहाबरे का समर्थक था, लेकिन जब तकनीक समझा तो पता चला कि हम वही देखते हैं जो वीडियो-एडिटर दिखाना चाहता है।
विनीत बाबू, आप तो ऐसे ही मीडिया से जुड़े मुद्धे उठाते रहें और मेरी पीएचडी में मदद करते रहें। खैर जहां तक तालिबान वाला मामला है तो यह कुछ नहीं है यहां तो लोग दिल्ली में बैठकर न्यूयार्क से बाइलाइन ले लेते हैं।