अप्रैल 2008 / April 2008
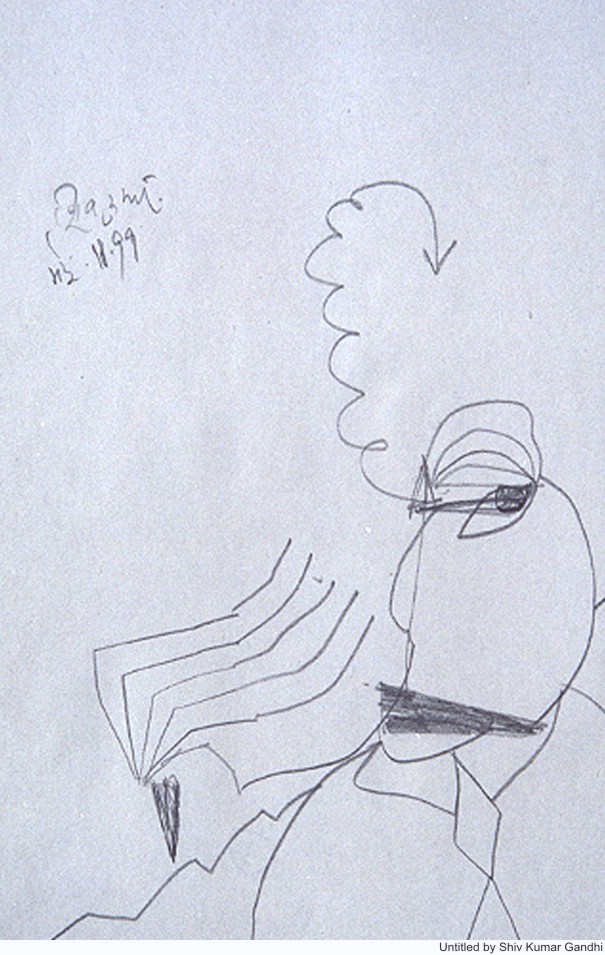
| पत्रिकाओं के पहले अंक उत्साह-से भरे और उनके पहले सम्पादकीय लगभग किःची (Kitschy) होते हैं.
ये सम्पादकीय ऐसी सामाजिक-वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं से लबरेज़ होते हैं कि हमें अपने साथ ‘गिरा’ लेते हैं. इस प्रफुल्ल पतन का अनुभव, अक्सर, हम सभी के लेखकीय जीवन की एक सहज ‘घटना’ है. हम यह बात यद्यपि मूलतः साहित्य, कला आदि की, और उनमे भी गैर-सांस्थानिक किस्म की पत्रिकाओं के सन्दर्भ में कह रहे हैं, लेकिन अन्य अनुशासनों में भी ‘रचनात्मक’ प्रयत्न अपनी शुरुआत में लगभग एक जैसी ‘वैज्ञानिक’ निश्चयात्मकता, और बीमा कंपनियों जैसी भविष्य-दृष्टि के साथ अवतरित होते हैं. वे किसी ईश्वरीय दूत की तरह बोलते हुए लगते हैं. अपने होने का औचित्य पाने के लिए वे संवादों, संघर्षों, यूटोपियाओं के धुंधलके में उतरते हैं. वे लगभग किसी प्रतिरोधक-टीके के बिम्ब में बदलने लगते हैं.यह सम्पादकीय लिखते हुए, अर्थात प्रथमतः यह पत्रिका निकालते हुए, हम इस प्रफुल्ल पतन से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं.इसके विकल्प में, प्रतिनिधित्वमूलक भाईचारे के एवज़ में, हम सिर्फ़ इतना ही कह पाएंगे कि : १. पत्रिकाओं को सिर्फ़ एक अंक की ‘योजना’ ठीक-ठीक मालूम होनी चाहिए. संसाधन १०० के होने चाहिए; संसाधन से हमारा तात्पर्य एक-दो उन्मादी संपादकों, एक-दो अच्छे कम्प्यूटरों, और थोड़े-बहुत पैसों से हैं. २. प्रतिलिपि का ई-पत्रिका होना सिर्फ़ एक औपचारिकता हैं. यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक पारंपरिक पत्रिका हैं. ३. वे बहुत सारे लेखक (किसी भी अनुशासन के) जिन्होंने कभी कोई पत्रिका नहीं निकाली, न प्रयत्न किए लेकिन बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं (उनमें भी जिन्हें वे अच्छी नहीं मानते) उन्हें कम-से-कम एक बार एक पत्रिका निकालनी की जेनुइन कोशिश करनी चाहिए. ४. संस्थानिक पत्रिकाएं या तो लोक-कल्याणकारी तकाज़ों/खज़ानों से निकलती है, या किसी प्रकाशन गृह की विपणन युक्ति के रूप में. इन दिनों पहली तरकीब की मियाद ख़त्म हो चुकी है और दूसरी वहनीय नहीं, कम-से-कम भारत में, चाहे हिन्दी में या अंग्रेज़ी में. हिन्दी में सब कवियों की पुस्तकें ३००-५०० छपती हैं पर हिन्दी में हर वर्ष ५००-१००० काव्य पुस्तकें छपती हैं . भारत में अंग्रेज़ी कविता की स्थिति और भी चिंतनीय है. (ऐसे में इस अंक के तीनों कवियों को सम्हाल कर रखें) प्रतिलिपि का पहला अंक हिन्दी की हंस, कथादेश, तद्भव, पहल जैसी और अंग्रेज़ी की द लिटिल मैगजीन,….., जैसी पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम. अगर वे नहीं होते तो इन दिनों गंभीर लेखन ‘अदृश्य’ ही होता. |
First issues of magazines tend to be over-enthusiastic. And first editorials, verging on kitsch.
These editorials so overflow with social and/or personal ambitions that they make us ‘fall’ for (or should I say with) them. Such enthralled falls are a part of all creative lives. I was going to say ‘writing lives’, having art, literature and magazines of a certain kind in mind, but it holds true for ad-ventures in other disciplines as well which start off with similar LIC-style visions for the future and ‘scientific’ certainty. They seem to speak like prophets, and in trying to justify their existence, descend into the fug of dialogues, struggles and utopias. In writing this editorial and, to be sure, in bringing out this magazine, we are trying to avoid that enthralled fall. In its stead we will only say this much: 1. That all you really need to start a magazine is a proper “plan” for one issue, and the resources for a hundred. By resources we mean a couple of zealous editors, a couple of decent computers, and a little money. 2. That Pratilipi is an online magazine only in that it is online. It is, otherwise, a magazine in the traditional sense. 3. That all those writers (of whatsoever discipline) who haven’t ever started a magazine, nor tried to, but have instead been published in many (including those they do not hold in great regard) – should, at least once, make a genuine attempt to do so. 4. There used to be two ways of bringing out institutional magazines – with social-welfare agendas/funds, or as a marketing strategy for publication houses. These days, the first is not even an option and the second is not viable. In Hindi, the print run for a poet ranges from 300 to 500 copies. Nevertheless, every year 500 to 1000 books of Hindi poetry are published. The situation for English poetry, in India, is even worse. (All the more reason to treasure the 3 poets in this issue.) This first issue of Pratilipi is dedicated to magazines like Hans, Kathaadesh, Tadbhav, Pahal etc. (in Hindi), The Little Magazine etc. (in English) – and their editors. Without them, today, serious writing would have remained merely something to aim for. |
editorial :good, but inadequate.
Thanks Madan, at one level we knew it was ‘inadequate’, in many ways, at another we wanted it to be ‘inadequate’ – at least to the extent that we could avoid knowing things in a ‘pahunchela/i’ manner.
We were scared of sounding ‘far too adequate’.
Editors
I like this line
वे बहुत सारे लेखक (किसी भी अनुशासन के) जिन्होंने कभी कोई पत्रिका नहीं निकाली, न प्रयत्न किए लेकिन बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं (उनमें भी जिन्हें वे अच्छी नहीं मानते) उन्हें कम-से-कम एक बार एक पत्रिका निकालनी की जेनुइन कोशिश करनी चाहिए
and
संस्थानिक पत्रिकाएं या तो लोक-कल्याणकारी तकाज़ों/खज़ानों से निकलती है, या किसी प्रकाशन गृह की विपणन युक्ति के रूप में. इन दिनों पहली तरकीब की मियाद ख़त्म हो चुकी है
congratulations for such a powerful and sincere effort.I heartly welcome “pratilipi”.
इस तथ्य से निराश होने की या इसे सत्य की तरह समझने की ज़रूरत नहीं है कि हिन्दी में सब कवियों की पुस्तकें ३००-५०० छपती हैं. इस तथ्य के अपवाद भी मैं या कोई बता सकता है लेकिन अपवाद भी नियम को पुष्ट ही करते हैं. यानी, अगर यह सच है तो भी एक प्रबल प्रतिसत्य के साथ इसका मुक़ाबला होना चाहिए, मसलन प्रतिलिपि जैसे सत्य के साथ. और यह बात सबके साथ मेरे लिए भी अब एक चुनौती है कि हर लेखक अपनी ज़िन्दगी में कम से कम एक पत्रिका निकाले.