With Hope, In Spite of Fear: Purushottam Agrawal
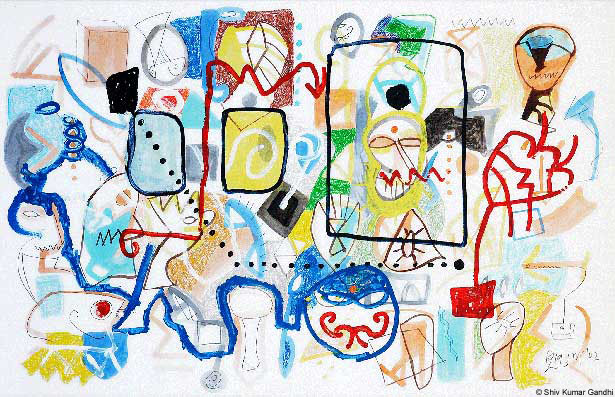
डर के बावजूद, उम्मीद के साथ: ‘फारेनहाइट 451’
मिखाइल बुल्गाकोव का उपन्यास मास्टर ऐंड मार्गरेटा एक प्रसंग में हमें बताता है- ‘जिस पर कुछ लिखा हो, ऐसा कागज जलने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता’ । बुल्गाकोव ने ये शब्द 1940 में, स्तालिन शासित सोवियत संघ में लिखे थे। जिस देशकाल की बात हम करने जा रहे हैं, उसने बुल्गाकोव के इन शब्दों को चुनौती मान कर ऐसे दुष्ट क़ागज़ को जलाने की एकदम पक्की व्यवस्था बना ली है, जो लिखे शब्दों के घमंड में जलने से इन्कार करने की गुस्ताख़ी करे।
वह ऐसा देशकाल है, जहाँ फायर-ब्रिगेड का काम आग बुझाना नहीं, किताबों में आग लगाना है। जहाँ फायरमैन असल में बुकबर्नर है। जहाँ सूचना-मनोरंजन का ही नहीं, सोच-विचार का भी सामाजिक रूप से स्वीकृत, एकमात्र माध्यम टीवी ही है। वह प्रगतिशील और संपन्न समाज किताब को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह समझ चुका है कि किताब खतरनाक है। जीवन और व्यक्तित्व से संपन्न सत्ता है। ऐसी सत्ता जो पढ़ने वाले के मन में पनपती है। खुद बदलती है, और पढ़ने वाले को भी बदल देती है। ऐसी खतरनाक चीज़ से पिंड छुड़ा कर आपको ‘सुखी’ रखने लायक़ समृद्धि उस देशकाल में जुटा ली गयी है, और इस समृद्धि के मजे़ लूटने के लिए आवश्यक सूचनाएँ( किस मॉल में क्या माल कितने कम दामों पर मिल रहा है!) कभी भी, किसी भी वक्त हासिल करने के लिए टीवी है न। चौबीसों घंटे और सैकड़ों चैनलों के साथ उपलब्ध टीवी!
हमारे समकालीन देशकाल की तरह उस देशकाल में भी टीवी केवल सूचनाएं नहीं देता, वह समाधान भी देता है। असल में तो वह समस्याएं भी आपके लिए स्वयं पेश करता है, और समाधान भी। आपको बस पेश किए गए समस्या-समाधान सेट में से उसे चुन लेना है, जो आपको सूट करे। आपको “सुखी” रखने पर आमादा व्यवस्था ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि आपको खुद सोचने-विचारने का फाल्तू, कष्टकारी और ‘पॉलिटिकली इनकरेक्ट” काम करना ही न पड़े। किताबें नहीं हैं, तो जाहिर है कि स्मृति भी नहीं है। स्मृति का मतलब इतना ही रह गया है कि कल आपने क्या खाया और परसों आपके प्रिय रियलिटी शो या सीरियल में क्या हुआ। किताब नहीं है तो कल्पना भी नहीं है। शब्दों के माध्यम से लेखक ने अपनी कल्पना को जो रूप दिया है, उसकी खास अपने लिए पुनर्रचना पाठकीय कल्पना के जरिए करने की कल्पना तक करने की किसी को अनुमति नहीं है।
अकेले होते हुए भी अकेले न होने का जो अहसास किताब के साथ होने से मिलता है, वह, जाहिर है कि समाज-विरोधी व्यक्तिवाद और अहंकार का प्रमाण है, और किसी तरह का सोच-विचार ऐसे अहंकार की अभिव्यक्ति। जो कुछ मतलब का है, बाहर ही है, किताबें आपको खामखाह भीतर की बेमतलब बातों में उलझाती हैं। वे खतरनाक हैं, उनसे आपको बचाना व्यवस्था का कर्तव्य है।
आपको विचारमुक्त, स्मृति-वंचित और इस प्रकार “सुखी” रखने के लिए ही व्यवस्था इतनी सुचारु बना दी गयी है कि यदि कोई समाज-विरोधी तत्व समाज को किताबों वाले पिछड़े वक्त में ले जाना चाहे, तो बचने न पाए। लोगों के संस्कार इस हद तक ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ हो चुके हैं कि करेक्ट व्यवहार की लीक तोड़ने वाले अपराधियों की खबर सत्ता को देने में, और सत्ता के साथ मिल कर ऐसे अपराधियों की खबर लेने का नेक काम ‘अपराधियों’ के अपने सगे-संबंधी करते हैं। उन्हें करना भी बस इतना ही है कि किसी के हाथ में, या घर में किताब देख लें तो फायर-ब्रिगेड को फोन कर दें। फायरमैन उर्फ बुकबर्नर आएंगे; उनके हाथों में पानी नहीं, आग उगलने वाले पाइप होंगे। किताब का दहन होगा और किताब पढ़ने के अपराधी का उपचार।
इस “सुखी” देशकाल की कल्पसृष्टि की थी, रे ब्रैडबरी ने- 1953 में प्रकाशित उपन्यास “फारेनहाइट 451” में। शीतयुद्ध के उस समय के अमेरिका में जैसी बुद्धि-विरोधी घुटन में रे ब्रैडबरी रह रहे थे, उसी को उन्होंने अपने उपन्यास में आने वाले समय के ‘डिसटोपिया’ के रूप में पेश किया। ऑरवेल का “1984” सर्वसत्तावादी समाज का ‘डिसटोपिया’ था, तो ब्रैडबरी का डिसटोपिया उपभोक्तावाद और सूचना-क्रांति का। उस समय इस उपन्यास को ‘साइंस-फिक्शन’ के तौर पर पढ़ा गया था। उपन्यास का नाम-‘फारेनहाइट 451’ उस तापमान की सूचना देता है, जिस पर कागज़ जल उठता है। वह “सुखी” देशकाल इस तापमान से इसीलिए पहचाना जाता है क्योंकि उसने मानव के जीवन में फिजूल के पंगे पैदा करने वाले असली खलनायक को पहचान कर “आदर्श समाज” से सदा के लिए बाहर कर दिया है।
ब्रैडबरी ने अपने उपन्यास को साइंस-फिक्शन ही मान कर लिखा था। उपन्यास में यांत्रिक कुत्ते हैं, जो भाग रहे अपराधियों को ‘काटते’ हैं। इन कुत्ता-यंत्रों के दाँतों में बेहोश करने वाली दवा भी है, और फौरन ही जान ले लेने वाले जहर भी। अपराधियों के खतरनाकपन के हिसाब से इन कुत्तों को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अपराधियों का पीछा करते फायरमैन ( उर्फ बुकबर्नर) और पुलिस वालों की कारगुजारियों का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। उपन्यास में परमाणु युद्ध का खतरा भी सदा मंडरा रहा है, “सुखी” समाज का अंत परमाणु हमले के कारण ही होता है। ब्रैडबरी के डिसटोपिया में स्पीड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के सुख की एक पहचान यदि सर्वव्यापी टेलीविज़न है, तो दूसरी है, बेहद तेज-रफ्तार गाड़ियां। यह सब सुख संभव करने वाले मूल कारण को तो आप जान ही चुके हैं- सुखशत्रु पुस्तकों का पूरी तरह से सफाया!
इस उपन्यास पर इसी नाम से फिल्म बनाई फ्रांस्वा त्रुफो ने 1966 में। यह फिल्म सर्वसत्तावाद के खिलाफ बयान तो है ही, पुस्तक-प्रेमी त्रुफो की निजी आस्था का रेखांकन भी है। मैंने यह फिल्म देखी बीस दिसंबर 2004 की रात- लिंडा हेस के घर पर, बर्कले में। असंभव है इस फिल्म को भूलना। आहत भावनाओं, राष्ट्रहित या ‘सही’ विचार की रक्षा के नाम पर किताबों पर बढ़ते हमलों का समय, गंभीर समस्याओं को पंद्रह सेकंड की बाइट में निबटाते और पुलिस मुठभेड़ों और फांसियों के लाइव टेलीकास्ट करते खबरिया चैनलों का समय कहाँ भूलने देता है- ‘फारेनहाइट 451’ को।
इस उपन्यास और फिल्म का कुछ प्रभाव सत्यजित राय की ‘हीरक राजार देशे’ पर भी महसूस होता है। हालाँकि, ‘हीरक राजार देशे’ साइंस-फिकश्न या फैंटेसी के नहीं, लोक-कथा के शिल्प में रची गयी है; उसमें टीवी या फ्यूचरिस्टिक टेक्नॉलॉजी का नहीं, किसी सनकी राजा का राज चलता है, लेकिन इतना तो वह राजा जानता ही है कि “ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा जाने, ज़्यादा जाने, कम माने, इसलिए स्कूल बंद”। त्रुफो की फिल्म के देशकाल का शासन कोई सनकी राजा नहीं, अत्यंत सक्षम और सूक्ष्म व्यवस्था चलाती है। वह शासन लोक-कथाओं के राजतंत्र की नहीं, हमारे आस-पास के आधुनिक और वैज्ञानिक तंत्र की याद दिलाता है।
दिसंबर 2004 याने जॉर्ज बुश को चुनाव में लगातार दूसरी बार मिली विजय का साल। मैं और लिंडा इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। माइकेल मूर की फिल्म ‘फारेनहाइट 9/11’ का ज़िक्र आना लाजिमी था, और इसी क्रम में रे ब्रैडबरी के उपन्यास और त्रुफो की फिल्म का। प्रसंगवश रे ब्रैडबरी (उनकी उम्र इस वक्त 88 साल है) माइकेल मूर से खासे ख़फ़ा हैं कि मूर ने अपनी फिल्म का नाम उनके उपन्यास से मार लिया। खै़र।
थोड़े ख़फ़ा ब्रैडबरी त्रुफो से भी थे कि उन्होंने फ़िल्म में उपन्यास की कई चीज़ें शामिल नहीं कीं। त्रुफो की फिल्म में वे यांत्रिक कुत्ते नहीं हैं, जो पुस्तकें पढ़ने के अपराधियों का पीछा करते-करते ही जहर के इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ डरावनी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां भी नहीं है। उल्टे, फिल्म में यह कहानी सुरम्य, शांत वातावरण वाले छोटे से नगर में खुलती है। परमाणु युद्ध के खतरे को भी फिल्म पारंपरिक युद्ध के खतरे के रूप में बदल देती है।
पात्रों के मामले में भी फिल्मकार ने उपन्यास से छूटें ली हैं। कुछ पात्रों की भूमिका घटा दी गयी है। लेकिन इस मामले में सबसे रोचक बात यह है कि कहानी के नायक गाय मोंटाग को बुकबर्नर से पुस्तक-प्रेमी में बदल देने वाली स्त्री क्लारिस की, और मोंटाग की शिकायत सत्ता तक पहुंचाने वाली उसकी पॉलिटिकली करेक्ट पत्नी मिल्ड्रेड की भूमिकाएं त्रुफो ने एक ही अभिनेत्री-जूली क्रिस्टी- से कराईं हैं। उपन्यास में क्लारिस किसी तेज रफ्तार गाड़ी की शिकार हो जाती है, लेकिन फिल्म में वह अंत तक मोंटाग के साथ है। मोंटाग की भूमिका ऑस्कर वर्नर ने की है। असल में फिल्म के लिए पैसा हासिल होने में इस तथ्य की अपनी भूमिका थी कि जूली क्रिस्टी और ऑस्कर वर्नर जैसे स्टार्स को प्रोजेक्ट ने आकृष्ट किया।
उपन्यास और फिल्म में सबसे महत्वपर्ण फर्क टीवी की भूमिका को लेकर है। फिल्म में टीवी ने, उपन्यास की ही तरह पात्रों के जीवन को आच्छादित तो कर रखा है, लेकिन वह अपने आप में, सारे पाप की जड़–सोर्स ऑफ ईविल– फिर भी नहीं है। फिल्म का आख्यान उपन्यास की ही तरह सुबोध है, लेकिन उसमें विन्यस्त दृष्टि सत्ता-तंत्र की जटिलताओं के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील है।
जीवन में टीवी की हैसियत 1953 में ब्रैडबरी को जितनी ‘फैंटेस्टिक’ लगी थी, 1966 में त्रुफो को उतनी नहीं लगी। फैंटेसी और अनुभूत वास्तविकता की दूरी टीवी के प्रसंग में कितनी तेजी से घटी है। 2008 का दर्शक तो पूछेगा-‘इसमें अजीब क्या है कि टीवी पति-पत्नी के झगड़े तक का लाइव कवरेज दिखाए?” सच तो यह है कि समकालीन समय मे टीवी और सूचना-तकनीकी की भूमिका को केवल नकारात्मक माना भी नहीं जा सकता। ये चीज़ें मनुष्य के जीवन में इंट्रूयूड तो करती हैं, लेकिन साथ ही सूचना पर सत्ता के एकाधिकार को डिस्टर्ब भी करती हैं। चौबीसों घंटे ताजा खबर देने की झक और टीआरपी की होड़ कुछ चैनलों पर भूत का मोबाइल नंबर दिखवाती है, तो कुछ चैनल सत्तातंत्र को समझने में मदद भी करते हैं। खै़र।
ब्रैडबरी इन छूटों से नाराज तो थे, लेकिन वह बात शायद वे भी समझ गए, जो ‘जलसाघर’ के प्रसंग में सत्यजित राय ने ताराशंकर बैनर्जी को समझाई थी। ‘जलसाघर’ फिल्म देख कर बैनर्जी मोशाय फिल्मकार द्वारा अपनी कथा में लाए परिवर्तनों से खिन्न हुए, ‘ सत्यजीत बाबू यह तो मेरी कहानी नहीं है’। सत्यजीत राय ने छूटते ही कहा, ‘बिल्कुल ठीक कहा आपने- यह मेरी फिल्म है’।
त्रुफो की फिल्म’फारेनहाइट 451′ उस “सुखी” देशकाल की डरावनी खबर ब्रैडबरी के उपन्यास ‘फारेनहाइट 451’ की तुलना में कहीं ज्यादा तीखेपन, कहीं ज्यादा गहरे असर के साथ सुनाती है। ठेठ साइंस-फिक्शन की विधा के लटकों-झटकों से लैस उपन्यास इस राहत, बल्कि लापरवाही की गुंजाइश छोड़ देता है कि डरावना कितना भी हो, यह डिसटोपिया है सुदूर भविष्य का ही। उपन्यास को फिल्म में बदलते हुए त्रुफो ऐसी किसी लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ते। सुदूर भविष्य के डिसटोपिया को त्रुफो हमारे आस-पास की हालत के गर्भ में आकार ले रहे आसन्न भविष्य की फैंटेसी में बदल देते हैं। ऐसी फैंटेसी जो फिल्म बनाए जाने के साल 1966 के बाइस सालों बाद, 2008 में उतनी फैंटेस्टिक भी नहीं लगती।
किताबें जलाने का औपचारिक तंत्र ज़रूर फैंटेसी सा लगता है, लेकिन किसी की “भावनाओं को ठेस” पहुंचाने वाली किताबों के साथ, लेखकों-कलाकारों के साथ जो सलूक विभिन्न विचारों और पहचानों के प्रतिनिधि इन दिनों अपने ही देश में कर रहे हैं, और सत्तातंत्र जिस तरह मजबूर दीख रहा है, उसे ध्यान में रखें, तो किताबें जलाने के औपचारिक तंत्र से भी हम कितनी दूर रह गए हैं? जो लोग हुड़दंगी ढंग से किताबें जलाते हैं, वे चाहें तो फिल्म में दिखाई गयी ‘एफिशिएंसी’ से प्रेरणा भी ले सकते हैं। एक तरह से तो ले ही रहे हैं। आखिरकार सारा हुड़दंग, आहत भावनाओं का सारा कोरस इसीलिए तो है कि अंततः किताबें जलाने के लिए हुड़दंगी ढंग की जरूरत ही न पड़े। किताब से, खुद के सोच-विचार की असामाजिक गतिविधि से लोगों को बचाना, किताबें जलाना व्यवस्था की दक्षता का प्रमाण हो जाए। ‘फारेनहाइट 451’ फैंटेसी की बजाय वास्तविकता बन जाए।
त्रुफो की फैंटेसी हमारे दैनंदिन अनुभवों के निकट आ चुकी है- डरावनी हद तक निकट।
असल में, जो बदलाव त्रुफो ने किए, उनमें से हरेक इस डरावनी निकटता को रेखांकित करता है। उपन्यास में मौजूद परमाणु युद्ध फैंटेसी सा लगता है, लेकिन फिल्म मे बताए गए “पारंपरिक” युद्ध से तो दुनिया एक पल के लिए मुक्त नहीं है। घटनाक्रम किसी अमानवीय ढंग से यांत्रिक और तेज-रफ्तार नगर में नहीं, बल्कि ऐसे नगर में खुलता है, जिसे यूरोप में ‘सिरीन नेबरहुड’ कहा जाएगा। यंत्र जो हैं, वे शायद 1966 में किसी हद तक साइंस-फिक्शन नुमा लगे हों, 2008 में तो हम उनसे कहीं आगे के यंत्र और मंत्र हासिल कर चुके हैं। त्रुफो के उस देशकाल को कंप्यूटर और सेलफोन हासिल नहीं हुए हैं! इस लिहाज से गनीमत है कि हमारे समय के फायरमैन अभी तक फायरमैन ही हैं, बुकबर्नर नहीं।
ब्रैडबरी का उपन्यास विचार-विरोधी सत्ता के रूप में, पाप की जड़ के रूप में टेलीविजन और टेक्नॉलॉजी को ही रेखांकित करता है. जबकि त्रुफो की फिल्म इन दोनों को विचार-विरोधी सामाजिक व्यवस्था के उपकरणों के रूप में पहचानती है। वह व्यवस्था जो अपनी जटिलता और सर्वव्यापी सूक्ष्मता के कारण लोगों के मन मे ‘आभ्यंतरीकृत सेंसर’ का काम तो करती ही है, लोगों का ‘मन-परिवर्तन’ करने में, अपने हिसाब से नया मनुष्य रचने में भी कामयाब हुई है। जाहिर कि तकनीक की तानाशाही से मुक्ति महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन अपने-आप में सिर्फ यह मुक्ति ही विचार-विरोधी, संवेदनहीन जीवन-पद्धति से भी मुक्ति सिद्ध हो- ऐसा कुछ नहीं है।
त्रुफो ने एक बदलाव और किया है। बेहद मानीखेज, सांस्कृतिक आशयों से संपन्न बदलाव। इस बदलाव की चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा।
‘फारेनहाइट-451’ की तुलना यदि 1984 से करें तो, जॉर्ज ऑरवेल के डिसटोपिया में ‘बिग ब्रदर’ के दर्शन भले न हों, लेकिन उसकी आवाज़ सारे आख्यान पर छाई हुई है। वह अदृश्य है, लेकिन अनुपस्थित नहीं। अदृश्य रहते हुए भी वह सदा उपस्थित( सामने बैठा!) है। ‘फारेनहाइट 451’ की विचार-विरोधी, मानव-चेतना विरोधी समाज-सत्ता इस अर्थ तक में उपस्थित नहीं है। उसे ‘सामने’ -बाहर होने की जरूरत ही नहीं। दिखने की तो क्या, उसे ‘बिग ब्रदर’ की तरह बोलने की भी जरूरत नहीं। वह तो लोगों की चेतना के भीतर पैबस्त हो चुकी है। वह उपस्थित( सामने बैठी) नहीं, वह इस भयानक डिसटोपिया में ईश्वर की तरह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। एक रोचक बात यह भी है कि ऑरवेल के विपरीत ब्रैडबरी ने अपने डिसटोपिया को किसी खास सन-संवत से नहीं जोड़ा है, हालांकि एक जगह यह अहसास ज़रूर होता है कि घटनाक्रम 1990 के बाद किसी वक्त का है। आपके अनुभूत वर्तमान से निकटता को रेखांकित करने को उत्सुक त्रुफो, फिल्म में वर्णित समय के किसी विशेष वर्ष या दशक में होने का ऐसा कोई अहसास तक नहीं होने देते।
दिलचस्प संयोग ही है कि त्रुफो का निधन 1984 में हुआ!
फिल्म शुरु होती है-फायर स्टेशन की गतिविधि से। किसी आपदा से निबटने के लिए जैसे उन्हें निकलना चाहिए, उसी तत्परता से फायरमैन उर्फ बुकबर्नर निकल पड़े हैं। किसी क़ानूनप्रिय नागरिक ने किसी असामाजिक तत्व के हाथ में किताब देख ली है- उसकी खबर लेना, किताब को जला देना-फायरमैन का काम यही तो है। इसी के लिए वे तत्परता से निकल पड़े हैं। फायरमैन गाय मोंटाग भी दूसरे फायरमैनों की तरह पुस्तक-दहन में दक्ष है, और अपनी पत्नी मिल्ड्रेड और अपने टीवी के साथ ‘सुखी’ भी। उसके ‘सुख’ में बाधक प्रश्नचिन्ह बन जाती है, नयी पड़ोसन क्लैरिस से मुलाकात। उससे बात करना जैसे एक और प्रोग्राम्ड मशीन, याने एक और ‘सुखी’ नागरिक से बात करना नहीं है। क्लैरिस उन ‘असामाजिक तत्वों’ में से है, जिन्होंने किताबों से वास्ता बनाए रखा है। हालाँकि यह बात अभी मोंटाग को मालूम नहीं पड़ी है। अभी तो वह क्लैरिस के अजीब से अलगपन की ऊष्मा से ही रोमांचित भी है, और कन्फ्यूज्ड भी।
मोंटाग की पत्नी मिल्ड्रेड सुख के सभी साधनों के बावजूद ऊब और डिप्रेसन से परेशान है। वह सचमुच आदर्श नागरिक है, किताबों से कोई वास्ता नहीं उसका, व्यवस्था के बारे में गलत ढंग से सोचने के पाप से कायिक-वाचिक-मानसिक हर धरातल पर मुक्त है, लेकिन फिर भी परेशान है। क्लैरिस से मिल कर लौटा मोंटाग मिल्ड्रेड को अचेत पाता है-उसने नींद की बहुत सी गोलियां खा ली हैं। अस्पताल से ‘डॉक्टर’ आते हैं, उनका रवैया मिल्ड्रेड के प्रति वैसा ही है, जैसा किसी कार-मैकेनिक का कार के प्रति हो सकता है। वे मिल्ड्रेड के शरीर का सारा ही रक्त बात की बात में बदल देते हैं, सोचिए ज़रा उस समाज द्वारा अर्जित वैज्ञानिक दक्षता के बारे में। घर बैठे सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन- जैसे कोई इंजेक्शन लगाने का काम हो। और यह काम होता है, उसी लहजे और मुहावरे में, जैसे किसी वर्कशॉप में कार की भीतरी-बाहरी सफाई हो रही हो। जो ‘डॉक्टर’ आए हैं, उनकी दक्षता का क्या कहना- लेकिन मिल्ड्रेड के प्रति संवेदना और मोंटाग के लिए सांत्वना?
क्या होती हैं ये चीज़ें? पिछड़ेपन की ऐसी निशानियां तो उस “सुखी” समाज ने कब की भुला दी हैं। मोंटाग भी भुला चुका था, लेकिन आज उस अजीब सी स्त्री से मिल कर आया है वह-उसे पहली बार ‘हैल्थ टेकनीशियनों’ का व्यवहार अजीब लगता हैः आज से उसकी नयी यात्रा आरंभ होती है।
इस यात्रा का सबसे मार्मिक पड़ाव जल्दी ही आ जाता है।
मोंटाग उस टीम में है, जो किसी बूढ़ी औरत के घर किताबें जलाने पहुंची है। यह पॉलिटिकली इनकरेक्ट औरत दूसरे पुस्तक-प्रेमियों से कुछ अलग है। वह किताबें जलाने का जबर्दस्त प्रतिरोध करती है। घर और किताबें फायर-ब्रिगेड के हवाले कर चुपचाप किताबों को जलती देखने की बजाय वह आत्मदाह कर लेती है। किताबों के पहले खुद ही जल जाती है।
मोंटाग अवसन्न है। किताबों के लिए शहीद हुई उस औरत की किताबों में से एक किताब उसने ‘चुरा’ ली है। अब उसकी और उसके समाज की जिन्दगी के बीच असाध्य मिसमैच अनिवार्य है। उसे जानना ही है कि फालतू के किस्से-कहानी और कविताओं की किताबों में ऐसा क्या होता है कि कोई उन्हें जलाने का विरोध करने के लिए स्वयं को जला ले। अब किताबें चुराना, उन्हें पढ़ने-समझने की विधियां तलाशना मोंटाग की आदत बन चली है। कोई साल भर के अरसे में वह अनेक किताबें चुरा कर घर में छिपा लेता है। और यहाँ से आख्यान इस बात का रेखांकन आरंभ कर देता है कि सभी किताबें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किताबों की दुनिया में भी, सीधा-सादा ‘ज्ञान’ देने की बजाय अजीब सी बातें करने वाले सर्जनात्मक साहित्य की अपनी खास जगह है। आखिरकार कुछ ऐसी बेतुकी बात पढ़ कर ही तो उसे किताबों में दिलचस्पी हुई थी कि, ” वक्त सो गया है, दोपहर की धूप में”। इस पंक्ति पर मोंटाग की नज़र उस औरत के घर में ही पड़ी थी, जो अपनी किताबों के साथ खुद भी जल मरी।
मोंटाग और दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, इसी से जाहिर है कि उस देशकाल को “निरक्षर” की बजाय, साहित्य-विरोधी कहना अधिक उपयुक्त है। जीवन जीने के लिए अक्षर-ज्ञान और ‘व्यवहारिक’ ज्ञान तो चाहिए ही। तकनीकी कौशल के लिए विज्ञान तो पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन साहित्य? कला? इतिहास? दर्शन? नागरिकों की बुद्धि भ्रष्ट करने वाले असली खलनायक तो ये हैं- और इनमें भी सबसे ज़्यादा- साहित्य!
हमारे अपने समय का सत्तातंत्र सूचना-माध्यमों में, विश्वविद्यालयों में, अन्य प्रतिष्ठानों में साहित्य को क्या हैसियत देता है? यह सवाल और इसका जवाब याद करते हुए देखें तो, एक बार फिर, ‘फारेनहाइट 451’ सुदूर भविष्य की फैंटेसी कम, और समकालीन यथार्थ की कल्पसृष्टि अधिक लगने लगती है। ख़ैर।
अब मोंटाग का वास्ता ऐसी कितनी ही पंक्तियों से पड़ता है, कैसे समझे इनका मतलब? कैसे बात करे क्लैरिस से इनके बारे में? किताब साथ लेकर बतियाने बैठना तो अकल्पनीय है, तो? किताब को याद कर लेने के सिवाय क्या किया जा सकता है? मोंटाग कोशिश करता है कि किताबों को अपनी यादों में सदा के लिए बसा ले। कलैरिस के अलावा वह अब फेबर के संपर्क में आता है, जो गुजर चुके गए-गुजरे ज़माने में साहित्य का प्रोफेसर हुआ करता था। उसके लिए अब मोंटाग को साहित्य पढ़ाना और मोंटाग का पढ़ना आस्था का अनुष्ठान बन जाता है। मोंटाग अब समाज-विरोधी तत्वों की जमात में बाकायदा शुमार है। किताबें, खासकर साहित्य की किताबें पढ़ना; क्लैरिस और फेबर के साथ उनके बारे में बात करना अब लाइलाज आदत है।
और आदत छुपी कहाँ रहती है? फायर चीफ कप्तान बीयट्टी स्वयं मोंटाग को समझाता है। सभी फायरमैन किताबें चुराते हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रति उत्सुकता स्वाभाविक ही ठहरी। लेकिन एकाध बार किताब चुरा कर पढ़ लेना और बात है, इसकी आदत ही डाल लेना और बात। किताबों को बचाने की कोशिश करना तो अक्षम्य समाज-द्रोह है ही। जैसे दूसरे फायरमैन किताबें जलाने के लिए लौटा देते हैं, वैसा ही मोंटाग को भी करना चाहिए। किताबें वाकई खतरनाक हैं, क्योंकि जो कुछ एक किताब कहती है, दूसरी उसे काट देती है। जीवन जीने की कोई स्पष्ट, निर्भ्रांत लाइन देने के स्थान पर वे मनुष्य को बिगूचन में डालती हैं। इसीलिए सत्ता ने कृपा करके लोगों को बिगूचन से बचा लिया, और साफ-साफ लाइन बता दी कि जीवन कैसे जिया जाए।
मोंटाग को क्या अधिकार है कि वह असामाजिक तत्वों के साथ मिल कर, आराम से चल रही इस व्यवस्था में फिर से बिगूचन पैदा करे?
व्यवस्था इस कदर ‘सामाजिक’ है कि मोंटाग से मनुष्य ही नहीं मशीनें भी असुविधा अनुभव करने लगती हैं। मनुष्य-मशीन के बीच आदर्श सहयोग पर टिके उस समाज में ऐसा तो होना ही चाहिए। घर का दरवाज़ा जो पैरों की आहट से ही खुलने के लिए प्रोग्राम्ड है, अब मोंटाग के लिए नहीं खुलता। उसने दरवाज़े के साथ अपने संबंध की पहली शर्त की उपेक्षा कर किताबों से रिश्ता बनाया है, अब दरवाजा कैसे उसका स्वागत करे?
मोंटाग से असुविधा दरवाजे को ही नहीं, पत्नी मिल्ड्रेड को भी है। आखिरकार, अपने सारे डिप्रेसन के बावजूद वह व्यवस्था के प्रति अटूट आस्था से संपन्न, पॉलिटिकली करेक्ट नागरिक है। मोंटाग ने फायर-चीफ बीयट्टी को किसी तरह यकीन दिला दिया था कि, जो किताबें वह फायर-स्टेशन में जमा नहीं कर पाया, उनका उपचार उसने स्वयं ही कर दिया है। वह यह देख, बल्कि सुन कर भी चकित है कि स्वयं बीयट्टी ने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, ताकि उनके ख़तरों से मोंटाग जैसों को आगाह कर सके। मिल्ड्रेड ने बीयट्टी को असलियत बता रखी है, मोंटाग के (और उसके अपने) घर में किताबें छुपाने के ठिकानों समेत। एक दिन फायरमैन अपना काम करने निकलते हैं, ‘निशाने’ तक पहुंच कर ही मोंटाग को मालूम पड़ता है कि इस बार निशाने पर उसका अपना घर है। मिल्ड्रेड अपना नागरिक दायित्व निभा कर, समाज-विरोधी मोंटाग को छोड़ कर जा चुकी है। क्रोध से पागल, मोंटाग न सिर्फ किताबें, बल्कि घर की तमाम चीज़ें, सारा घर जलाने पर उतारू है। उसे अपना यह सामाजिक अस्तित्व ही जला डालना है।
बीयट्टी को अब मोंटाग के साथियों की- फेबर और क्लैरिस- की तलाश है। वह उन्हें कानून के हवाले करने पर आमादा है, और अपने आमादापन को इतनी जिद के साथ मोंटाग के सामने जताता है कि मोंटाग उसे उसी तरह फायरपाइप से जला देता है, जिस तरह उन दोनों ने न जाने कितनी किताबें जलाईं हैं।
मोंटाग को जान-बूझ कर ताव दिलाता बीयट्टी कहीं खुद ही तो अपनी जिंदगी से नजात पाना नहीं चाहता? कहीं खतरनाक किताबों ने खुद उसके दिमाग पर भी तो असर नहीं कर दिया? कहीं वह भी तो सुखदायी व्यवस्था के डरावनेपन को समझने तो नहीं लगा? इस हद तक कि व्यवस्था से ही नहीं जीवन मात्र से पलायन में ही मुक्ति है, और स्वयं इस मुक्ति तक पहुंचने का साहस नहीं, सो मोंटाग को माध्यम बनाया जाए।
नैरेशन इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता। दे भी क्यों? अनुत्तरित रह कर ये प्रश्न दर्शक के साथ ज़्यादा देर तक, और ज़्यादा मतलब के होकर रहते हैं।
अब मोंटाग को भागना है। उस समांतर, भूमिगत पुस्तक-प्रेमी समुदाय की ओर-जिसके बारे में वह क्लैरिस और फेबर से सुनता रहा है। मोंटाग भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है, और साथ में हैं इस सारे घटना-क्रम का लाइव टेलीकास्ट करते कैमरे। क्लैरिस उसके साथ है, फेबर मारा जा चुका है। आखिरकार ये दोनों पुलिस और टीवी को चकमा देकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। पुस्तक-प्रेमियों का समुदाय। इनमें से कुछ ‘ऑफिशियल समाज’ के लिए सपरिवार गायब-मिसिंग- हैं; तो कुछ अपने पॉलिटिकली करेक्ट परिजनों से भी लुक-छिप कर यहां तक पहुंचे हैं।
इन लोगों ने ‘फारेनहाइट 451’ के ताप से पुस्तकों को बचाने की अद्भुत विधि खोज निकाली है। स्मृति को सायास ध्वस्त करने पर उतारू उस समाज में इन लोगों ने स्मृति को बचाने का सचेतन और व्यवस्थित आयोजन किया है। किताबें ये भी जला देते हैं, क्योंकि खुदा-ना-खास्ता कभी पकड़ लिए गए और बस्ती में एक भी किताब बरामद हो गयी तो किसी बस्ती वाले की ख़ैर नहीं।
ये किताबें जला देते हैं, लेकिन उन्हें स्मृति में सुरक्षित कर लेने के बाद। हरेक किसी न किसी किताब को कंठस्थ किए हुए है। अब ये किताबें ही उनकी पहचान हैं। ये ही उनमें से हरेक का परिचय हैं। मोंटाग को उनका परिचय इसी तरह दिया जाता है-‘देखो. ये हैं श्री ‘ए टेल ऑफ टू सिटीज’ और इनसे मिलो,ये हैं श्री डेविड कॉपरफील्ड। वह प्यारी सी बच्ची है ‘एलिस इन वंडरलैंड’ और वह रही, ‘प्राइड ऐंड प्रेज्युडिस’। अपने में मस्त उन सज्जन का नाम है, ‘क्रिटीक ऑफ प्योर रीज़न’ और वे बूढ़े बाबा हैं ‘ वार ऐंड पीस’।
इस समुदाय में रहने की विधि यही है। जो किताब मोंटाग बचा लाया है, उसके लिए कुछ कु्रबानी दे- अपनी पहचान की कुरबानी। त्याग दे अपना नाम- अपनाए उस किताब का नाम। बदल दे अपने जीवन को किताब के जीवन में। किताब को तो जलाया ही जाना है, लेकिन उसे जीवित रखना होगा स्मृति में। किताब का भौतिक अस्तित्व तभी तक के लिए संभव है, जब तक कि मोंटाग उसे कंठस्थ न कर ले। मोंटाग जब उस किताब में बदल जाएगा तब, जिसे उस किताब से संवाद करना होगा-वह मोंटाग के पास आएगा, और मोंटाग का कर्तव्य होगा कि उस व्यक्ति को किताब सुनाए। स्मृति का श्रुतिदान करे।
मोंटाग स्मृति और श्रुति के इस अनुष्ठान का श्रीगणेश कर देता है। और जैसे ही आप ध्यान देते हैं कि जान हथेली पर रख कर भागते समय जो किताब बचा लाया था, वह किताब उपन्यास में बाइबिल है, लेकिन फिल्म में बाइबिल नहीं है, वैसे ही उपन्यास और फिल्म का वह फ़र्क, त्रुफो द्वारा लाया गया वह बदलाव स्पष्ट होने लगता है, जिसे मैंने इस निबंध के आरंभ में बेहद मानीखेज, सांस्कृतिक आशयों से संपन्न बदलाव कहा था।
ब्रैडबरी के मोंटाग के लिए बाइबिल उस आस्था को धारण करती है, जिसे उपभोक्तावादी समाज के बीच बचा कर रखना है। स्पष्ट है कि त्रुफो के लिए बाइबिल आस्था को धारण करने वाली पुस्तक नहीं है। फिल्म में मोंटाग कास्पर हाउज़र के बारे में लिखी गयी किसी किताब को साथ लेकर पुस्तक-प्रेमी समुदाय में पहुंचता है। त्रुफो सचेत रूप से न केवल बाइबिल के आस्थापरक आशयों से बच रहे हैं, बल्कि बाइबिल जैसी विशिष्ट पुस्तक के जीवन जैसा ही महत्वपूर्ण पुस्तक मात्र के जीवन को मान रहे हैं।
मैं कह नहीं सकता कि इस बदलाव के बृहत्तर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आशयों के प्रति सजगता के साथ त्रुफो यह बदलाव लाए या नहीं। लेकिन, इन आशयों का उस दर्शक के चित्त में कौंधना लाजिमी है, जिसे यूरोप के इतिहास में जिज्ञासा और सर्जनात्मकता के साथ चर्च ( केवल कैथॉलिक ही नहीं, प्रोटेस्टेंट चर्च भी) के रवैये का इतिहास मालूम हो।
पुस्तक-दहन के विशिष्ट प्रसंग में ही कुछ मार्मिक प्रसंग याद करें, तो 1533 में मिशेल सर्वेंतीस नामक लेखक को यह अनूठा सम्मान हासिल हुआ कि जेनेवा के प्रोटेस्टेंटों ने तो उन्हें और उनकी किताबों को जिन्दा जला दिया, और फ्रांस के कैथॉलिकों को उनका पुतला जला कर ही संतोष करना पड़ा। कैथॉलिक चर्च विडंबनापूर्ण ढंग से पुस्तकों के जीवन का नोटिस लेता था। किताबें जलाने का, और विरोधियों-हेरेटिक्स- को फांसी लटकाने का काम जल्लाद ही करते थे। चर्च द्वारा निर्मित आस्था के नगर में किताब को जलाना जैसे पापी को मृत्युदंड देना ही था। दोनों काम उसी सलीके और सक्षमता के साथ किए जाते थे, जिस तरह ‘फारेनहाइट 451’ के सुखी नगर में। रोम के पारंपरिक विश्वासों को जिस दौर में नवगठित चर्च कुचल रहा था, उस दौर में ऑरेटर लैबीनस ने अपनी किताबों को दाह की सजा सुनाए जाने पर आत्महत्या कर ली थी। और यह सुन कर एक अन्य ऑरेटर कैसियस सेवेरस ने कहा था कि ‘मुझे भी जला दो, क्योंकि मुझे लैबीनस की सभी किताबें कंठस्थ हैं’।
पता नहीं, बाइबिल की जगह दूसरी किताब को फिल्म में लाते हुए त्रुफो के दिमाग में यह सब था या नहीं, लेकिन किताबें जलाते समाज में किताबों को कंठस्थ कर उन्हें जल्लादों से बचाने का प्रयत्न करते लोगों को देखते हुए, जानकार दर्शक के दिमाग में तो यह सब आएगा। उसी तरह, जैसे कि बुल्गाकोव की बात( मुश्किल से जलता है वह कागज, जिस पर कुछ लिखा हो) सुन कर दूसरी सदी के विद्वान बेन जोसेफ अकीबा की बात याद आएगी- ” काग़ज़ भले जल जाए, शब्द तो उड़ कर कहीं और पहुंच जाते हैं”।
“उड़ कर”, देशकाल की सीमाएं लांघ कर कहीं से कहीं पहुंच जाने की जो अजब जिद और ताकत सर्जनात्मक शब्द को हासिल है, उसके कारण ही तो ऐसे शब्द से वे डरते हैं, जिन का दावा है- सत्य पर एकाधिकार का- और जिन्हें यह एकाधिकार या तो स्वयं ईश्वर ने दिया है, या स्वयं इतिहास ने!
संगठित धर्म हों या दुनिया बदलने के दावे करने वाली विचारधाराएं- मनुष्य की स्मृति को दोनों नियंत्रित और दूषित करना चाहते हैं। चिंतन की, और चिंतन संभव करने वाली संस्थाओं की स्वायत्तता दोनों की दृष्टि में महापाप है।
चिंतन पर चर्च के अत्याचारों की जो स्मृतियां यूरोप के बौद्धिक अवचेतन में मौजूद हैं, उन्हें देखते हुए, बाइबिल की जगह किसी और किताब को रेखांकित करने का, त्रुफो का फैसला सोचा-समझा हो, चाहे संयोगवश, है सांकेतिक और महत्वपूर्ण।
सबसे सांकेतिक और मार्मिक है, फिल्म के अंतिम पलों का वह दृश्य, जिसमें अंत समय निकट आया जान एक वृद्ध अपनी स्मृति में सुरक्षित ‘ओडेसी’ की श्रुति किसी बच्चे को दे रहा है। वह वृद्ध अब और नहीं रहेगा, लेकिन ‘ओडेसी’ रहेगी- वह बूढ़े की जीर्ण काया से नयी देह में संतरित हो रही है। उस भयानक देशकाल में स्मृति को श्रुति के सहारे बचाया जा रहा है। बूढ़े श्री ओडेसी तो गुजर गए, लेकिन वो देखिए, वे रहे हमारे नए श्री ओडेसी। अक्षर को अक्षर स्मृति और श्रुति ही बनाती हैं।
फिल्म देखी थी, लिंडा हेस के घर। बीस दिसंबर 2004 को। उस अमेरिका यात्रा का यह अंतिम दिन था। दूसरे दिन एयरपोर्ट के लिए निकले, तो रास्ते में दिखा- फायर स्टेशन। हम एक दूसरे को देख कर मुस्करा पड़े, ‘कम से कम अभी तक तो फायर-ब्रिगेड का काम किताबें जलाना नहीं, आग बुझाना ही है!
लेकिन कब तक? कितनी दूर हैं हम दक्षता के साथ किताबें जलाने वाले देशकाल से? पता नहीं।
लेकिन वह वृद्ध याद है न जो उस डिसटोपिया के समांतर ही जीवित उस पुस्तक-प्रेमी यूटोपिया में अपनी स्मृति में सुरक्षित पुस्तक का श्रुतिदान भविष्य को कर रहा था। उम्मीद करें कि ऐसी विधियां हमें याद रहेंगी, उम्मीद करें कि कुछ और विधियां सूझेंगी भी।
डिसटोपिया का यह आख्यान उस के ही गर्भ में पल रहे यूटोपिया के बयान के साथ समाप्त होता है।
डर के बावजूद, उम्मीद के साथ।