अकथ कहानी प्रेम कीः पुरूषोत्तम अग्रवाल
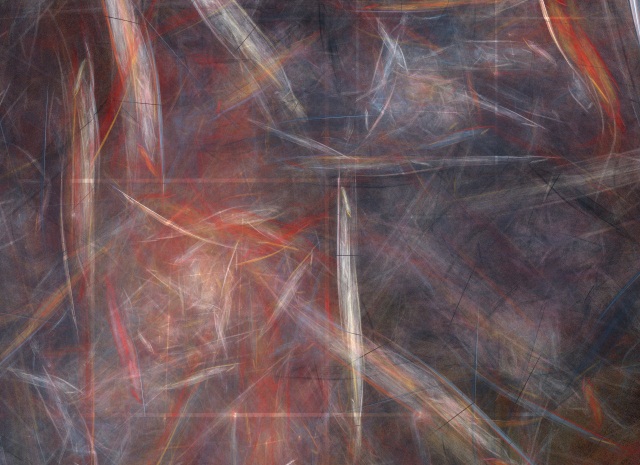
कबीर के प्रसंग में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है, वह है उन्हें कवि मानने में सर्वव्यापी संकोच। लिंडा हैस्स ने जरूर कबीर को प्राथमिक रूप से कवि मानते हुए विचार किया है; बाकी अध्येता कबीर की व्यंग्य-प्रतिभा की प्रखरता मानते हुए भी, कबीर को ‘वाणी का डिक्टेटर’ मानते हुए भी, उनके कवित्व को स्वीकारने में संकोच बरतते हैं। शुक्लजी का साफ कहना था ही, कि कबीर की बानी ‘उपदेश देती है, भावोन्मेष नहीं करती’ ; द्विवेदीजी के अनुसार भी कबीर चूंकि ‘धर्मगुरु थे, इसलिए उनकी वाणी का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होना चाहिए’।
धर्मगुरु की वाणी का काम उपदेश करना ही होता है, भावोन्मेष कहीं-कहीं हो जाए तो सोने पर सुहागा, धर्मगुरु की वाणी को सुना तो आध्यात्मिक उपदेश के लिए ही जाता है। बाकी आलोचक भी घुमा-फिरा कर कहते यही हैं कि, ‘ और जो हों, धर्मगुरु, धर्म-प्रवर्तक, क्रांतिकारी, समाज-सुधारक; कबीर कवि तो नहीं ही हैं’। उन तक हमें जाना तो उपदेश की उम्मीद में ही चाहिए। उपदेश अध्यात्म-विद्या का हो, या क्रांति-विद्या का, है तो उपदेश ही; कबीर चाहें ‘जोग’ की जुगति सिखाएं, चाहे क्रांति की, हैं तो उपदेशक ही।
संकोच स्वयं कवि को भी है। चेतावनी देते हैं —‘तुम जिन जानौ यह गीत है, यह तो निज ब्रह्मविचार रे’।
जाहिर है कि कबीर कवियशःप्रार्थी निश्चय ही नहीं थे। तो, हम क्या केवल कवियशःप्रार्थियों को ही कवि मानें ? यदि हाँ, तो कबीर को मानें, ना मानें, तुक बाँध कर चुटकुले सुनाने वालों को तो कवि मानना ही पड़ेगा। शब्द की कौन सी साधना कोरा उपदेश देती है, और कौन सी भावोन्मेष करके स्वयं को कविता साबित करती है—यह तय करने का एक ही तरीका है, कवि की बजाय कविता की बात सुनना। कवि की घोषणा पर नहीं, उसकी शब्द-रचना पर भरोसा करना।
ऐसा करते ही आप देखेंगे कि कबीर की कविता कितना गहरा भावोन्मेष करती है। वह मजबूरी भी देखेंगे, जो उपदेशक नहीं, कवि के सामने आती है। कबीर निर्गुण-निराकार के साधक थे। ऐसी क्या मजबूरी है कि वे निर्गुण को माता-पिता और स्वामी के गुण देते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि वे निराकार को कभी तड़पाने वाले, तो कभी बारात लेकर आने वाले बालम का आकार देते हैं? मजबूरी यह है कि कबीर मूलतः कवि हैं, और बिना रूपासक्ति के कोई कवि नहीं होता। निराकार उपासना का विषय हो सकता है, लेकिन प्रेम तो किसी मूर्त रूप से ही किया जा सकता है। ‘बुतपरस्ती’ को कुफ्र और ‘बुतशिकनी’ को सबाब बताने वाले इस्लाम के सांस्कृतिक परिवेश में, कविगण रूपासक्ति—बुतपरस्ती—के जरिए, भावोन्मेष करने के साथ-साथ धर्मशास्त्रीय सोच से जिरह भी करते रहे हैं:
काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की
गो वाँ नहीं हैं, वाँ के निकाले हुए तो हैं।
कबीर का स्वभाव और भाषिक व्यवहार कवि का है। इस स्वभाव को भुलाकर ही उन पर ‘उद्धत’ और ‘अक्खड़’ जैसे विशेषण चस्पा किए गए हैं। बात शुरु ही होती है, कवि को उपदेशक या समाज-सुधारक मान कर। ऐसा मानकर इस बात पर प्रकट या अप्रकट रूप से खेद व्यक्त किया जाता है कि बात करने की उनकी विधि सुधार-भावना के अनुकूल नहीं है। या फिर, यह तो याद रखा जाता है कि ‘कटुक वचन कबीर के, सुनत आग लग जाए’; लेकिन यह भुला दिया जाता है कि ‘घट-घट में तेरा सांई बसता, कटुक वचन मत बोल रे’। कुछ लोग मान कर चलते हैं कि समाज-सुधारक को कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिएं, दूसरी तरफ, कुछ लोगों के हिसाब से, बिना कड़वाहट के भला कोई क्रांतिकारी हो सकता है!
कवि के भाषिक व्यवहार में, न तो कटुक वचन अनपेक्षित हैं, न ऐसे कटुक वचन बोलने से अपने आप को बरजना।
‘काम मिलावे राम सूं’ कहने वाली कविता प्रेम के ‘लौकिक-अलौकिक’ विभाजन को व्यर्थ बना देती है। याद दिलाती है कि लौकिक प्रेम ही अलौकिक अनुभवों, आकांक्षाओं और अनुष्ठानों को अर्थ देता है। प्रेमभावना ही जटिल ‘रहस्य-साधना’ को भी संभव करती है और उसकी अभिव्यक्ति को भी।
कबीर और अन्य निर्गुण संतों की गोष्ठियां प्रसिद्ध हैं। कबीर की कविता पढ़ते हुए, उनके और ‘अपरंपार पार परसोतम’ के बीच ऐसी ही गोष्ठी की कल्पना मन में आती है। कबीर ने कहा होगा, अपने राम से, कौन जाने, ‘पीछे-पीछे फिरने’ वाले राम ने ही कबीर से कहा होः “ प्रेम और विवेक- इन दो शक्तियों के रूप में आप मेरे भीतर विद्यमान हैं। घोर बिगूचन ( कंफ्यूजन) के, अकेले पलों में, जोर से आंखें मींच कर आपका नाम लेता हूं/ लेती हूं, और बस सारा बिगूचन बिलाय जाता है। प्रेम और विवेक के दीपक बाहर-भीतर उजियारा कर देते हैं”।
प्रेम अपने विस्तार में जीवनदाता है, और गहराई में जानलेवा। प्रेम सहज संभव भी है, और सर्वथा अप्राप्य भी। इस अप्राप्य का विरह जिस ‘घट’ में ‘संचरता’ है, उसकी आंखों से पानी नहीं, लहू के आंसू गिरते हैं:
सोई आंसू साजना, सोई लोक बिड़ांहि।
जौ लोइन लोही चुवै तौ जांनौ हेत हियांहि।
यह साखी हमारी स्मृति को इलहामों और उपदेशों की ओर नहीं, एक और बड़े कवि की ओर ले जाती हैः
रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काइल
जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है।
जैसे प्रेम और रूपासक्ति के बिना कोई कवि नहीं होता, वैसे ही मृत्यु से टकराए बिना भी कोई कवि नहीं होता। प्रेम और मृत्यु जीवन के भी प्राथमिक और अंतिम सत्य हैं, और कविता के भी। कबीर की काव्य-संवेदना में मृत्यु निषिद्ध विषय नहीं है। वे जैसी मार्मिकता से प्रेम के उल्लास और दर्द को कहते हैं, समाज के सत्य को बखानते हैं, वैसे ही जीवन के अटल, अंतिम सत्य को भीः
यह जग अंधला, जैसी अंधी गाई।
बछा था सो मर गया, ऊभी चाम चटाई।
संसार की नश्वरता इस साखी का कथ्य जरूर है, लेकिन दिल हिला देने वाला भावोन्मेष करता हैः मरे बछड़े को चाटती गाय का बिंब।
कबीर की चेतना में,प्रेम, मृत्यु और समाज एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। कबीर की काव्य-संवेदना रामभावना, कामभावना और समाजभावना को एक साथ धारण करती है। इन तीनों के सर्जनात्मक सह-अस्तित्व को, समग्रता में पढ़े बिना, कबीर को पढ़ने के दावे व्यर्थ हैं।
कबीर जागने-रोने के कवि तो हैं ही, देखने और हँसने के कवि भी हैं। उलटबांसियों का संबंध सिद्धों की संधाभाषा से जोड़ा गया है, लेकिन ‘गूढ़-गंभीर’ व्याख्याओं का मोह छोड़ कर आप, यदि इन्हें सहज रूप से पढ़ें तो निश्चय ही पहली प्रतिक्रया बेतुकेपन पर हँसने की होगी—जैसे लिंडा हैस्स और उन्हें उलटबाँसियां समझाने वाले दादा सीताराम की हुई थी। यदि कबीर के समय के साथ-साथ अपना समय भी याद करते रहें, तो, उलटबांसियों में झलकने वाले ‘उनके वक्त के’ बेतुकेपन पर हँसने के साथ अपने वक्त के बेतुकेपन का चेहरा भी जैसे आईने में नजर आएगा। भाषा के सामान्य अर्थ-बोध को जानबूझ कर ‘उलटती’ ये कविताएं कबीर के अपने समय के पाठक/ श्रोता के साथ ही परवर्तियों को भी अवसर देती हैं कि वे अपने-अपने वक्तों के बेतुकेपन को पहचान सकें।
[…]
कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी राज की स्थापना के पहले का भारत धरा पर स्वर्ग समान था। हमारी हर समस्या विदेशियों की देन है। दूसरे शब्दों में, अपनी समस्याएं हल तो हम क्या करेंगे, इतनी भी सामर्थ्य परमात्मा ने भारतीयों को नहीं दी है कि अपने लिए कुछ समस्याएं खुद ही पैदा कर सकें।
दूसरी ओर, कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी राज आया तो मुक्ति आई, आधुनिकता आई, वरना तो भारतीय समाज जैसे बर्फ में जमा हुआ था। अंग्रेजी राज के पहले, भारतीय जन-जीवन में, अत्याचारों और तर्कविहीन परंपराओं के अंधानुगमन के सिवाय, था क्या?
परस्पर विरोधी दिखने वाले ये मूल्यांकन असल में एक ही जमीन पर खड़े हैं। वह जमीन है— औपनिवेशिक ज्ञानकांड की जमीन। यह ज्ञानकांड भारतीय समाज का ‘वस्तुनिष्ठ अध्ययन’ नहीं बल्कि समाज के परंपरा-बोध और दैनंदिन जीवन में मूलगामी और दूरगामी तोड़-फोड़ कर रहा था। इस में अंतर्निहित थी—यूरोपीय आधुनिकता की अहम्मन्यता और साम्राज्यवाद की क्रूरता।
इस हस्तक्षेप के इतिहास और परिणामों का बोध प्राप्त किए बिना, कबीर के समय के भारत का प्रामाणिक बोध प्राप्त करना असंभव है। ऐसा प्रामाणिक बोध प्राप्त करने की पहली शर्त्त हैः देशभाषा के स्रोतों से गहराई के साथ गुजरना और समाज के दैनंदिन व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना।
कबीर को ‘पढ़ने’ के लिए, एक तरफ देशज मनीषा को,और दूसरी तरफ औपनिवेशिक हस्तक्षेप को ‘पढ़ना’ अनिवार्य है—यह अहसास मुझे निरंतर चलती आ रही जिज्ञासा-यात्रा के दौरान ही प्राप्त हुआ है। कबीर से मेरा क्या नाता है—यह भी इसी यात्रा में समझ आया।
नवलदास से मिलना इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था।
दस बरस बीत चले। सन निन्यानवे के दिसंबर में, बनारस में नवलदास जी से भेंट हुई थी। जाति के कुरमी, ये बुजुर्ग ‘पारखमार्ग’ पर चलने वाले कबीरपंथी थे। संस्कृत और अंग्रेज़ी दोनों से अनभिज्ञ होने के कारण, हिन्दी भी बस पढ़ ही सकने के कारण, “पढ़े-लिखे” लोगों के मुहावरे में नवलदास “अनपढ़” कहे जाएँगे। ठीक उसी तरह, जैसे उनके “ज्ञानीजी” को – कबीर को- को “पढ़े-लिखे” लोग “अनपढ़” कहते आए हैं। उन्होंने कबीर-बानी की जिस तरह व्याख्या की, उससे एकाएक लगा, “ अरे! ये तो वैसी ही बातें कर रहे हैं, जैसी मुझे बचपन में सूझा करती थीं”। उन दिनों, जब सहज-बोध तरह-तरह के शास्त्र-ज्ञान और विमर्शों से आच्छादित नहीं हुआ था, मुझे भी तो लगता था: “ जो कुछ है, भीतर या बाहर, संसार भर में, सब एक अखंड का ही पसारा है। इस अनादि-अनंत जगत के परे कौन परमात्मा हो सकता है? कहाँ हो सकता है?”
सर्वव्यापी,अखंड चेतन का बोध मनुष्य मात्र का जन्मजात बोध है। जीव ही चैतन्य है, और वही व्याप्त है सारे ब्रह्मांड में। इसे “जानने” के लिए कहीं “बाहर” जाने की ज़रूरत नहीं। इस व्याप्ति को बखानने के लिए ब्रह्म, ईश्वर, निर्गुण या राम जैसे नाम देने पड़ते हैं- यही नाम की महिमा है।जीव चैतन्य की बेकली को कहने के प्रयत्न में ; जो कही नहीं जा सकती, उस अकथ कहानी को कहने की जिद में ही वाणी की सार्थकता है। इस सार्थकता का ही नाम कविता है।
ऐसा ही सहजात बोध है, मनुष्य-मात्र की समता का। जन्म से न कोई ऊँचा होता है, न कोई नीचा। न्याय की कामना इस सहज समता-बोध की ही परिणति है। केवल अपने या अपने जैसे लोगों के लिए ही नहीं, सबके लिए न्याय। चैतन्य की ब्रह्मांड –व्याप्ति के बोध को ‘आध्यात्मिक’ और समता-बोध और न्याय-कामना को ‘सामाजिक’- सुभीते के लिए भले ही कह लें, किन्तु इनके बीच किसी मूलभूत विरोध की कल्पना निराधार है।
[…]
कबीर का निधन के पचास साल के भीतर-भीतर हरिराम व्यास ने उनके तथा उनके गुरु रामानंद के गुण गाए। सौ साल के भीतर-भीतर अनंतदास ने कबीर की परिचई लिखी। परिचई शब्द परिचय के साथ ही चमत्कार वर्णन का आशय भी व्यंजित करता है। कहावत है-‘देवी दिन काटे, पंडा परचा (चमत्कार का प्रमाण) मांगे’। निधन के सौ बरस के भीतर ही कबीर की हैसियत चमत्कारी शख्सियत की मान ली गयी थी। लेकिन “आधुनिकों” को कबीर असफल नजर आते हैं। किसी को लगता है कि वे ‘मुसलमानों के बीच रह कर भगवान के दुष्टदलनकारी रूप की बात करने का साहस न जुटा सके’, तो किसी को लगता है कि वे अलग धर्म की स्थापना करना तो चाहते थे, कर नहीं पाए।
औपनिवेशिक आधुनिकता में रची-बसी ‘खोज-दृष्टि’ कबीर के समाज की लोक-स्मृति को ही नहीं, स्वयं कबीर को भी ऐसी कृपादृष्टि से देखती है जिसे कबीर अबोध बच्चे से नजर आते हैं, जो अपने घर का पता तक ठीक से नहीं बता पाता। देखिए न, असल में तो वे थे— ईसाई मिशनरी के पूर्व-पुरुष, शरा या बेशरा सूफी, महायानी बौद्ध, नाथपंथी या आजीवक, लेकिन समझते थे खुद को नारदी भक्ति में मगन-‘ भगति नारदी मगन सरीरा-इहि विधि भव तरै कबीरा’!
कबीर अकेले ही क्यों, ऐसे खोजियों के हिसाब से तो सारा समाज ही एक तरफ ‘भोले-भाले’ अबोध लोगों और दूसरी तरफ सुबह से शाम तक साजिश रचने वालों के बीच बंटा हुआ था। औपनिवेशिक आधुनिकता और उत्तर-आधुनिकता ने कुछ लोगों की साजिशों और बाकी लोगों के बुद्धूपन को भारतीय सांस्कृतिक अनुभव की ऐतिहासिक व्याख्या के बीज-शब्दों (की कंसेप्ट्स) के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।
कबीर को अंगुली पकड़ कर चलाने की बजाय, उनकी कविता की अंगुली पकड़ कर चलें; विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और प्रमाणों के साथ मनमानी करने की बजाय, उन्हें विवेक के साथ, समग्रता में पढ़ें, तभी हम कबीर की संवेदना और उनके समय के बारे में प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकेंगे।
भारत ही नहीं, किसी भी समाज या परंपरा के अनुभवों को साजिश और बुद्धूपन सरीखे ‘बीज-शब्दों’ (!) के जरिए नहीं समझा जा सकता।
संस्कृत, फारसी के मुकाबले देशभाषा स्रोतों की उपेक्षा औपनिवेशिक ज्ञानकांड में बद्धमूल थी और अभी भी है। इसी संस्कार के कारण, उन्नीसवीं सदी के ‘पाखंडखंडिनी’ और ‘त्रिज्या’ के विवाद को, उन्हीं दिनों चल रही, कबीर की ‘खोज’ में, ध्यान देने योग्य पाठ की हैसियत नसीब न हो सकी। बीजक की ‘पाखंडखंडिनी’ टीका पारखमार्ग के प्रणेता पूरन साहब की ‘त्रिज्या’( 1837ई0) का खंडन करने के लिए ही लिखी गयी है। ‘पाखंडखंडिनी’ के रचयिता विश्वनाथसिंह जू देव ने चूँकि कुछ और काव्य-रचना भी की थी, सो शुक्लजी के ‘इतिहास’ में उनका उल्लेख हुआ। उन्होंने कबीर को सगुण रामावतार का ही उपासक सिद्ध कर दिया था। यह चलन बन गया कि कबीर के अध्येता ‘पाखंडखंडिनी’ पढ़ें न पढ़ें, उसका उल्लेख अवश्य करें। ‘त्रिज्या’ के लेखक पूरन साहब भी खासे कल्पनाशील टीकाकार थे। उन्होंने कबीर को जैनों जैसा ‘जीववादी’ सिद्ध कर दिया था। शायद इसीलिए वे शुक्लजी को उल्लेखनीय न लगे हों। जो हो, ‘हरिऔध’ के बाद किसी “आधुनिक” अध्येता ने ‘त्रिज्या’ को थोड़ी-बहुत चर्चा करने योग्य भी नहीं समझा। हाँ, क्षितिमोहन सेन और केदारनाथ द्विवेदी जैसे कुछ विद्वानों ने कबीर-पंथ के प्रसंग में ‘त्रिज्या’ का उल्लेख भर जरूर किया।
कबीर के अध्येताओं ने देशभाषा में बोलने वाले व्यक्तियों और रचनाओं का उपयोग औपनिवेशिक ज्ञानकांड द्वारा “खोजी” गयी किसी न किसी कबीर-छवि को “प्रामाणिक” सिद्ध करने भर के लिए, ‘नेटिव इंफार्मेंट’ की तरह किया है। नेटिव इंफार्मेंट का मतलब हैः ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज के बारे में कुछ सूचनाएं अध्येता तक पहुंचाए। उससे यह उम्मीद नहीं की जाती कि इन सूचनाओं का अर्थ समझे या उस पर विचार-विमर्श कर सके। उसका काम सूचना देना भर है, विचार-विमर्श करने की अक्ल उसमें कहां? सूचना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखने की सामर्थ्य उसमें कहां?
देशभाषा स्रोतों को ‘भोले-भाले’, ‘नेटिव इंर्फामेंट’ की तरह बरतने के कारण, भारतीय चिन्तन परंपरा को संस्कृत तक सीमित कर देने के कारण, चौदहवीं सदी से आरंभ हुए भक्ति-आंदोलन और ‘प्राचीन भागवत धर्म’ के अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह सवाल ही लोगों के मन में नहीं उठता कि सोलहवीं सदी के अनंतदास आखिर क्यों और किस अर्थ मे चौदहवीं सदी के नामदेव को ही कलियुग में भक्ति का प्रतिपादन करने का श्रेय दे रहे थे—“ कलिजुगि प्रथमि नामदेव भइयो”।
अन्य वैष्णवों की तरह अनंतदास भी कलियुग का आरंभ श्रीकृष्ण के गोलोकगमन के बाद से ही मानते रहे होंगे। ‘प्राचीन भागवत धर्म’ इस घटना के बाद ही आया था। लेकिन अनंतदास ‘प्राचीन भागवत धर्म’ को नहीं, सैकड़ों साल बाद के, चौदहवीं सदी के नामदेव को कलियुग में भक्ति के प्रतिपादन का श्रेय दे रहे हैं। विनांद कैल्वर्त्त जैसे लोग रामानंद को कबीर का गुरु बताने के कारण अनंतदास के इतिहास-बोध पर तरस खाते हैं। रामानंद, कबीर, पीपा और रैदास जैसों की भक्ति का आरंभ गुप्तकाल के भागवत धर्म से नहीं, नामदेव से बताने वाले अनंतदास के भक्ति-बोध पर ध्यान दें तो कैल्वर्त्त साहब के अपने बुद्धि-बोध का उद्धार होने की संभावना बनती है।
कबीर ही नहीं, भारतीय इतिहास लेखन मात्र के प्रसंग में, परिचई के लेखक अनंतदास से लेकर त्रिज्या-टीका रचने वाले पूरन साहब तक सरीखे देशभाषा के बौद्धिकों के साथ जो संबंध “आधुनिक” अध्येताओं ने बनाया है, वह याद दिलाता है, फिल्म ‘गाइड’ के एक दृश्य की। राजू गाइड को गांव वाले साधु-महात्मा समझने लगे हैं। गांव के पुरोहितों को राजू का सम्मान नागवार गुजरता है। वे संस्कृत बोलने की चुनौती देकर राजू को साधु नहीं, अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं—“ बोलेंगे क्या, संस्कृत आती हो तब ना!” राजू गाइड की नाक का सवाल है। वह अंग्रेजी बोलने लगता है, और पुरोहितों को अज्ञानी सिद्ध कर देता है—“बोलेंगे क्या, अंग्रेजी आती हो तब ना!”
जो न संस्कृत या फारसी बोलते हैं, न अंग्रेजी, वे “बोलेंगे क्या?” –इस मानसिकता से मुक्त होकर सुनें तो हम सुन सकते हैं कि कबीर को उनके समाज और परंपरा ने न असफल स्वर माना न हाशिए की आवाज। हम देख सकते हैं कि कबीर के समय का भारत उद्धार के लिए यूरोपीय आधुनिकता के अवतार की प्रतीक्षा करता भारत नहीं, स्वयं अपनी परंपरा से पनप रही, देशज आधुनिकता की ओर बढ़ता भारत था। कबीर और तुकाराम आधुनिक इसलिए नहीं लगते कि वे अपने समय से आगे निकल कर आधुनिक हो गए हैं, बल्कि इसलिए लगते हैं क्योंकि जिस समय में ये कवि रचना कर रहे हैं, वह समय भारतीय इतिहास में आधुनिकता के उदय का समय है।
कबीर के समय और भारतीय सांस्कृतिक अनुभव के बारे में मेरी धारणाएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं; कारण यही है कि पिछले कई सालों से मैंने संस्कृत और अंग्रेजी के साथ उन स्रोतों को भी पढ़ने, सुनने और गुनने की कोशिश की है, जो न संस्कृत, फारसी बोलते हैं, न अंग्रेजी।
[…]
एक विचारक मानते थे कि यहूदी पैदाइशी झूठे और दुष्ट होते हैं। उनकी एक किताब का शीर्षक ही है: ‘यहूदी और उनके झूठ’। इसमें वे ‘अपने’ लोगों को धिक्कारते हैं कि ‘शर्म करो, यहूदी जिन्दा हैं’। वे आव्हान करते हैं कि इन ‘जहरीले कीड़ों’ के घर, उपासना स्थल, पवित्र पोथियां जला दी जाएं। ऐसी हालत कर दी जाए कि यहूदी या तो सदा के लिये, जहन्नुम नहीं तो‘कहीं और’ चले जाएं, ताकि हमारा प्यारा देश उनके फैलाए गंद से पाक हो। देश में रहना ही है तो यहूदी हमारे दास बन कर रहें।
इन विचारक के परिवेश में पुस्तक दहन का सांस्कृतिक कार्यक्रम जोर-शोर से चल रहा था, कुरान के अनुवाद को भी जलाने का फैसला हो चुका था, विचारक ने कुरान को न जलाने की सिफारिश की, ताकि लोग जान सकें कि ‘इस किताब में कैसी- कैसी शैतानी खुराफातें भरी हुई हैं, और इसका अनुगमन करने वाले किस हद तक शैतान की गिरफ्त में हैं’।
हिटलर की नहीं, हम बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर की, जो कबीर के समकालीन थे, और जिनसे कबीर की तुलना ब्रिटिश अध्येता किया करते थे । लूथर का समय 1483-1546 है। ‘यहूदी और उनके झूठ’ की रचना लूथर ने जवानी के जोश में नहीं, पौढ़ी उम्र में की थी। इस समय वे प्रोटेस्टेंट रिफार्मेशन के जन्मदाता के रूप में विख्यात हो चुके थे। लूथर के यहूदी-विरोधी विचारों ने हिटलर को काफी प्रेरित किया था। कुरान का लैटिन अनुवाद जलने से लूथर ने 1530 में बचाया था। बचाने का कारण आप देख ही चुके हैं।[i]
पुस्तक दहन यूरोप में सदियों तक चला सुनियोजित अनुष्ठान था,जिसमें कैथॉलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे थे। जहां-जहां ये दोनों पहुंचे, वहां-वहां इस होड़ को भी साथ ले गये। खुद “परमात्मा का वचन” भी इस होड़ का शिकार होने से बच नहीं पाया। दक्षिण भारत में लूथरपंथी प्रोटेस्टेंटों ने बाइबिल का तमिल अनुवाद प्रकाशित किया, और आरोप लगाया कि जेसुइटों ने इस प्रोटेस्टेंट बाइबिल की प्रतियां खोज खोज कर जलाईं।[ii] इस होड़ का सबसे मार्मिक दृष्टांत बना मिशेल सर्वेटस का भाग्य। जेनेवा के प्रोटेस्टेंटों ने उन्हें उनकी पुस्तकों के साथ जिन्दा जला देने में बाजी मार ली, फ्रांस के कैथॉलिकों को सर्वेटस के पुतले जला कर ही संतोष करना पड़ा।[iii] आलम यह था कि इंग्लैंड के रोजर विलियम्स ने परस्पर सहिष्णुता दिखाने का निवेदन करते हुए एक पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक को ही 1644 में बाकायदा पार्लामेंट के आदेश पर फूंक दिया गया।
कबीर शाक्तों से काफी चिढ़ते थे,और तुलसीदास निर्गुणपंथियों से, लेकिन अपने प्रशंसकों को दोनों में से किसी ने नहीं धिक्कारा कि शर्म करो, ये चिढ़ाऊ लोग जिंदा हैं। पुस्तक दहन ने ऐसी लोकप्रियता कबीर और तुलसी के समाज में कभी नहीं पाई। आजकल जरूर अपने देश में भाँति-भाँति के लोग भाँति-भाँति की पुस्तकें जलाते पाए जाते हैं, यह “परंपरा” औपनिवेशिक आधुनिकता के ही उपहारों में से एक है।
आरंभिक आधुनिक काल के यूरोप में, 1480 से 1700 के बीच कोई एक लाख औरतें चुड़ैल कह कर सताईं गयीं, और जिन्दा जलाईं गयीं। विपथगामियों (हेरेटिक्स) को चर्च द्वारा निर्धारित ‘सन्मार्ग’ पर लाने वाले इंक्विजीशन’ के बारे में तो सब जानते ही हैं। संस्थाबद्ध असहिष्णुता और विस्तृत यातना के इस भयानक रूप की गतिविधियों का ‘स्वर्ण युग’ वही था, जिसे यूरोपीय इतिहास का ‘आरंभिक आधुनिक युग’ कहा जाता है। इसी युग में हुए फीरोज तुगलक या औरंगजेब को धार्मिक असहिष्णुता के देहधारी रूप माना जाता है,लेकिन इनमें से किसी को नहीं सूझा कि विधर्मियों और विपथगामियों को यातना देने के लिये बाकायदा एक संस्था खड़ी कर दी जाए।
मध्यकालीन और आधुनिक केवल समयसूचक शब्द नहीं, मूल्यबोधक ‘टर्म्स’ भी हैं। व्यापार के विस्तार, मानवकेंद्रित चिंता और चर्च के प्रति असंतोष के उदय के आधार पर यूरोप में मध्य और आधुनिक काल की संधि-वेला चौदहवीं-पंद्रहवीं सदी में मानी जाती है। मान्यता यह है कि यूरोप तो मध्यकाल की ‘जकड़’ से चौदहवीं सदी में ही निकल चला था, जबकि भारत समेत बाकी सारी दुनिया इतिहास की चौदहवीं सदी में तो थी, लेकिन यूरोप की तरह आरंभिक आधुनिक काल में प्रविष्ट हो जाने की बजाय मध्यकाल में ही ठहरी हुई।
इतिहास-क्रम में प्रबोधन आधुनिकता के पीछे आता है। आधुनिक होने के पहले कोई समाज प्रबुद्ध नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकते हैं, ऐसे लोग अपने वक्त से आगे कहलाते हैं, लेकिन प्रबोधन के मूल्यों का व्यापक समाज में प्रचार तो आधुनिकता के बाद ही हो सकता है। यूरोप में आरंभिक आधुनिक काल शुरु हुआ पंद्रहवीं सदी में। प्रबोधन( एनलाइटेनमेंट) का दौर शुरु हुआ सत्रहवीं सदी से। इसी अर्थ में यूरोपीय प्रबोधन से वंचित लोग- क्या अकबर क्या कबीर और क्या तुकाराम अपने वक्त से आगे और आधुनिक (अर्थात् प्रबुद्ध) चित्त के निकट कहे जाते हैं। प्रबोधन के मूल्य हैं- व्यक्तिसत्ता की स्वीकृति, सहिष्णु्ता और विवेक। बोलचाल में आधुनिक और प्रबुद्ध घुलमिल जाते हैं। आधुनिक का अर्थ हो जाता है विवेकपरक, व्यक्ति-सत्ता स्वीकार करने वाला, सहिष्णु चित्त; और मध्यकालीन का मतलब व्यक्ति-सत्ता को नकारने वाला। प्रेमी जोड़े को फांसी चढ़ाने का आदेश देने वाली पंचायत का व्यवहार मध्यकालीन और प्रेमी-प्रेमिका का आधुनिक।
अकबर ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों की स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया, दासों के व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की—दूसरे शब्दों में व्यक्ति-सत्ता के सम्मान को, हर मनुष्य की मनुष्यता की स्वीकृति को राजकीय नीति और व्यवहार का आधार बनाने की यत्न किया, सुलहकुल को राजकीय नीति बनाया। राजधर्म की अकबरी धारणा एम. अतहर अली के शब्दों में, यह थी, “प्रचलित विश्वासों के प्रति सहिष्णुता शहंशाह के कर्त्तव्य का सिर्फ़ एक अंश है; बुद्धि का अनुकरण करने और इस तरह परंपरावाद को नकारने पर लोगों को आमादा करना भी एक आवश्यक और पूरक कर्त्तव्य है”।[iv]
उपरोक्त धारणा राजसत्ता की सामाजिक भूमिका की ठेठ आधुनिक समझ को व्यंजित करती है, लेकिन यूरोपीय न होने के पाप का फल ही कहिए कि अकबर तो मध्यकालीन कहलाता है, जबकि उस के समकालीन, विच-हंटिंग तथा इंक्वीजीशन में विशेष महारत हासिल करने वाले स्पेन और फ्रांस के राजा आधुनिक समय में स्थित माने जाते हैं।
सोचना चाहिए, कबीर या तुकाराम जैसे “आधुनिकता का पूर्वाभास” देने वाले कवियों को क्या निरवधि काल और विपुला पृथ्वी से आशा करनी पड़ी कि कभी न कभी उनका भी कोई समानधर्मा उत्पन्न होगा, जो उन्हें सराहेगा, उनके महत्व की ‘खोज’ करेगा; या उनके अपने ‘स्तब्ध मनोवृत्ति’ वाले ‘मध्यकाल’ में ही उन्हें विपुल श्रोता समुदाय और व्यापक सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ?
हिन्दुओं और मुसलमानों के जो “प्रतिनिधि” कबीर के विरुद्ध शिकायतें लेकर सिकंदर लोदी के हुजूर में पहुँचे थे,उनकी शिकायत अनंतदास के शब्दों में यही थी,“तातैं हमें माने न कोई, जब लग जुलाहा कासी होई”। कबीर के अंतिम संस्कार को लेकर जिनके बीच तलवारें खिंच गयीं, उनमें से एक राजा थे, दूसरे नवाब। कबीर ने स्वयं न तो कोई नया धर्म चलाया, न कोई निराला पंथ निकाला, लेकिन जब उनके नाम से पंथ चला तो संपन्न व्यापारी धर्मदास ने चलाया। कबीर-चौरा की आचार्य-परंपरा में कबीर के तुरंत बाद नाम आता है, सुरतिगोपाल साहब का। ये वही पंडित सर्वजीत थे, जो कबीर को शास्त्रार्थ में परास्त करने की इच्छा लेकर आए और कबीर के शिष्य बन गए। किंवदंतियों के अनुसार सर्वजीत का विवाह कबीर की पुत्री कमाली के साथ हुआ था।
किंवदंतियाँ ऐतिहासिक स्मृति के लोक-चित्त में स्थापित होने की विधियाँ ही हैं। किसी समय और समाज के चित्त, चिंतन और चिंताओं को समझने के लिए उसमें प्रचलित किंवदंतियों के संकेतों को समझना ज़रूरी है।
कबीर के समय में व्यापार के विस्तार के कारण व्यापार जुड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। वर्णाश्रम-व्यवस्था अप्रासंगिक हो रही थी। दसवीं सदी के बाद से, भारत में आर्थिक जीवन का पुनरोदय होता दीखता है, लेकिन देश की राजनीतिक स्थिति और व्यापार की संभावनाओं में अंतर्विरोध था। रामशरण शर्मा इस स्थिति को “दो भिन्न वास्तविकताओं के रंग से रंगा चित्र” कहते हुए बताते हैं, ‘इस चित्र में एक तरफ उपसामंतीकरण है, परजीवी पुरोहित व्यापार और शिल्पोद्योग से प्राप्त आय हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरी ओर आय के नकद अनुमान, बेगार का लोप और मुद्रा का व्यापक प्रचलन जैसे लक्षण दिख रहे हैं’।[v]
सरहपा से लेकर कबीर तक को मिली सामाजिक स्वीकृति इन “दो भिन्न वास्तविकताओं” के अंतस्संघर्ष के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। सरहपा और कबीर जैसे देशभाषा के विचारक तो ‘मनुवाद’ का प्रतिवाद कर ही रहे थे, संस्कृत चिंता भी मनु के विचारों से आगे बढ़ कर, व्यापार के पुनरोदय के कारण उत्पन्न नयी स्थितियों के अनुरूप धर्मशास्त्र की नयी व्याख्याएं कर रही थी। बारहवीं सदी में, देवल दो टूक शब्दों में कह रहे थे कि ‘जहां तक व्यापार का सवाल है, लोक-स्वीकृत और व्यावहारिक व्यवस्थाओं को एक नहीं, सैकड़ों ‘धर्मशास्त्रीय’ वचनों पर वरीयता दी जानी चाहिए, भले ही “वचन” स्वयं मनु के ही क्यों न हों।[vi] ‘यशतिलक’ में तेली वंश में जन्मे मंत्री, नाई घर में जन्मे सेनापति, वर्णसंकर महामंत्री, वेश्यापुत्र राजा और हीनकुलोत्पन्न राजगुरु का बाकायदा नाम लेकर उल्लेख किया गया है। बंगाल के वल्लालसेन ने महेश नामक मल्लाह को महामंडलीक नियुक्त किया था, और लक्ष्मणसेन ने धोयी नामक जुलाहे को राजकवि।[vii]
मनु के अनुसार, अपराधी ब्राह्मण को बहुत नरम सजा दी जानी चाहिए, उसे प्राणदंड तो किसी भी स्थिति में नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिस काल की बात हम कर रहे हैं, उसमें गौतमीय धर्मसूत्रों पर भाष्य करते हुए हरदत्त व्यवस्था देते हैं कि सारे वैदिक संस्कार विधिपूर्वक करने वाले ब्राह्मण को ही अवध्य माना जा सकता है, ब्राह्मणकुल में जन्मे जिस-तिस को नहीं। ‘विवाद-रत्नाकर’ के रचयिता चंडेश्वर अवध्यता के लिए इतनी कड़ी शर्तें लगाते हैं कि किसी अपराधी ब्राह्मण का अवध्य होना असंभव हो जाए। उनके अनुसार केवल वही ब्राह्मण अवध्य है, जो वेद-वेदांग-न्याय; इतिहास-पुराण में पारंगत हो, शास्त्रानुकूल आचरण करता हो, षड़कर्म पालन करता हो; ऐसा ब्राह्मण भी तभी अवध्य है, जब अपराध उससे गलती से हो गया हो। इरादतन अपराध करने वाला आचारनिष्ठ ब्राह्मण भी, चंडेश्वर के अनुसार न तो अवध्य है, न उसे शारीरिक दंड से किसी छूट का अधिकार है।[viii]
कबीर की कविता में, उनके पूर्ववर्तियों से भिन्न, ‘चिलम न पा सकने वालों’ के आक्रोश और ‘हीन भावना की ग्रंथि’ की बजाय जो आत्मविश्वास आ. हजारीप्रसाद द्विवेदी[ix] नोट करते हैं, उसका संवेदनात्मक कारण प्रेम-भक्ति अवश्य है, लेकिन संरचनात्मक कारण कुछ और है, और इतिहास-लेखन की दृष्टि से वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापारियों, दस्तकारों की आर्थिक ताकत और सामाजिक हैसियत में बढ़ावा आ रहा था। नगर विकसित हो रहे थे, भक्ति का लोकवृत्त प्रभावी भूमिका निभा रहा था। कबीर और उनके जैसे अन्यों के आत्मविश्वास का संरचनात्मक कारण यही था कि चंद ब्राह्मण और मौलवी जो भी कहते रहें, कबीर जैसे लोग इस वक्त हाशिए की आवाज नहीं, समाज के महत्वपूर्ण तबकों-व्यापारियों और दस्तकारों की आकांक्षाओं की आवाज बन चुके थे।
दस्तकारों की तादाद में बढ़ोत्तरी क्या व्यापार के विस्तार के बिना संभव है? सामंती मनमानी के विरुद्ध फेयर-प्ले — न्यायसंगत व्यवहार—की माँग दुनिया भर के इतिहास में व्यापार के विकास और व्यापारियों के सामाजिक प्रभाव के विस्तार से जुड़ी हुई रही है। निर्गुण संवेदना की केन्द्रीय विशेषता (आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में फेयर-प्ले की माँग) का सीधा संबंध व्यापारियों के सामाजिक अनुभवों और आकांक्षाओं से जुड़ता था। इसी कारण परजीवियों द्वारा उत्पीड़ित ये संत व्यापारियों और दस्तकारों के बीच पुजने की हद तक लोकप्रिय हुए।
कबीर का आत्मविश्वास केवल उनकी संवेदना का नहीं, व्यापार के विस्तार, भारतीय समाज के ऐतिहासिक विकास का भी परिणाम था।
मजे की बात यह है कि पक्के भारतीयतावादी हों या ठेठ क्रांतिकारी, भारतीय समाज की इतिहासविहीनता के अंधविश्वास में दोनों ही विश्वास करते हैं। मनु महाराज के भक्त हों या मनुवाद के घोर विरोधी, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कात्यायन को प्रमाण बताते हुए देवल और वरदराज व्यवस्था दे रहे थे कि शास्त्रवचन की संगति लोकाचार के अनुकूल ही लगानी चाहिए और प्रसंगविशेष में ‘धर्मानुकूल आचरण’ क्या है, इसका निर्णय राजशासन को करना चाहिए।[x] समाज जजमानी पर नहीं, ‘पॉलिटिकल इकॉनॉमी’ के आधार पर चल रहा था। राजसत्ता ऊपर-ऊपर की, फालतू की वस्तु नहीं थी,बल्कि धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के निर्णय में व्यापारिक जरूरतों के साथ-साथ राजाज्ञा की भी भूमिका निर्णायक थी। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को शाश्वत मानने वाले, बाकी सभी लोगों के जीवन की सार्थकता ब्राह्मणों की सेवा में ही मानने वाले मनु कबीर के समय में इतने भी महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे कि कबीर और अन्य लोग नाम लेकर उनकी आलोचना करने की जरूरत समझें।
दसवीं सदी में व्यापार का पुनरोदय हुआ था, मनु-महिमा का पुनरोदय हुआ अठारहवीं सदी में, जब ग्यारह ब्राह्मणों की कमेटी ने 1773 से 1775 तक, ओरियंटलिस्ट नेथेनियल हालहेड की अध्यक्षता में ‘हिन्दू विधि’ –हिन्दू लॉ को ‘कोडिफाई’ किया। हालहेड साहब स्वयं संस्कृत नहीं जानते थे। कोडिफाइड ‘हिन्दू लॉ’ का संस्कृत से मौखिक बांगला अनुवाद किया गया, इस अनुवाद का अनुवाद हालहेड साहब की सहूलियत के लिए फारसी में किया गया, और उन्होंने उस फारसी अनुवाद का अनुवाद अंग्रेजी में किया। इतने अनुवादों से गुजर कर ‘हिन्दू लॉ’ में भ्रष्टता तो आ ही जानी थी।
विलियम जोंस इस भ्रष्ट अनुवाद से बहुत असंतुष्ट थे। लेकिन उनके हिसाब से यह भ्रष्टता ‘कोडिफिकेशन’ के लिए अपनाई गयी विचित्र विधि, और हालहेड के अज्ञान की नहीं, पंडितों के स्वभाव की ‘नैतिक भ्रष्टता’ की ही परिणति थी।
जोंस तथा अन्य औपनिवेशिक विद्वान मानते थे कि हिन्दू सोच-विचार का जितना विकास होना है, हो चुका है। उन्हें इस बात का न बोध था, न परवाह कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों परंपराएं, दोनों ‘विधियां’ शास्त्र और लोक के, सार्वत्रिक और स्थानीय के संवाद के कारण लगातार विकसित होती रही है, स्वयं उनके समय में हो रही हैं।
जोंस साहब ने हालहेड के ‘भ्रष्ट’ पंडितों की बजाय ‘अपने’ श्रेष्ठ पंडित चुने, और हिन्दू विधि का ‘प्रामाणिक’ पाठ तैयार किया। 1794 में जोंस द्वारा इन पंडितों के सहयोग से तैयार किया गया ‘मनुस्मृति’ का पाठ- ‘दि इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिन्दू लॉ ऑर दि ऑर्डिनेंसेज़ ऑफ मनु’ प्रकाशित हुआ। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आश्वस्त थे कि पंडित जगन्नाथ तर्कपंचानन जैसे प्रतिष्ठित पंडितों के जुड़े होने के कारण इस ‘ऑर्डिनेंसेज’ को हिन्दुओं के बीच मान्यता प्राप्त हो सकेगी, सर जॉन शोर रोमांचित थे कि ब्राह्मण विद्वानों ने हिन्दू विधि का ‘निर्माण’ एक अंग्रेज के ‘निर्देशन’ में किया है।[xi]
औपनिवेशिक सत्ता कई तरह के प्रयोग कर रही थी, वाद-विवाद-संवाद की प्रदीर्घ, जीवंत परंपरा को ‘ऑर्डिनेंसेज ऑफ मनु’ और ‘दि मोहम्मडन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस’ के जरिए जड़ बना देने के, नाक की लंबाई के आधार पर रक्तशुद्धि और उसके आधार पर जाति-व्यवस्था में स्टेटस निर्धारित करने के, सारे के सारे जन-समूहों को पैदाइशी रूप से अपराधी घोषित करके ‘कंसंट्रेशन कैंपों’ में बंद कर देने के, समलैंगिकता को ‘भारतीय परंपरा’ के लिए घातक, शर्मनाक घोषित कर देने के…।
अकबर इलाहाबादी ने अंग्रेजों की बनाई नयी दिल्ली की ‘तारीफ’ में एक ग़ज़ल कही है, उसका एक शे’र , ऐसे प्रयोगों के संदर्भ में बरबस याद आता है:
औजे वक्त मुलाकी उनका, चर्खे हफ्त तबाकी उनका
महफिल उनकी साकी उनका, आँखें मेरी बाकी उनका।
1794 को मनुवाद के पुनर्जन्म का वर्ष माना जा सकता है। इसके पहले, मनुस्मृति बीस में से बस एक स्मृति थी। निश्चय ही थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण, लेकिन अंतिम रूप से निर्णायक और हर स्थिति में, हर स्थान पर बाध्यकारी कदापि नहीं।
कबीर मनुवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाली देशज आधुनिकता के कवि हैं। औपनिवेशिक आधुनिकता को श्रेय जाता है देशज आधुनिकता को अवरुद्ध करने का, वर्णाश्रम में नस्लवाद को जोड़ देने का, मनुवाद की पुनः प्रतिष्ठा करने का, वाद-विवाद से भरपूर उस समय को स्तब्ध मनोवृत्ति के समय के रूप में पेश करने का।
[i] हंस जे. हिलरबैंड, ‘ ऑन बुक बर्निंग ऐंड बुक बर्नर्स: रिफ्लेक्शंस ऑन दि पॉवर (ऐंड पॉवरलेसनेस ऑफ आइडियाज़)’– जर्नल ऑफ दि अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन,खंड 74, अंक 3, सितंबर, 2005, पृ0 598.
[ii] केट टेल्सचर, ‘इंडिया इंस्क्राइब्ड: योरोपियन ऐंड ब्रिटिश राइटिंग ऑन इंडिया 1600-1800’, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, 1997, पृ0 101.
[iii] हंस जे. हिलरबैंड, पृ0 600.
[iv] एम. अतहर अली, ‘ अकबर और अबुल-फ़ज़्ल के भारत संबंधी विचार’ ( मध्यकालीन भारत-6, सं0इरफान हबीब, राजकमल, नयी दिल्ली, 2004), पृ0 19.
[v] रामशरण शर्मा, ‘भारतीय सामंतवाद’ राजकमल, नयी दिल्ली, 1973, पृ0 269.
[vi] आशुतोष दयाल माथुर, ‘मीडिएवल हिन्दू लॉः हिस्टॉरिकल इवोल्यूशन ऐंड एनलाइटेंड रिबेलियन’ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्नी, 2007, पृ014.
[vii] पुरुषोत्तम चंद्र जैन, ‘सोशियो इकॉनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मीडिएवल इंडिया’, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1976, पृ0 12,14.
[viii] वही, पृ0 188.
[ix] हजारी प्रसाद द्विवेदी, ‘कबीर’ राजकमल, नयी दिल्ली, 2000, पृ0 132.
[x] आशुतोष दयाल माथुर, पूर्वोद्धत,पृ06.
[xi] केट टेल्सचर, पूर्वोद्धृत, पृ0 199-200.
this article is a guide to GURU s of hindi depts. I am a reguler reader of Dr Aggarwal. thanks for this article. can you inform about the print edition of the pratilipi including the back issues. TARUN GOYAL Muzaffarnagar UP
बेहतरीन पुस्तक….
पुरुशोत्तमजी की पुस्तक पढ कर कबीर की कविता पर और विश्वाश बढा.
एक तेजी से गड़बड़ होते समय में बहुत ही अच्छी पुस्तक.
पिछले कई महीनो से दिल्ली की हिंदी अकादमी के पदाधिकारियों के चयन और शलाका सम्मान विवाद के अंत की शुरुआत करने के लिए प्रो.अग्रवालजी को बधाई .दरअसल उन्होंने इसका पुरस्कार लौटाकर यह सिद्ध कर दिया है कि साहित्यकार अपनी अर्थवत्ता कैसे कायम रख सकता है .जो आज कृष्ण बलदेव वैद्य के साथ हुआ कल को वही किसी दूसरे के साथ हो सकता है.एक अच्छी खबर यह भी है कि केदारजी ने शलाका सम्मान लेने से मना कर दिया है.ऐसे में एक बार फिर कबीर प्रासंगिक हो उठे हैं…….जब सच कहने का अवसर आये सच कहना ही होगा…..मन कभी झूठ नहीं बोलता !
A fantastic research cum critical creation on Kabir.