चेतना का प्रवाह: नंदिता दास
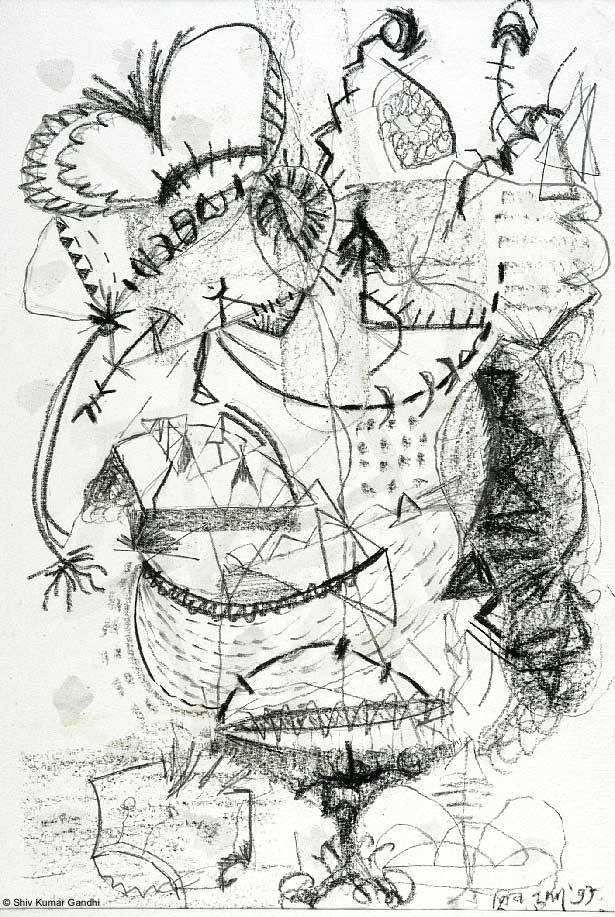
चेतना का प्रवाह
गुरुवार की सुबह तक मैं इतना विचलित नहीं हुई थी. पिछली रात मैं एक मित्र के घर थी जब टीवी पर मैंने घायलों को स्ट्रेचर पर डाल, लोगों को इधर से उधर भागते देखा. पुलिस असहाय सी खड़ी थी, लोगों में दहशत व्याप्त थी, टीवी का उदघोषक उसी तरह की उत्तेजना के साथ सूचनाएं दिए जा रहा था, जिस तरह की उत्तेजना वह तब पैदा करना चाहता है जब राखी सावंत अपने प्रेमी की पिटाई कर देती है.
कहना न होगा कि मुझ पर इस सब का बहुत मामूली असर हुआ था. मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी, “नहीं फिर से नहीं… फिर लोग मारे जाएंगे, ज्यादा दहशत, दुराग्रह और हिंसा फैलेगी.” कुछ हद तक यह प्रतिक्रिया तात्कालिक और स्वाभाविक किस्म की थी.
लेकिन आज सुबह जब मैं जागी, स्थिति बदल चुकी थी. मुझे किसी अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला था “देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या कर डाला.” लगभग इसी तरह का संदेश मेरे एक अन्य निकट मित्र को भी मिला, लेकिन उसे संदेश भेजने वाला परिचित व्यक्ति था. मुझे यह संदेश मिला क्योंकि मेरी फिल्म “फिराक” यह बताती है कि जब हिंसा भड़कती है तो मुसलमान भी उससे कैसे प्रभावित होते हैं, इसलिए यह मान लिया गया कि आतंकवादी मेरे दोस्त हैं.
आज अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वह एक सामान्य मुसलमान युवा है. मुझे मेरे अनेक मुसलमान दोस्तों के संदेश मिले जिन्हें किसी भी अन्य से ज्यादा इस घटना की निंदा करने की जरूरत महसूस होती है, जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी को जताने का दबाव किसी भी अन्य से ज्यादा महसूस करते हैं. वे गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें आतंकवादियों के साथ जोड़ कर न देखा जाए, यह एक ऐसा भय है जिसे निराधार नहीं कहा जा सकता.
इसके अलावा ऐसे असंख्य संदेश भी थे जो दुनियाभर से मेरे शुभचिंतकों ने भेजे थे जिनमें मेरी और मेरे प्रिय जनों की कुशलता पूछी गई थी. ऐसा ही मैंने भी किया. और तब ही, अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे. इस तरह से सोचना ही कितना अजीब है कि अगर हमारे प्रियजन सुरक्षित हैं तो सब ठीक है. क्यों उन लोगों के आहत होने से हमारे दिल में दर्द नहीं उठता जिन्हें हम जानते नहीं हैं और शायद जिनसे कभी हमारी जान पहचान होने की कोई उम्मीद भी नहीं है. मैं जितने ही ज्यादा लोगों के एसएमएस के जवाब में यह लिख रही थी कि मैं ठीक हूं, उतना ही ज्यादा उदासी मुझे घरेती जा रही थी.
भावनाओं का बहना भी कितना कमाल का अहसास है. यह कितने छुपे कोनों से आवेगों को बाहर ले आता है. मैं हमेशा खुद को बहुत मजबूत इरादों वाली व्यक्ति मानती रही हूं और ऐसा ही मेरे बारे में बाकी लोग भी मानते हैं. लेकिन आज मैं इस तरह आंसू बहा रही थी जिसका ठीक-ठीक कारण मैं खुद भी नहीं जानती थी. यह ऐसा था जैसे चेतना की कोई धारा कहीं और से ही बह रही हो. एक स्तर पर सब कुछ व्यर्थ नजर आता है. सबके प्रति मन आक्रोश, गुस्से और नाराजगी से भर जाता है… लगता है हम कैसे समय में जी रहे हैं.
“फिराक” के बारे में बात करते हुए मैंने अक्सर कहा है कि एक चीज है जो हम बदल सकते हैं और वह है हमारे आस-पास होने वाली घटनाओं – हिंसा, दुराग्रह, घृणा आदि के प्रति हमारी प्रतिक्रिया. यह बात याद आते ही मुझे खुद पर, अपने गुस्से पर शर्मिंदगी का अहसास हुआ. निश्चय ही एक लिहाज से यह गुस्सा जायज है और पिछली रात हमने हिंसा की जैसी गतिविधियों को देखा उसकी तुलना में यह हिंसा बहुत गौण है. लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कम या ज्यादा कुछ हद तक आक्रोश के बीज हम सभी में मौजूद रहते हैं? क्या कई बार हम जो कह या कर जाते हैं उस पर हम खुद ही हतप्रभ नहीं रह जाते हैं? बंदूक के निशाने पर लोगों की हत्या करने वाला युवक, किसी मासूम बालिका से बलात्कार करने वाला व्यक्ति, दहेज के लिए किसी महिला को जिंदा जला देने वाले लोग हमे भयभीत करते हैं, लेकिन क्या वे सभी असामान्य या बुरे लोग हैं या वे ऐसे लोग हैं जिनसे हम टकराते हैं, जिनमें से कोई शायद हमारे साथ काम करता हो या हमारे आस-पास ही मौजूद हो. व्यक्तिगत आक्रोश भी सामुहिक आक्रोश और इस तरह घृणा की राजनीति को बढ़ावा देता है. खैर यहां हम घृणा की ताकत को समझने की सैद्धांतिक कोशिश नही कर रहे है. मैं अपने भीतर आक्रोश के इस बीज को और सींचना नहीं चाहती. क्योंकि जो हुआ उसके असर को मिटने में तो लंबा समय लगेगा लेकिन हमारी एक-एक सकारात्मक ऊर्जा दुनिया को बदल सकती है. इस स्वीकारोक्ति के साथ ही मेरे आंसू बहना रुक गए हैं और मुझे करने के लिए काम मिल गया है, एक मकसद मिल गया है.
लेकिन यह सवाल फिर भी बना हुआ है, “अब क्या?” आतंकवाद के प्रति उदासीन हो कर नहीं बल्कि उसके इरादों को नाकाम करने के लिए क्या मुझे हमेशा की तरह अपने काम में लग जाना चाहिए? उनका इरादा हमें डराना और आतंक का माहौल पैदा करना है. अगर वे जो चाहते हैं मैं उन्हें वह हासिल ही न करने दूं तो क्या होगा? लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि मैं हमेशा की तरह अपने काम में न जुट सकूं, तब क्या? यदि मेरे मन में इसके प्रति इतना आक्रोश भर गया हो कि मैं उसे नजरअंदाज न कर सकूं तब क्या? अपनी छोटी सी दुनिया में सीमित हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है. वास्तव में हम में से अधिकांश शहरी सम्पन्न लोगों के साथ यही हो भी रहा है. अक्सर “गंभीर फिल्में” न देखने के पीछे मुझे यही बहाना सुनने को मिलता है. यह आराम से कह दिया जाता है कि “जिंदगी में पहले ही बहुत तनाव हैं, ऐसे में यथार्थवादी फिल्में देख कर अपने दिमाग पर और बोझ क्यों डालें, जबकि पलायनवादी मनोरंजक फिल्में देखकर उस यथार्थ से, कुछ देर के लिए ही सही, मुंह चुराया जा सकता है.” लेकिन तब क्या जब ऐसा ही कोई यथार्थ हमारी ठहरी हुई जिंदगी में अचानक से घुसपैठ कर जाता है, तब हम उसका मुकाबला करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं. तब हम क्या करते हैं?
मैं जिस दौरान इस द्वंद से जूझ रही थी, उस वक्त सुबह की भयानक खबरों और तस्वीरों को देखने से बची हुई थी, क्योंकि मुंबई में मैं अपनी जिस दोस्त के घर में ठहरी थी उसके घर में न तो टीवी है और न अखबार ही मंगवाया जाता है. तो संयोगवश ही सही मैं इन घटनाओं से लगभग अनजान थी.
और तब दिल्ली वापसी के लिए हवाई जहाज में बैठने के बाद मैंने अखबारों में वे भयावह तस्वीरें देखीं जिन्हें शायद बाकी सभी लोग रात भर देखते रहे होंगे. इन तस्वीरों ने मुझे अंदर तक विचलित कर दिया और इससे भी ज्यादा विचलित किया अन्य पृष्ठों पर छपी उन तस्वीरों ने जो “सामान्य कार्य व्यापार के चलते रहने” की सभी परिभाषाओं का अतिक्रमण कर जाती हैं. इनमें एक पेज पर यह बताया गया था कि घुंघराले बाल अब फिर फैशन में हैं. एक अन्य पृष्ठ पर मोनिका बेदी के राहुल महाजन से विवाह की इच्छा रखने औरे ऐसी ही अन्य खबरें अंटी हुई थीं. मैं अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन मेरा माथा घूमने लगा था.
रोजाना अखबार इन्हीं सब जरूरी खबरों से भरा रहता है और इस भयावह दिन की याद के धुंधलाने के साथ ही फिर उन्हीं सब बातों को अपनी पूरी जगह मिल जाने वाली थी, तो क्यों सिर्फ एक दिन इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता था? क्या साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम अपने शोक को प्रकट कर सकें और इस तरह की हिंसा के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज करा सकें? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम साल में किसी एक सप्ताह उत्सव न मनाएं और अपने संसाधनों को हमारी पुलिस को ज्यादा बेहतर उपकरणों, बुलेटप्रूफ जैकेटों और हथियारों से सज्जित करने के लिए दें सकें? क्या देश पर गर्व महसूस करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर अपने यान को चांद पर भेजने के अलावा कोई ऐसा तरीका भी है जिससे बेहतर सुरक्षा उपाय कर मासूम लोगों को इस तरह मारे जाने से बचाया जा सके? क्या कोई ऐसा मास्टर प्लान सुझा सकता है जिसके अनुसार हम सभी इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में शामिल हो सकें. क्या कोई ऐसा तरीका है कि आक्रोश को इतनी गहरे जड़े जमाने से रोका जा सके जिसकी परिणति इस तरह की हिंसा में होती है?
जब मैं इन २०-२२ साल के युवाओं को देखती हूं, तो एक गहरी उदासी से भर जाती हूं और मेरे मन में यही सहज सवाल उठता है कि आखिर वह क्या वजह रही होगी जिसने उन्हें यहां ला छोड़ा है? क्या इसके पीछे यही कारण है कि सभी को जीवन में एक मकसद की तलाश रहती है और जब कोई युवा इस राह पर आता है, जिसे “मिशन” का नाम दिया जाता है तो अचानक उसे जीने का मकसद मिल जाता है, और उसकी निगाह में उसकी अपनी अहमियत बढ़ जाती है, और वे उसी राह पर चल पड़ते हैं? क्या यह संसार उन्हें इतना नाकुछ होने का अहसास कराता है कि जैसे ही उन्हें कोई एक पहचान मिलती है वे उससे चिपक जाना चाहते हैं, उसे ओढ़ लेना चाहते हैं? निश्चय ही यह वे मामले हैं जिनकी चरम परिणति सामने है और जिन्हें बहुत रणनीतिपूर्वक बहकाया गया है. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म से कोई भी बुरा नहीं होता और दस वर्ष तक की उम्र तक कोई भी बच्चा महज बच्चा ही होता है. तब फिर इस कोमल मस्तिष्क में बाद में ऐसा क्या घटित हो जाता है कि जिसके लिए उसे खुद अपने प्राणों का भी मोह नहीं रह जाता है? क्या कोई उपाय है कि इन भटके हुए युवाओं को बचाया जा सके? यह कोई परोपकार की बात नहीं है बल्कि अगर हमें खुद को सुरक्षित रखना है तो हमें बाकी सभी को बचाने की कोशिश करनी ही होगी. मुझे एक टीवी पत्रकार की ओर से एक अजीब संदेश मिला जिसमें कहा गया था “आतंकवादियों को माफ किया जाना चाहिए या नहीं, यह ईश्वर की मर्जी पर छोड़ा जा सकता है. लेकिन ईश्वर के साथ उनकी मुलाकात सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है – भारतीय सेना.” यहां आतंकवादी शब्द को बदल कर उसकी जगह अमेरिकी / हिंदू / मुसलमान या कोई और नाम लिख दें और नीचे आतंकवादी का हस्ताक्षर कर दें तब भी अर्थ बहुत भिन्न नहीं होगा. किसी “आम इंसान” के मन में इतनी घृणा का होना मेरे लिए कम भयावह नहीं है. आंख के बदले आंख मांगने वाले इस दुश्चक्र से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होना ही चाहिए.
मुझे नहीं पता इसके अलावा और क्या-क्या मैं महसूस कर रही हूं. यह सब उलझे हुए विचार अपना रास्ता तलाश रहे हैं. मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि हम इस तरह सनकी हो नहीं सकते, चाहे कितनी ही हिंसा और घृणा का सामना क्यों न करना पड़े. यदि हम भी यही प्रतिक्रिया करने लगे तो हालात और बदतर होंगे.
सुबह अपनी फिल्म “फिराक” अर्थहीन लग रही थी, लेकिन अब जब अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए इतना कुछ लिख चुकी हूं, तब मैं यह महसूस कर रही हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म के बारे में बताना चाहती हूं. क्योंकि मैं यह जानती हूं कि यह समय गुजर जाएगा लेकिन इसकी जो याद पीछे रह जाने वाली है वह लंबे समय तक लोगों के दिलों में भय, आक्रोश, दुराग्रह और प्रतिशोध के रूप में बसी रहेगी और धीरे-धीरे उनके मानस का अंग बन जाएगी. हमें खुद को इससे बचाना होगा और समझ, सहानुभूति और प्रेम को बचाने का रास्ता खोजना होगा. यह तमाम सुंदर शब्द जिन्हें मैं जानती हूं अपना अर्थ खोते हुए जान पड़ते हैं. हमें अपनी पूरी इच्छाशक्ति के साथ इन्हें फिर से अर्थ देना है और अपने जीवन में शामिल करना है.
(अनुवाद: देवयानी)
bahut prasangik lekh liya hai girirajji aapne …nandita ka yah kahna choota hai ki ….यह समय गुजर जाएगा लेकिन इसकी जो याद पीछे रह जाने वाली है वह लंबे समय तक लोगों के दिलों में भय, आक्रोश, दुराग्रह और प्रतिशोध के रूप में बसी रहेगी और धीरे-धीरे उनके मानस का अंग बन जाएगी. हमें खुद को इससे बचाना होगा और समझ, सहानुभूति और प्रेम को बचाने का रास्ता खोजना होगा…iski gunjaish bachi rahe…
“मुझे नहीं पता इसके अलावा और क्या-क्या मैं महसूस कर रही हूं. यह सब उलझे हुए विचार अपना रास्ता तलाश रहे हैं. मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि हम इस तरह सनकी हो नहीं सकते, चाहे कितनी ही हिंसा और घृणा का सामना क्यों न करना पड़े. यदि हम भी यही प्रतिक्रिया करने लगे तो हालात और बदतर होंगे.”
Its a good article, may force to think for all these going on unncessarily