कविता और देश से दरबदर: उदय प्रकाश
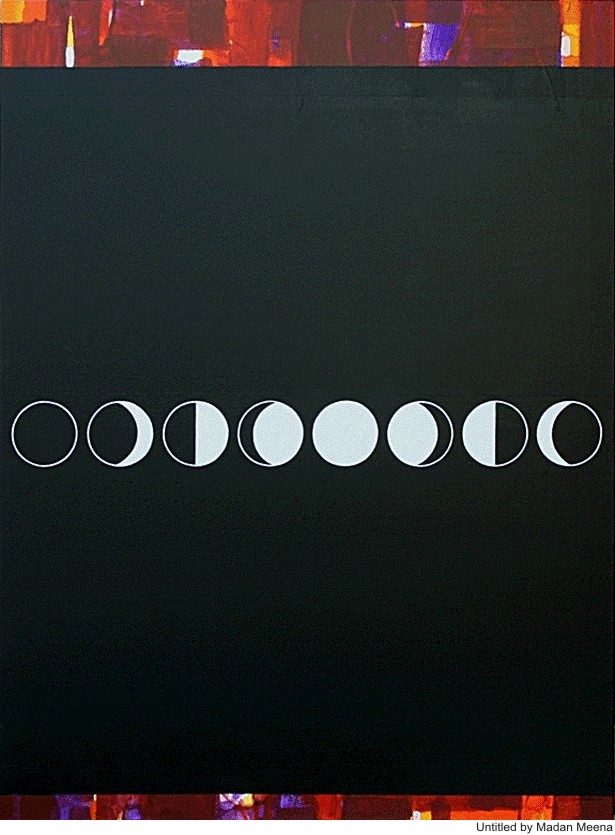
तिब्बत
तिब्बत से आये हुए
लामा घूमते रहते हैं
आजकल मंत्र बुदबुदाते
उनके खच्चरों के झुंड
बगीचों में उतरते हैं
गेंदे के पौधों को नहीं चरते
गेंदे के एक फूल में
कितने फूल होते हैं
पापा ?
तिब्बत में बरसात
जब होती है
तब हम किस मौसम में
होते हैं ?
तिब्बत में जब तीन बजते हैं
तब हम किस समय में
होते हैं ?
तिब्बत में
गेंदे के फूल होते हैं
क्या पापा ?
लामा शंख बजाते है पापा?
पापा लामाओं को
कंबल ओढ़ कर
अंधेरे में
तेज़-तेज़ चलते हुए देखा है
कभी ?
जब लोग मर जाते हैं
तब उनकी कब्रों के चारों ओर
सिर झुका कर
खड़े हो जाते हैं लामा
वे मंत्र नहीं पढ़ते।
वे फुसफुसाते हैं ….तिब्बत
..तिब्बत …
तिब्बत – तिब्बत
….तिब्बत – तिब्बत – तिब्बत
तिब्बत-तिब्बत ..
..तिब्बत …..
….. तिब्बत -तिब्बत
तिब्बत …….
और रोते रहते हैं
रात-रात भर।
क्या लामा
हमारी तरह ही
रोते हैं
पापा ?
कविता और देश से दरबदर
1.
यह बात आज से कई साल पुरानी है। आप में से कई लोगों का जन्म भी तब तक नहीं हुआ होगा। आज के कई चर्चित और प्रतिष्ठित लेखक-लेखिकाओं का भी जन्म नहीं हुआ होगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव सीतापुर में सन् 1952 में हुआ था। तब तक हमारे यहां बिजली नहीं आई थी। हमारा घर बहुत पुराना था और नदी के ठीक तट पर बना हुआ था। तट मतलब यह कि जब नदी में बाढ़ आती थी तो हमारी रसोई तक पहुंच जाती थी। तब तक नदी में पुल नहीं बना था। पेड़ के मोटे तने को खोखला करके उसे नाव की तरह, बांस की लंबी डांग से ठेलते हुए चलाते थे। इसे `डोंडा़´ या `डोंगा´ कहते थे। जब नदी में बाढ़ अधिक होती और नदी की धार बहुत गहरी और तेज़ हो जाती, तो काठ की यह नाव नहीं चलती थी। क्योंकि बांस की डांग उतनी लंबी नहीं होती थी कि धार की गहराई की थाह ले सके और नाव को आगे ठेल सके।
उस समय तक गांव में बिजली नहीं थी। लालटेनें, दिये, ढिबरियां जलती थीं। मैंने खुद भी लिखना-पढ़ना, चित्र आदि बनाना बिना बल्ब और बिजली के सीखा है। बल्कि आज तक मुझे लालटेनें और ढिबरियां अच्छी लगती हैं। हालांकि इस उम्र में और शहरों में इतने वर्षो से रहने के बाद उनकी रोशनी में अब कुछ लिख-पढ़ पाना संभव नहीं होता। दियों को मैं दीवाली और पूजा-त्यौहार के अलावा कभी पसंद नहीं कर पाया क्योंकि उनकी रुई की बाती को बार-बार बढ़ाना पड़ता है, ऐसे में उंगलियों में तेल लग जाता है और अगर आप कागज पर लिख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो वे तेल के धब्बे हमेशा के लिए वहां आ जाते हैं।
जो बात मैं `तिब्बत´ के बारे में आपको बता रहा हूं, वह इसके बहुत बाद की है। तब तक हालांकि बिजली हमारे गांव में नहीं आई थी, लेकिन बैटरी से चलने वाला रेडियो आ गया था। अंग्रेजी के नौ के अंक के भीतर से एक छलांग मारती लंबोतरी-सी बिल्ली उस रेडियो की बैटरी पर होती थी। अगर उस समय मैं यह जानता कि इस बैटरी को बनाने वाली कम्पनी वही हैं , जिसने कई साल बाद १९८४ में भोपाल में एक ज़हरीली गैस से कई हज़ार लोगो को मार डाला , तो मैं उस बैटरी ही नही रेडियो से भी डरने लगता. लेकिन तब तक मुझे यह पता नही था. रेडियो में गाने और उसके भीतर से लोगों को बोलते हुए सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कई बार रेडियो के भीतर झांक कर देखने की कोशिश करता कि वे लोग बाजा कहां पर खड़े होकर बजाते हैं और कहां से बोलते हैं। क्योंकि आवाज़ ठीक उस रेडियो के अंदर से ही आती थी। कहीं और से आती हुई बिल्कुल भी नहीं लगती थी। कोई सितार या बांसुरी बजती तो लगता इसी जगह से वह आवाज़ पैदा हुई है। बिल्कुल साफ़। धातु के तारों की आकिस्मक झनझनाहट और बांस की नली के भीतर से गुज़रती सांस की स्पष्ट सरसराहट के साथ।
अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार मैंने देर रात गये, रेडियो के अंदर, उसके भीतर के असंख्य नन्हें-नन्हें यंत्रों की नीली-लाल, हरी-पीली कई रंगों की धुंधली रहस्यपूर्ण रोशनी में बिल्कुल छोटे-छोटे, पुतलियों जैसे लोगों को एक वृत्त में खड़े होकर कई तरह के साज़ बजाते और धीरे-धीरे झूमते और गाते हुए देखा था, तो क्या आप इसे मानेंगे ? आप कहेंगे कि मैं वहीं रेडियो के पास सो गया होऊंगा और नींद में ऐसा देख लिया होगा।
बचपन में घटने वाली ऐसी किसी भी घटना को कोई भी दूसरा वयस्क बाद में नहीं मानता।
नेरुदा का संस्मरण आपने पढ़ा होगा, जब बचपन में उसके सिर के ऊपर से, उसकी मां द्वारा बुनी गई हरे रंग की ऊनी टोपी आंधी में उड़ गई थी और नेरुदा ने देखा था कि वह टोपी हरे रंग का तोता बन कर तोतों के झुंड में शामिल हो गई थी। उसने जब अपनी मां से इस घटना के बारे में बताया, तो मां ने उस पर विश्वास नहीं किया।
आपमें से अगर किसी ने मेरी एक कहानी `डिबिया´ पढ़ी हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे साथ, मेरे बचपन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं। `अरेबा-परेबा´ कहानी भी ऐसी ही बचपन की एक घटना के बारे में है। यह सचमुच गहरे अकेलेपन, असहायता और पराजय का क्षण होता है, जब आप पाते हैं कि आपके साथ घटे किसी सच का न तो कोई गवाह है, न कोई उस पर विश्वास कर रहा है। फिर सबसे बड़ी और पीड़ादायक स्थिति यह कि संसार के ज्ञान-विज्ञान के जितने भी प्रामाणिक और विश्वसनीय तरीके हैं, उनके द्वारा आप अपने उस सच को प्रमाणित भी नहीं कर सकते। मेरे साथ तो एक निजी समस्या यह भी है कि कई बार मैं स्वयं ही उलझन में पड़ जाता हूं कि अभी-अभी जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, वह सच है या कोई स्वप्न। `तिरिछ´ के पिताजी और बाद में उसके नैरेटर के साथ, या `पीली छतरी वाली लड़की´ की वह घटना जब छतरी तितली में बदल जाती है, या फिर `वारेन हेस्टिंग्स का सांड´ में चोखी और हेस्टिंग्स के बीच का पहला प्रसंग ही नहीं, उस पूरे आख्यान में यहां से वहां तक फैला असमंजस, एक तरह का विभ्रम। अगर आप ध्यान दें तो मेरी हर कहानी में मिथ्या और सत्य, कल्पना और यथार्थ, स्वप्न और वास्तविकता, अतीत और भविष्य सब आपस में एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं। इस हद तक कि उन्हें ठीक-ठीक से पहचान कर अलग कर पाना संभव नहीं लगता। स्वयं मेरे लिए भी .
मैं ऐसी कोई कहानी पढ़ भी नहीं पाता जिसमें कोई स्वप्न और विभ्रम न हो। हो सकता है बचपन से गांव में सुनी गई कहानियों-किस्सों और रामायण-महाभारत से लेकर कई ग्रंथों और बाद में पढ़े गये बहुत से श्रेष्ठ उपन्यासों-कथाओं और देखे गये सिनेमा का असर हो।
तिब्बत के साथ भी मेरा एक ऐसा ही बिल्कुल निजी प्रसंग और संबंध है। `तिब्बत´ कविता जब मैंने 1977-78 में लिखी, तो वह बचपन की एक ऐसी ही घटना से जुड़ी हुई थी।
2.
मुझे बिल्कुल ठीक-ठीक साल याद नहीं, जब यह घटना घटी। शायद 1960-61 का वर्ष होगा। हो सकता है इसके आगे-पीछे का कोई साल हो। हां, इतना ज़रूर याद है कि हमारे गांव के आज वाले घर के सामने का हिस्सा बन कर तैयार हो चुका था। यानी 1957-58 बीत चुका था। नेहरू जी तब हमारे प्रधानमंत्री होते थे और वे जीवित थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। गांव के स्कूलों में उन्हें यही सिखाया जाता था। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी और उसका झण्डा बिल्कुल राष्ट्रीय तिरंगे जैसा होता था बस बीच में अशोक चक्र की जगह पर चरखा बना रहता था। कहते थे कि वह चरखा गांधी जी ने नेहरू जी को दिया था, जिसे गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू जी ने कांग्रेस के झण्डे में छपवा दिया था। उन दिनों जब चुनाव होते तो पैंफलेट बंटते, जिनमें छपा होता -`मुहर हमारी वहीं लगेगी, जहां बनी बैलों की जोड़ी।´ अब पता नहीं वे बैल झण्डे से निकल कर कहां चले गये?
तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी शायद जीवित थे और मैं अपने बालों को उनकी तरह बनाने की कोशिश किया करता था। बालों के मामले में केनेडी और देवानंद मेरे आदर्श हुआ करते थे। बालों में तेल और पानी चुपड़कर और सामने पेंसिल खोंसकर, दोनों तरफ से हथेलियों में बालों को दबा कर बहुत बार मैंने देवानंद की तरह फुग्गे बनाये। लेकिन केनेडी के सूखे हुए बाल हमेशा मुझे अधिक पसंद थे। शायद तब तक रूस का अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन अंतरिक्ष तक पहुंच गया था। इसके पहले रूस एक कुतिया `लाइका´ को भी अंतरिक्ष तक पहुंचा चुका था। स्पेस टेक्नोलाजी के लिहाज से अमेरिका बहुत पीछे छूटता जा रहा था। पिता जी के पास रात में बैठने वाले लोगों में अक्सर बहस होती थी कि रूस और अमेरिका में कौन आगे है, कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन हमारा सच्चा दोस्त है।
मेरी मां भी तब जीवित थीं, कैंसर में उनकी श्वासनली नहीं गली थी और तब तक `नेलकटर´ कहानी लिखने की यंत्रणापूर्ण कल्पना मैं कर भी नहीं सकता था। मेरी मां और नेहरू जी की मृत्यु एक ही साल -1964 में हुई थी। 27 मई को नेहरू जी और 30 दिसंबर को मां। ये दोनों घटनाएं मेरे बचपन की बहुत दुखद घटनाएं थीं। 27 मई को पिता जी ने रोते हुए कहा था कि नेहरू जी के दिमाग की नस चीन से धोखा खाने के कारण फटी थी।
मैंने नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनका एक चित्र अपने घर की दीवाल पर वाटर कलर से बनाया था। `अस्ताचल की ओर जाते चाचा नेहरू´। मां ने उस चित्र को देखा था और मुझे डांटा था कि तुमने नेहरू जी का चेहरा, जो कि इतना सुंदर था, वह क्यों नहीं बनाया? उनकी पीठ क्यों बनाई ? पिता जी बताते थे कि नेहरू जी इतने सुंदर थे कि केनेडी और देवानंद उनके सामने कुछ नहीं थे। नेहरू जी की सुंदरता पर भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की पत्नी और अमेरिका की कोई मशहूर हीरोइन (शायद मर्लिन मुनरो या शरले मक्लीन या फिर कोई और) फिदा थीं। दोनों नेहरू जी से शादी करना चाहती थीं लेकिन नेहरू जी ने कहा था – `नो……नो, आई कैन नॉट डू दिस´। फिर थोड़ा रुक कर पिताजी जोड़ते -`बिकॉज़ आयम आलरेडी मैरीड !´ मां कहतीं कि नेहरू जी की पत्नी बहुत सुंदर थीं, लेकिन नेहरू जी के बिलायत चले जाने और अंग्रेजों जैसा बन जाने से इलाहाबाद में अकेली रहते-रहते बीमार होकर मर गईं।
मैंने मोमबत्ती और सनलाइट साबुन की बटि्टयों को चाकू और ब्लेड से छील-छील कर नेहरू जी के कई बस्ट और पुतले बनाये थे। अगर आप में से किसी ने `नेहरू, अस्ताचल और खंडित स्त्रियां´ नाम की कई साल पहले लिखी गई मेरी कहानी पढ़ी हो, तो जान सकते हैं कि नेहरू जी का संबंध हमारे घर और मेरे बचपन के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक बात मैं यहां यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि इन संबंधों का राजनीति से कभी कोई संबंध नहीं था। इस सब पर मैं कभी बाद में लिखूंगा। अभी तो लौटें उस घटना की ओर, जिसका `तिब्बत´ से लेना-देना है।
जिस दिन वह घटना घटी थी, उस दिन मैं रसोई में मां की ही बनाई रोटियां और आलू परवल की सब्ज़ी, जो पिता जी को बहुत पसंद थी, खाकर हाथ-मुंह धोने पछीत (पिछवाड़े) की ओर निकला था। पछीत की तरफ ही, थोड़ी दूर, नदी बहती थी और उस दिन वह बाढ़ में उतरा रही थी। शायद जुलाई, यानी आषाढ़ का महीना रहा होगा।
मैं रसोई के पिछले दरवाज़े के पास रखे पत्थर पर खड़ा होकर हाथ-मुंह धो रहा था, जब मैंने वह देखा, जो मेरी स्मृति में किताबें के लिए गया हो गया और जो कई साल बाद `तिब्बत´ कविता लिखने का कारण बना।
उस समय मेरी उम्र, आप अनुमान लगा सकते हैं, आठ या नौ साल की रही होगी। उन दिनों मैं खूब चित्र बनाता था, कविताएं लिखता था और एक पुराने `रोली कॉर्ड´ कैमरे से 120 ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच कर उन्हें खुद ही प्रिंट करने की ओ में लगा रहता था। मेरे भाई तकनीकी के मामले में मेरे गुरु थे। आप में से जिन्होंने भी `अपराध´ और `भाई का सत्याग्रह´ कहानियां पढ़ी हैं, वे यह जानते होंगे कि पांच साल की उम्र में ही पोलियो के कारण उनका एक पांव बेजान हो चुका था। तब भी साइकिल चलाने और तैरने में उनका कोई मुकाबला नहीं था।
हमारे घर में `भारत´ नाम का अखबार इलाहाबाद से आता था और कभी-कभी `नव-भारत´ भी। पत्रिकाएं बहुत-सी आती थीं, जिन्हें कभी नये घर की परछी (बारामदे) में तो कभी घर से ज़रा-सा बाहर कटहल के पेड़ के नीचे, बेंत की आराम कुर्सी पर बैठे हुए पिता जी पढ़ते रहते थे। पिता जी को किताबें और बेंत की कुर्सियां बहुत पसंद थीं, जिन्हें वे इलाहाबाद से मंगाते थे। हमारे घर में एक ग्रामोफोन भी था, जो खराब पड़ा था। एक हैंडिल से उसमें चाभी भरने पर रिकॉर्ड घूमता था लेकिन चूंकि उसका स्प्रिंग टूटा हुआ था और साउंड बॉक्स भी जंग खाकर बेकार हो चुका था इसलिए वह ग्रामोफोन अटारी (दुछत्ती) के स्टोर रूम में रख दिया गया था। रेडियो आ चुका था इसलिए उसे हमारे घर ने त्याग दिया था।
टेक्नॉलॉजी के साथ हमेशा यही होता है। एक समय का `क्रेज़´ देखते ही देखते कबाड़खाने का सामान बन जाता है। अपने गौरवशाली अतीत पर ऐंठता और जंग खाता हुआ। लेकिन यह बात मनुष्यों पर भी लागू होती हैं।
मैं और मेरे भाई दोनों ऐसी त्यागी जा चुकी पुरानी-चीज़ों को दुबारा जीवित और ठीक करने में दिन रात लगे रहते थे। ग्रामोफोन में जो डिस्क लगता था, उसे शहरी लोग `रिकॉर्ड´ कहते थे और गांव के लोग `तवा´। वह चमड़े या लाख का बना होता था और देखने में उसी लोहे के तवे जैसा दिखता था, जिस पर मां रसोई में रोटियां बनाती थीं। हमारी अटारी में ऐसे अनगिनती तवे थे। अनमोल घड़ी, आह, आग, जाल, पता नहीं कितनी फिल्मों के गाने उन तवों की बारीक लकीरों में बंद थे जो सुई रखते ही जिंदा हो जाते थे।
यह सोचना भी अब कितना विचित्र लगता है कि पलाश या छिउला के पेड़ में रहने वाले छोटे-छोटे लखौरी कीड़े पेड़ के तने और पत्तियों से जो गाद के रवे इकट्ठी करते थे, उसी लाख से ये रिकॉर्ड बनते थे जिसकी बारीक लकीरों पर सुई के घूमते ही -`मेरा सुंदर सपना बीत …..गया ´ या `आवाज़ दे कहां है, दुनिया मेरी जवां हैं….´ जैसे गाने निकलने लगते थे। क्या यह कौतुक किसी जैव-यांत्रिकी, यानी छिउले के नन्हें-नन्हें कीड़ों और जर्मनी से लेकर कलकत्ता तक फैलीं रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनियों की मशीनों के तालमेल का अनोखा जादू नहीं था?
इसीलिए मैं कभी भी, आज तक किसी नयी से नयी प्रविधि या टेक्नॉलाजी को वैसा अ-मानवीय और अ-प्राकृतिक नहीं मान पाता, जैसा लोग अक्सर मानते हैं।वह तो प्रविधि का इस्तेमाल हैं, जो यह सब तय करता हैं।
3.
मैंने और मेरे भाई ने उस छोटे से गांव में, जहां तब तक बिजली नहीं आई थी, पुल और सड़क नहीं बनी थी, जहां महेश सिंह के गोसार में से गायों-भैंसों के निकल जाने के बाद, वहीं टाट पट्टी बिछा कर हमारा स्कूल चलता था, जहां छुई मिट्टी की दवात, सरकंडे और करील की कलम और काठ की पाटी में हम वर्णमाला लिखते-पढ़ते थे, लेकिन ऐसा गांव, जहां रेडियो आ चुका था, अखबार और तमाम पत्रिकाएं आने लगीं थीं, वहां हमने कई तकनीकें विकसित कीं। मार्क्वेज़ के `वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड´ के कस्बानुमा गांव मकांदो से अलग और भिन्न हमारा गांव नहीं था। मकांदो में किये जा रहे वैज्ञानिक-तकनीकी आविष्कारों से कम रोमांचक हमारे बचपन की उपलब्धियां नहीं थीं।
बैटरी और चुंबक और टिन की पट्टी से बार-बार जलने-बुझने वाला बल्ब, तांबे के तारों को मोम में डुबाकर, इंसुलेट करके और आर्मेचर बाइंडिंग करके घूमने वाली छोटी -सी पंखी, जिसे देख कर मां हैरत में पड़ गईं थीं, शायद थोड़ा-सा डर भी गईं थीं। पतंगी धागे के दोनों सिरों पर दो खाली डिब्बे जोड़ कर अपने घर से टिर्रा-किरपाल के घर को कनेक्ट करने वाली टेलिफोन लाइन। कागज के काले गत्ते को पिन या सुई से बारीक छेद कर, बंद कमरे की अंधेरी दीवाल पर बाहर के संसार के चलते-फिरते रंगीन उल्टे दृश्य … पेट्रोमेक्स, जिसे हमारे यहां `गैसबत्ती´ कहते थे, उसके कांच की तीन पटि्टयों के त्रिभुज बनाकर, ऊपर काला कागज़ लपेटकर, उसके अंदर रंगीन चिंदियां डाल कर बनाया गया केलाइडोस्कोप। चकमक और लोहे को रगड़कर पैदा की गयी चिनगारी और मूंज की बत्ती से बनने वाली `परमानेंट माचिस´…..और प्रिज्म ….! ….और हां, मार्क्वेज़ के मकांदों के कर्नल बुएंदी की तरह ही आतिशी शीशे और सूर्य की किरणों के फोकस और आग के अनेक खेल ….
लेकिन हमारी कुछ टेक्नॉलॉजियां खासी क्रूर और निर्मम भी हुआ करती थीं, जैसे पतंगों या बड़ी तितलियों को पकड़ कर उनकी पूंछ में धागा बांध कर कागज की चिंदी या माचिस का खोखा लगा देना, काले गुबरैलों की कमर में खाली गत्ते के डिब्बों की `ट्रॉली´ जोड़ देना और फिर कंकड़ों को उसमें भर कर लोड करना और फिर अपने इस ज़िंदा ट्रक की ताकत देखना। आज सोच कर लगता है, गुबरैले कीड़े को कितनी तकलीफ होती रही होगी। …..और स्कूल जाते वक्त, तालाब के पास की गड़ही को पार करते वक्त अक्सर टांगों में चिपक जाने वाली खून-चूस जोंकों को चुटकी भर नमक डाल कर काठ के एक फट्टे के दोनों सिरों पर कील ठोंक कर जोंक को तान देना और फिर उसे एकतारे की तरह बजाना ….साँप को सिर के पास से …. गर्दन पकड़ कर पत्थर पर रगड़ना , जो हमने बंदरों से सीखा था , या उसकी पूंछ पकड़ कर उसे घुमाते हुए पेड़ के तने पर बार बार पटकना (मैं इस सब पर कभी विस्तार से लिखूंगा, और उन जंगली जानवरों के बच्चों के बारे में भी, जिन्हें हमने उन दिनों पाला। कई बार लगता हैं कि पिछडे आदिवासी समाजों में ऐसी कितनी निर्ममताएं होती है….अन्य प्राणियों के प्रति हिंसाओँ से भरी, लेकिन जब आप अपने आज के विकसित और प्रविधियों से आधुनिक हो चुके समाजों द्वारा किए गए संहार और युद्ध और पर्यावरण तथा मनुष्यों के विनाश की व्यापकता को देखते है तो क्या ये पुरानी हिंसा बच्चों का खेल नहीं लगती?
तो ऐसा ही कुछ समय था, जब हमने अपने गांव में पहली बार तिब्बत से आये हुए `लामाओं´ को देखा। उनके परिवारों को देखा। पिता जी ने बताया कि `लामाओं´ के गांव तिब्बत पर चीन ने हमला कर दिया है और वे भाग कर हमारे यहां आ गये हैं। वे लोग सरगुजा के पहाड़ पर रहेंगे, जहां ‘पहाड़ी कोरबा’ और ‘ओरांव’ लामा लोग रहते हैं। उस समय हम हर तिब्बती को `लामा´ ही कहते थे। जिस जगह वे बसने जा रहे थे उस जगह का नाम था ‘मेनपाट’।
हमारे गांव से तीन किलोमीटर दूर अनूपपुर रेल्वे जंक्शन था। आप में से शायद किसी ने मेरे पहले कविता संग्रह `सुनो कारीगर´ में वह कविता पढ़ी हो, जिसका शीर्षक है `अनुकपुर जंक्शन ´ और जो बाबा कारंत जी को बहुत पसंद थी । यह एक छोटा-सा जंक्शन है, जहां से सरगुजा यानी अंबिकापुर की ओर जाने के लिए आज भी गाडी बदलनी पड़ती है। अगर आप अमरकंटक जाना चाहें जो सोन और नर्मदा, दोनों का उदगम है, तब भी आपको अनूपपुर में ही उतरना पड़ेगा। यानी अब आप जान ही गये होंगे कि मेरा गांव इन दो बड़ी नदियों के उद्गम के बिल्कुल करीब है। माफ़ करिये, सोन नदी नहीं, नद है। `मेल रीवर´। उसे पुराणों में `भद्र´ कहा गया है। देश के उन पांच पुरूष नदों में से एक जिनमें व्यास, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि आते हैं। कहते हैं सोन की तो नर्मदा से शादी होने जा रही थी। मंडप लग चुका था और फेरे पड़ने वाले थे। बस अचानक नर्मदा को गुस्सा आया और वे विवाह की गांठ तोड़ कर उल्टी दिशा में भाग गईं। वज़ह यह कि नर्मदा `कुलशीला´ थीं, यानी `ऊंची जाति´ की और सोन इसलिए `कुल-भ्रष्ट´ हो गया था, क्योंकि उसका प्रेम-प्रसंग एक नीची जाति की लड़की `जुहिला´ से चल रहा था। आप अगर विंध्य क्षेत्र के नक्षे को देखें तो पायेंगे कि `जुहिला´ भी एक नदी ही है, ज़रा छोटी और दुबली-पतली, लेकिन जो जाति बहिष्कृत अपने प्रेमी सोन से , कटनी के पास, लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर की दुर्गम-कठिन यात्रा करने के बाद, मिल जाती है। फिर दोनों बिहार में `पतित-पावनी´, `मोक्ष-दायिनी´ गंगा में समाहित हो जाते हैं। जब कि अपने `कुल-शील´ पर इतराती नर्मदा गंगा से कभी नहीं मिल पाती। वह भारत की अकेली ऐसी नदी है जो उत्तर से पश्चिम-दक्षिण की ओर, यानी उलटी दिशा में बहती है। हमारे गांव के लोग कहते हैं देखो भाग्य का खेल और ईश्वर की लीला, कुजात ठहरा दिया गया सोन जुहिला के साथ गंगा में मिलकर तर गया और अहंकारी नर्मदा गिरी जाके लंपट की गोदी में। कहते हैं कि समुद्र का देवता वरुण लंपट होता है, इंद्र और कुबेर की तरह। तमाम यक्षिणियों के साथ फ्लर्ट करने वाला।तब से कई साल बाद जब मैं आज नर्मदा के `सरदार सरोवर´ बांध वाले विवाद की ओर देखता हूं, तो लगता है सचमुच बेचारी नर्मदा कितनी अभागी थी। आज भी (धन) कुबेरों की वासना और लोभ की जंजीरों में जकड़ी हुई।क्या उसे अपनी जाति के दंभ का दण्ड मिला ?
ओह, मैं आपको कहां भटकाने लगा। दरअसल, मैं खुद ही भटक गया था।हम तो तिब्बत के शरणार्थियों की बात कर रहे थे, जिन्हें हम सब `लामा´ ही कहते थे।तो…… `लामा´ अपने परिवारों के साथ उसी अनूपपुर के प्लेटफॉर्म पर उतरते थे। अगली गाड़ी के लिए उन्हें वहां कई-कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। कई बार, खासतौर पर बरसात के दिनों में, सरगुजा की ओर जाने वाली वह अकेली गाड़ी, रास्ते में पड़ने वाली नदियों में बाढ़ आ जाने या पटरियों पर पानी भर जाने के कारण कई-कई दिनों के लिए रद्द हो जाती थी, तब `लामा´ हमारी नदी के किनारे की रेत पर आ जाते। वहीं खाते-नहाते। उन्हें वहां देखना हम बच्चों के लिए एक बिल्कुल नया दृश्य बनता। याद रखें तब तक टी वी नहीं था और सिनेमा था तो, लेकिन हमारे गाँव तक नहीं पंहुचा था॥ ..हमारे गांव और आस-पास के लोग तो ज्यादातर काले रंग के थे। मेरे कई चचेरे भाई और बहनें भी काली ही थीं। लेकिन `लामा´ लोग खूब गोरे और सुंदर होते थे। उनके बच्चे और स्त्रियां भी। बच्चे और स्त्रियां तो इतनी सुंदर होतीं, कि उन्हें देखते हमारी आंखें पलक झपकना बंद कर देतीं।
हम बच्चों को `लामा´ लोग प्यार करते थे। अपने कंधे पर लटकते गेरुआ झोले में से `लेमंचूस´ और रंगीन मीठीगोलियां देते थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए लगते। उनकी आंखें और उनका चेहरा, जब भी देखो तब धीरे-धीरे मुस्कुराता हंसता हुआ लगता। एक अजब सी शांति से भरा. …..और गेरुआ लबादा पहनने वाले, घुटे हुए सिर वाले बूढ़े लामाओं का तो जैसे पूरा शरीर ही किसी बहुत धीमी मुस्कान में डूबा हुआ लगता।
गांव वाले कहते कि ये लोग बुद्ध भगवान के पुजारी हैं। तो क्या वह बुद्ध की मुस्कान थी, जो उनकी पूरी देह और उनकी समूची उपस्थिति में दिखाई देती थी? बुद्ध की वही मुस्कान, जिसके नाम पर तब से लगभग सैंतीस साल बाद 1998 में भारत की, अपने आपको ‘धार्मिक’ कहने वाली, सरकार ने परमाणु बम बनाया और फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए पोखरण में फोड़ा ?
पिता जी ने एक बार बताया था कि `लामा´ लोगों का असली व्याकरण राहुल सांकृत्यायन ने तैयार किया था। इसीलिए लामा लोग भाषा में राहुल सांकृत्यायन को और धर्म में बुद्ध को गुरु मानते हैं। उसी तरह जैसे तमिल लोगों का व्याकरण अगत्स्य मुनि ने तैयार किया था। पता नहीं इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है पिता जी ने यही कहा था।मेरा मन उन दिनों अक्सर `लामाओं´ के साथ भाग कर सरगुजा के पहाड़ पर हमेशा के लिए चले जाने का करता था। इसके पीछे `लामाओं´ द्वारा दिये जाने वाले लेमंचूस और रंगीन मीठीगोलियों का लालच और उनके व्यक्तित्व में फैले रहस्यपूर्ण, बुद्ध की मुस्कान का चुंबक तो था ही, अपने बचपन को घेरने वाले एक भयानक डर का भी इसमें हाथ ……था।
वह डर था महेश सिंह के गोसार में चलने वाले स्कूल और उसके मुच्छड़, त्रिपुंडधारी, कसरत करने वाले पहलवान मास्टर राजमनी सिंह का, जिन्हें मैं गुस्से, भय और वितृष्णा में `राज-मटा सिंह´ कहा करता था। (`मटा´ आम और जामुन के पेड़ों में पाये जाने वाले काले, कटखने और बड़े से खतरनाक चींटे का नाम होता है।)
राज़मटा पहाड़ा और दूनियां ठीक से न रटने वाले लड़कों को सिरकिन या सनई के सोंटे से मारते थे, कनपटी के बाल चिकोटी में भरकर खींचते थे या बड़ेरी की बल्ली में हाथ के पंजों की कैंची बनवा कर उन्हें घंटों के लिए लटकता छोड़कर ताश खेलने किसी गंजेडी-भंगेडी के घर चले जाते थे। उस समय तक `क्रुएलिटि अगेंस्ट चिल्ड्रेन´ वाला कानून शायद नहीं बना था, वर्ना कोई नहीं तो मैं ज़रूर उन पर मुकदमा दर्ज करता। राक्षस जैसे त्रिपुंडधारी राजमनी सिंह उर्फ़ राजमटा सिंह की तुलना में तिब्बत से आये हुए `लामा´ हम बच्चों के लिए दया, वत्सलता, करुणा और प्रेम से भरे देवदूत जैसे लगते थे। मैंने कई बार उनके साथ अपना घर और गांव छोड़कर भाग जाने की योजना बनाई, लेकिन पता नही क्यों, उस पर कभी अमल नहीं कर पाया।
बहुत बाद में मैंने बोर्खेज़ की या शायद किसी दूसरे लातीनी अमेरिकी लेखक की वह कहानी पढ़ी, जिसमें अमेरिका का किसी शहर का एक व्यक्ति लगातार अपने सपने में बर्फ से ढंके पहाड़, उसकी तलहटी पर बसी बस्तियों और रास्ते में चलने वाले लोगों के काफिले का दृश्य वर्षों से देखता रहता है। फिर उसे लगने लगता है कि जिस शहर में वह रह रहा है, वहां वह कोई अजनबी या आप्रवासी है। वह तो यहाँ का …. इस शहर का है ही नहीं। फिर उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे यानी अपना पूरा परिवार कुछ पराया-सा लगने लगता है।
……और तब, बेचैन होकर, अधेड़ से भी अधिक की उम्र में वह उस जगह की खोज में निकल पड़ता है, जिसके दृश्य वह बचपन से अपने सपने में देखता आया है। आखिर सारी दुनिया भटकने के बाद एक दिन वह तिब्बत पहुंचता है और स्तब्ध रह जाता है। ठीक वैसे ही बर्फ से ढंके पहाड़, ठीक वैसी ही बस्ती, उसी तरह के घर। aur…. लोगों का एक झुंड भी ठीक उसी काफिले जैसा जो वह हमेशा अपने स्वप्न में देखता आया था।तभी उस काफिले में से एक औरत उसे पहचान लेती है और दो छोटे-छोटे बच्चों के साथ तिब्बती में उसका कोई नाम पुकारती हुई बदहवास उसकी ओर दौड़ती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। दोनों बच्चे भी उससे चिपक जाते हैं। इस तरह कई वर्षों तक किसी पराये देश के पराये शहर में पराये लोगों के बीच रहे आने वाला वह व्यक्ति आखिरकार उस दिन पहचान लिया जाता है। उसे अपने असली नाम का पता चलता है और हमेशा के लिए वह अपने परिवार के साथ रहने लगता हैं ।
4.
वह आषाढ़ का महीना रहा होगा।
कुछ दिन पहले लगातार हुई बारिश थम चुकी थी लेकिन हवा और मिट्टी में भारीपन और नमी छोड़ गई थी। शायद आषाढ़ की पहली बारिश थी। वैशाख-जेठ की तीखी धूप में महीनों से जली-झुलसी धरती पर जब वर्षा की पहली बूंदें गिरती हैं तो धरती का अब तक का ताप बुझता है। जैसे गर्म तवे पर पानी के छींटे मार दिये गये हों। और फिर मिट्टी की सोंधी गंध चारों ओर भाप बनकर बिखर जाती है। हम गहरी सांसें खींचते हैं और पृथ्वी का सोंधापन हमारे फेफड़ों में भर जाता है। समूची देह में सिहरन दौड़ती है और हम जान जाते हैं कि बरसात आ गई। कहते हैं कि महान चित्रकार पिकासो, ऐसी पहली बारिश में, बादलों को घिरते देख कर, अपनी छत पर चढ़ जाता था और नाचने लगता था। वर्षा का आना संसार की और हमारे जीवन की हरबार एक अपूर्व और महान घटना होती है। मैंने अब तक बहुत खोजा लेकिन शायद अभी तक किसी परफ्यूम कंपनी ने कोई ऐसा सेंट नहीं बनाया है, जो आषाढ़ की पहली वर्षा के साथ धरती की देह से उठती मिट्टी की गंध की स्मृति जगा दे।
ऐसी ही वर्षा के बाद, गरमी के दौरान धरती के भीतर, अपने बिलों में अब तक छिपी असंख्य चींटियां अचानक बाहर निकल आती हैं और शाम को आकाश में उड़ने लगती हैं। उनके पंख उग जाते हैं। झुंड की झुंड वे बाहर आकाश की ओर उड़ती हुई आंगन के ऊपर मंडराने लगती हैं। लेकिन उनके पंख इतने क्षणभंगुर होते हैं, कि बस हवा के एक हलके झोंके या उनकी किसी छोटी उमंग भरी हरकत से तिड़क कर टूट जाते हैं और फिर वे किसी कीड़े की तरह, अपने असली रूप में, किसी शरन्य की खोज में धरती पर गिर कर असहाय रेंगने-भटकने लगती हैं। हम इन चींटियों को पतंगों के नाम से, उनके जीवन के कुछ पलों में जानते हैं। जहां कहीं उजाला दिखे, कोई बिजली का बल्ब, लालटेन या कंदील, ये पतंगे झुण्ड के झुण्ड वहां टूट पड़ते हैं। आषाढ़ की पहली बारिश की शीतलता और कंदील या बल्ब की जिस रोशनी ने उनके जीवन में भविष्य की नयी आशाएं जगाईं थीं, कुछ ही देर के बाद उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है।हर सुबह हम अपनी देह पर उगे निर्बल पंखों के साथ आकाश की ओर उड़ती और किसी उजाले को देख कर एक साथ किसी सामूहिक आशावाद में टूट पड़ने वाली इन चींटियों के अनगिनत शव झाड़ू लगाकर बाहर फेंक देते हैं। उनका वह कुछ पलों के कौतुक और उल्लास से भरा जीवन, सुबह तक कचड़े के ढेर में तब्दील हो चुका होता है। पंख लगी चींटियों के जीवन का यह छोटा-सा अध्याय, उनकी सभ्यता के इतिहास में किसी `यूटोपिया´ के बनने और फिर उसके टूटने का मार्मिक अध्याय होता है। ठीक मनुष्यों की सभ्यता के इतिहास के किसी खण्ड की तरह।
तो, वह ऐसी ही कोई रात थी। आषाढ़ की पहली वर्षा के बाद की कोई रात।
उस रात नदी उतरा रही थी। अगर एक-दो दिन के भीतर फिर पानी बरस गया तो बाढ़ आ जाएगी और नदी हमारी रसोई के पीछे तक बहने लगेगी। रात में घर में, हर ओर, नदी की धार के साथ बह कर आने वाले सांप, गोजर, कनखजूरे और कछुए टहलने लगेंगे। मेंढकों का भी तो यही समय होता है। धरती की दरारों में महीनों से समाधि लगाए या `हाइबरनेट´ करते ये तरह-तरह के मेंढक भी पहली बरसात के साथ ही बाहर निकल आते हैं और रात भर हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। दादुर-धुन। एक अजब सा संगीत। झींगुरों के गिटार, पहरुए पक्षी की टनक, किसी रात्रि-पक्षी की दूर तक जाती मेंडोलिन या बांसुरी की संगत में लगातार चलता संगीत। उस रात आलू और परवल की सब्जी बनी थी। पिताजी की पसंद। मैं हमेशा की तरह कुछ बनाने या पढ़ने में लगा था। पंख वाली चींटियों पर कुढ़ता-भुनभुनाता हुआ, जो बार-बार किताब के पन्नों पर, मुझ पर या मेरी लालटेन पर आकर गिरती थीं। रात में खाना खाते हुए भी बहुत सतर्क रहना होता है। एक बार ऐसे ही, लालटेन की धुंधली रोषनी में, रात में हमारे घर कोई खाना खा रहा था और जब उसने थाली में रखे अचार को उठाना चाहा तो अचार एक अजीब सा शोर करता हुआ उड़ गया। हम जूतों के भीतर रात में पांव डालते डरते हैं। कहीं कोई मेढक, सांप या कोई और जंतु छुपा न बैठा हो। एक बार फूफा जी ने आधी रात अपने सिरहाने रखी टॉर्च उठानी चाही तो वह अजीब सी आवाज़ निकालता भाग गया। पता नहीं बारिश से बचने कोई नेवला या ऊदबिलाव उनके तकिये के पास, जहां टॉर्च थी, छिपा बैठा था।
मैं हमेषा मां के साथ खाता था। मां सब लोगों के खाना खा लेने के बाद बचा-खुचा अपने लिए लेकर बैठती थीं। हां, मेरे लिए एक कटोरी सब्जी वह हमेशा अलग से रख लेती थीं।खाना खाने के बाद हाथ-मुंह धोने और कुल्ला करने के लिए जब मैंने रसोई का पिछला दरवाज़ा खोला तो नदी के शोर, िझलमिलाते अंधकार और रात की असंख्य आवाज़ों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अगर आपका घर किसी नदी के तट पर है तो आप जान सकते हैं कि यह सब कितना अजब और सम्मोहक होता है। चारों ओर से घेर कर आपको अपने भीतर खींचकर डुबा लेने वाला। लेकिन हमेशा भय और दुस्वप्न के एक साथ-साथ चलने वाले अनुभव के साथ। कितना विरल होता है बाढ़ में उतराती नदी के पास रात में अकेले खड़े होना। किसी इंद्रजाल में बिंधे हुए। अंदर-अंदर भय से सिहरते हुए। फिर भी वहां से हटने से इनकार करते हुए। और तभी मेरी निगाह अंधेरे में, बाढ़ में उतराती नदी के दूसरे पार की ओर गई। वहां पहले, वर्षों पहले, एक मंदिर हुआ करता था। वहां बुद्ध की एक मूर्ति थी। तथागत। लेकिन उन्हें चंदन-टीका लगाकर दूसरे देवी-देवताओं के साथ रख दिया गया था। कहते थे कि वे सिद्ध-भगवान हैं। इस पूरे इलाके में अब भी बुद्ध की बहुत-सी खंडित, टूटी-फूटी प्रतिमाएं यहां-वहां मिलती हैं। उस इलाके में जब कोई कुआं खोदता है या अपने नये घर की नींव, तो ऐसी मूर्तियों का मिलना एक सामान्य सी बात है। कलिंग का वह क्षेत्र, जहां अतिक्रमणकारी सम्राट् अशोक की सेना ने निहत्थे, गरीब, शांत लोगों के अहिंसक प्रतिरोध के उत्तर में भयावह जनसंहार किया था और फिर जहां से पूरब-दक्षिण, राजगीर-उदयगीर तक पहुंचते-पहुंचते उसे स्वयं अपनी हिंसा से ग्लानि हुई थी और वह बौद्ध हो गया था, उस उत्कल-कलिंग क्षेत्र का सीमांत विंध्य पर्वत की इसी श्रृंखला के पास है। मैं कई बार सोचने लगता हूं कि बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़कर जगह-जगह मंदिर खड़ी कर देने वाले लोग आखिर कौन थे? ब्राह्मण ? प्राचीन इतिहास के हिंदू तालिबान ? या कोई और ? उस रात बाढ़ में उफनती नदी के दूसरे पार आग की लाल, पीली, नीली लपटें किसी क्रम में टहल रहीं थीं। जैसे कुछ लोग अपने हाथों में नन्हीं-नन्हीं मशालें लिए एक वृत्त में घूम रहे हों। हमारे गांव में माना जाता है कि रात में चितावर की लकड़ी इसी तरह जलती है। और अगर उसे नदी के पानी में डुबा दिया जाय तो वह सांप बन जाता है। लेकिन चितावर को पकड़ पाना आसान नहीं होता। अगर कोई उसे पकड़ ले तो चितावर पारस पत्थर की तरह काम करता है। यानी जिस भी धातु को चितावर की लकड़ी से छू दोगे, वह सोना बन जाएगा।
बचपन में हम में से बहुतों की फैंटेसी में चितावर को पाना उसी तरह उपस्थित था जैसे बहुत पहले अरब, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के अलकीमियागरों (अलकेमिस्ट) की फैंटेसी में किसी ऐसे रासायनिक फार्मूले की खोज, जो किसी भी धातु या पदार्थ को सोने में बदल दे। क्योंकि हर पदार्थ (मैटर) तो असल में एक ही होता है, उसकी आंतरिक संरचना ही उसे दूसरों से भिन्न बना डालती है। पदार्थ की उसी आंतरिक संरचना को बदलने वाले सूत्र को खोज निकालने के शताब्दियों तक चलने वाले प्रयत्नों के बीच ही उस विज्ञान का जन्म हुआ जिसे हम `केमिस्ट्री´ के नाम से आज जानते हैं।
क्या हमारे `मकांदो´ जैसे गांव की चितावर वाली अवधारणा के पीछे भी कोई ऐसा ही विज्ञान था, जिसका आविष्कार आज तक नहीं हो पाया ? या वह सब एक सामुदायिक लोक-विश्वास था? एक पूर्व-आधुनिक मिथ्याचेतना? कोई अंधविश्वास ?बाद में, जब मैं आठवीं दर्जे में पढ़ता था, तब केमिस्ट्री के हमारे अध्यापक वर्मा जी, जो काले रंग के थे, चेहरे में चेचक के दाग थे और जिनकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं, ने बताया था कि रात में मरे हुए जानवरों और मनुष्यों की हडि्डयों का फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज़ हो कर इसी तरह जलता है और लोग डर जाते हैं।
5.
आषाढ़ महीने की उस रात, नदी के पार, दूसरे तट पर, रहस्यपूर्ण आग की धुंधली-झिलमिलाती नन्हीं-नन्हीं लपटें टहल रही थीं। हमारे बीच की दूरी में बाढ़ में उतराती नदी की तेज धार और उसका हहराता हुआ शोर था। मैंने मां को पुकारा, `मम्मा, देखो नदी के पार चितावर जल रहा है।´
मां उठ कर आयीं। उन्होंने गौर से देखा और कहा, `सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आदमियों की? ´
मैंने अपने कान उधर लगाए। धीरे-धीरे बाढ़ के शोर और रात की दूसरी ध्वनियों में कहीं डूबी हुईं मनुष्यों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कुछ ही पलों बाद पता लगने लगा कि इसमें संगीत जैसा कुछ है। कुछ ध्वनियों की बार-बार आवृत्ति।
मां रसोई के अंदर जा चुकी थीं और मैं वहीं खड़ा था चुपचाप। उन रंगीन धुंधली रोशनियों को घूमते-टहलते देखता और वहां से उठने वाली आवाज़ों को सुनने की चेष्टा करता हुआ।
कुछ देर के बाद, उन सुदूर रोशनी के वृत्तों में से मनुष्यों के आकार झलकने लगे। अस्पष्ट, अस्थिर लेकिन निश्चित जीवित मानव आकृतियां। कुछ-कुछ उस जैसा, जैसा मैंने एक बार बचपन में रेडियो के भीतर देखा था, लेकिन जिसे बाद में बड़े और वयस्क लोगों ने मेरा सपना कह कर टाल दिया था। तभी से मैंने यह तय कर लिया था कि भविष्य में अपने साथ घटने वाली ऐसी कोई घटना दूसरों को नहीं बताऊंगा, जिस पर उनको विश्वास नहीं होगा। अगर आप मेरी एक बहुत पहले लिखी गई कहानी `डिबिया´ पढ़ेंगे, तो आपको मेरे इस निर्णय के बारे में पता चल जाएगा।
उस रात भी मैं यही सोच रहा था। मेरी आंखें साफ देखने लगीं थीं कि नदी के उस पार, नन्हीं नन्हीं कंदीलें लिए और किसी लय में लगातार कुछ बोलती-दोहराती हुई वे आकृतियां किसी और की नहीं, लामाओं की ही हैं। पिताजी ने बताया था कि उनके गांव तिब्बत पर चीन ने हमला कर दिया है और वे अपना घरबार, सब कुछ वहां छोड़कर, भाग कर हमारे देश में चले आये हैं। अब वे सरगुजा के उस पहाड़ पर रहेंगे, मेनपाट में, जहां `पहाड़ी कोरबा´ और `ओरांव´ रहते हैं। तो, इसका मतलब, नदी के पार आग का वह खेल, चितावर या मृत पशुओं और मनुष्यों की हडि्डयों में उपस्थित फास्फोरस के ऑक्सीजन में जलने से पैदा होने वाला दृश्य नहीं था, वह कोई विभ्रम या स्वप्न भी नहीं था, बल्कि वहां एक असली और वास्तविक घटना घट रही थी।मैं पता नहीं कितनी देर तक वहां, रसोई की पछीत में, बाढ़ में उफनते सोन के किनारे, अंधेरे के पार यह दृश्य देखते और अपने कान वहां से उठने वाले शब्दों को पकड़ने में लगाए, ध्यानमग्न, चुपचाप खड़ा रहा।
मां ने खाना खा लिया था। बचा-खुचा खाना आलमारी में रख दिया था। बरतन समेट दिये थे। इसके बाद वह बाहर आयीं और मुझसे पूछा -`कुछ पता चला? कौन लोग हैं ?´उत्तर में मैंने सिर्फ इतना कहा कि `मुझे तो लामा लग रहे हैं।´ और चुप हो गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि उस रात मुझे स्पष्ट लगा था, कि जो संगीत जैसी आवाज़ वहां से आ रही थी, वह कोई गाना नहीं, कोई ऐसा मंत्र था, जिसमें कोई दारुण विलाप भी सम्मिलित था। जैसे कोई समूची आत्मा, देह और हृदय के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ रोते हुए शोकगीत में कोई प्रार्थना करे। अगली सुबह नदी में और ज्यादा बाढ़ आ चुकी थी। इतनी बाढ़ में पेड़ के तने को खोखला करके बनाया गया हमारे गांव का डोंगा, बांस की बल्ली से ठेलकर चलाया नहीं जा सकता। बल्ली तो नदी की धार की थाह ही नहीं पाएगी।
सुबह मैंने फिर रसोई की पछीत से जाकर उस जगह को देखा, जहां रात में यह घटना घटी थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जगह सुनसान थी लेकिन उस तक बाढ के कारण पहुंचा नहीं जा सकता था।
कई दिनों के बाद गांव के लोगों ने बताया कि अनूपपुर से सरगुजा की ओर जाने वाली रेलगाड़ी पांच-छह दिनों के लिए रद्द हो गई थी और वहां स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी बीमार तिब्बती शरणार्थी की मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि उस रात लामा लोग उसी अपने साथी का अंतिम संस्कार करने नदी के तट पर आये थे।
मैं आज तक नहीं जानता कि लामा मृतक का अंतिम संस्कार किस तरह करते हैं। उसे दफनाते हैं, जलाते हैं, पारसियों की तरह कहीं शव को छोड़ देते हैं या नदी में बहा देते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगता है कि अपने घर और देश से हज़ारों मील दूर, जब कोई तिब्बती किसी और पराये देश में मरता है, तो अंतिम संस्कार के समय लामा जो प्रार्थना करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, तो वह असल में, ध्यान से सुनो तो, और कुछ नहीं, एक विलाप जैसा कुछ होता है। बहुत मार्मिक। भीतर तक बेध डालने वाला। व्याकुल कर डालने वाला।
और अगर कोई सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, उसके भीतर मनुष्य जैसा कुछ बचा रह गया है तो उसकी स्मृति का पीछा यह विलाप कभी नहीं छोड़ता। मेरी स्मृति में तो यह दृश्य इसलिए भी अमिट रहा आया क्योंकि मां की मृत्यु के बाद ही मैंने गांव का वह घर छोड़ दिया था और फिर पिताजी की मृत्यु के बाद तो वहां लौटने का विकल्प ही नहीं था।
इस घटना के वर्षों बाद, 1975-76 में, जब मैं जे एन यू में शोधछात्र था, जहां बाद में कुछ समय के लिए अध्यापक भी हुआ, तब मैंने वहां की लाइब्रेरी में विश्वप्रसिद्ध कथाकार असिमोव की एक कहानी पढ़ी। वह कहानी मुझे कभी नहीं भूलती। उस कहानी का सारांश, स्मृति के सहारे आपको बता रहा हूं।
अमेरिका के दो भाषावैज्ञानिकको कहीं से पता चलता है कि ल्हासा के प्राचीन बौद्धमठ में तिब्बत की प्राचीन लिपि में लिखी गई एक ऐसी पांडुलिपि है, जिसमें स्रिष्टि के निर्माण और विनाश का सारा रहस्य बंद है। लेकिन समस्या यह है कि `मोहनजो दाड़ो´ की लिपि की तरह ही, उस अज्ञात लिपि को भी अभी तक संसार का कोई भाषावैज्ञानिक `डिकोड´ नहीं कर पाया है। पश्चिम और अमेरिका ही नहीं, कई दूसरे देशों के भाषा वैज्ञानिक चोरी छुपे उस सैकड़ों पृष्ठों वाली पांडुलिपि के कुछ पन्नों की नकल अपने साथ ले गये हैं और भरपूर मेहनत की है, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। उस मठ के लामाओं के अनुसार इस अज्ञात लिपि को किसी अन्य भाषा में समझना या बदलना वर्जित है। उनकी मान्यता के अनुसार, जिस दिन कोई मनुष्य इस पांडुलिपि को पूरी तरह `डिकोड´ कर देगा, यह समूची स्रिष्टि उसी पल नष्ट हो जाएगी।
अमेरिका के वे दोनों वैज्ञानिक दिन रात उस अज्ञात लिपि का अध्ययन करने में लगा देते हैं। कई वर्षों के बाद वे दोनों उस लिपि को `डिकोड´ करने में सफल हो जाते हैं और फिर एक छोटा `टू-सीटर´ हवाई जहाज लेकर तिब्बत पहुंचते हैं और वहां के लामा से उस रहस्यपूर्ण पांडुलिपि को देखने और पढ़ने की इच्छा प्रकट करते हैं।
लामा उन्हें मठ में, उस पांडुलिपि को देखने और पढ़ने की अनुमति तो देता है लेकिन कड़े शब्दों में उन्हें चेतावनी भी देता है कि वे उसे `डिकोड´ करने और दूसरी, आज की किसी जीवित भाषा में बदलने और व्याख्यायित करने की कोशिश न करें, वर्ना यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी।
दोनों भाषावैज्ञानिक रोज़ उस मठ के भीतर जाकर, उस प्राचीन पांडुलिपि को चोरी से `डिकोड´ करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि लामाओं की यह मान्यता किसी पूर्व-आधुनिक, पूर्व-वैज्ञानिक समय में जन्म लेने वाले अंधविश्वास से अधिक और कुछ नहीं है।
लगभग दो महीने की दिन-रात की कठिन मेहनत के बाद वे पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ तक पहुंच जाते हैं। फिर अंतिम पैरा तक। और फिर आखीर में पांडुलिपि का सिर्फ अंतिम वाक्य बचता है।
इस जगह दोनों को गहरा असमंजस होता है। एक दुविधा, जिसमें एक तरह का भय भी शामिल है। कहीं लामाओं की वह प्राचीन मान्यता सच हुई तो ? अंत में वे दोनों उस अंतिम वाक्य को भी `डिकोड´ करने का निर्णय लेते हैं और कुछ ही पलों में उसे पूरा कर डालते हैं।
वे दोनों ल्हासा के उस प्राचीन बौद्ध मठ से बाहर निकलते हैं। बाहर बर्फ उसी तरह है, वैसी ही शांति, उसी तरह बस्तियां और चहल-पहल। कहीं कुछ नहीं बदला। दोनों को हंसी आती है।
उसी रात वे लामा से विदा लेकर अमेरिका के लिए उड़ जाते हैं। इतने वर्षों तक अज्ञात और अबूझ रही आयी एक प्राचीन लिपि को विखंडित कर डालने और अब उसे आज की आधुनिक भाषा में ले जाने का गर्व एक तरफ और तिब्बतियों के पुराने अंधविश्वास के गलत सिद्ध हो जाने की प्रसन्नता दूसरी तरफ। दोनों नशे में हैं और तिब्बतियों का पेय `छंग´ पी रहे हैं।
और तभी उनके एयरक्राफ्ट का पायलट डरा हुआ कहता है :` सर, उधर तो देखिये, सामने! ये क्या हो रहा है?´ दोनों भाषावैज्ञानिक स्तब्ध रह जाते हैं।वे सामने, अंतरिक्ष की ओर देखते हैं,….. वहां सौरमंडल के चमकते हुए सारे नक्षत्र एक-एक कर बुझ रहे हैं।
अगर आपने मेरी कहानी `वारेन हेस्टिंग्स का सांड´ पढ़ी है तो उसके नायक सांड को अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसे तिब्बत के एक बूढ़े लामा ने सैम्युएल टर्नर को दिया था, और जो दरअसल एक याक था। इस कहानी की अंतिम पंक्तियां एक बार फिर पढ़िये।
… वैसे तिब्बत का वह बूढ़ा लामा दिल्ली के `मजनूं का टीला´ नामक इलाके में शरणार्थी के रूप में अब भी रहता है। उसे सैम्युएल टर्नर की याद है, जिससे वह लगभग सवा दो सौ साल पहले मिला था।
रहस्यभरी झुर्रियों में मुस्कुराता हुआ वह लामा कहता है, “वह सांड अभी मरा नहीं है।”
(गद्य और पद्य दोनों का अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.)
a
dbhut shilp aur bhasha ki takat udaiprakash ki kaninion ko shresthta pradan kartee hei.tibbtion ke prati pratibadh
rachnakar ki gahre judi samvedna,unke sangharsh ke prati apni drashti in rachnaon main shreshtha kalatmak roop main hai.udaiprakashji ka padhya “suno karigar”,”abutar-kabutar”,tiriksh peeli chattri wali ladki aur ye kavita apni peedi ke chuninda rachna karo main khada karti hein.umeed hai hame aise hi enrich karte rahenge.
वस्तुतः तिब्बत कविता के पीछे छिपे इन संस्मरणों को पढ़ने से उदय प्रकाश की किसी लंबी कहानी को पढ़ने जैसा आस्वाद ही मिलता है। बचपन की स्मृतियों को इन संस्मरणों में वे बिलकुल साफ, चमकदार, नीले और पारदर्शी आसमान की तरह देख पा रहे हैं। उन कारुणिक दृश्यों को वैसा ही दर्ज कर रहे हैं जैसा अपनी कहानियों में दर्ज करते रहे हैं, कल्पना के बारीक और मुलायम धागों से बुनते हुए, जो गहरे दुःख और पीड़ा के रंग से रंगे हुए हैं। एक कवि अपनी कविता लिखने के लिए दूसरों के दुःख में किस कदर घुलमिल जाकर किस कलात्मक ढंग से उस अनुभव को अभिव्यक्त करता है जो बरसों बरस उसके जेहन में अमिट बने रहे हैं, यह उसकी एक मिसाल है।
यह कविता न केवल तिब्बतियों पर चीन के अत्याचारों को बहुत ही कारूणिक ढंग से औऱ लगभग उतनी ही मासूमियत से बताती-जताती है जितना मासूमियत भरा लामाअों का जीवन होता है। दूसरी तरफ यह इसी अकेलेपन, पीड़ा और मासूमियत से वह ताकत हासिल करती है जिससे इन अत्याचारों के खिलाफ बिना शोर किए एक प्रतिरोध भी पैदा होता है। बीस साल पहले लिखी गई एक छोटी सी कविता आज कितनी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है यह हम उन खबरों के आईने में भी देख सकते हैं जब चीन में अोलिंपिक के मद्देनजर तिब्बतियों पर चीनी सरकार फिर से अत्याचार करने पर उतर आई है। जाहिर है यह सस्मरण हमें एक बार फिर उस पीडा और अवसाद के जल में झांकने का मौका देता है जो लगातार अनदेखा किया जाता रहा है। यह संस्मरण कल्पना औऱ यथार्थ, करुणा औऱ अवसाद, बचपन और घर, बालमन औऱ आसपास के आश्चर्यलोक का ऐसा विशाल दृश्य चित्रित करता है कि हम उदय प्रकाश की रचनात्मकता के प्रति गहरे आदर से भर जाते हैं। रवींद्र व्यास, इंदौर
Aadarniya Uday Prakash ji ko jab bhi parhta hun, unki rachnaon se phir se pyar ho jata hai.Ve hamare yug ke sarvashreshtha sahityakar hain.Unka lekhan adbhut hai.Tibet ki peera ko unka yeh blog sashakt dhang se swar deta hai.Uday Prakash ji ko haardik badhai.Ishwar unhe deerghayu banaye.Aise mahan sahityakar hamare beech sadiyon mein aate hain.
________________________Sushant Supriye.
Uday Prakashji, Jise Sitapur Me ‘Donga’ Kahte Hain, Use Orissa Me ‘Danga’ kahte hain, yaani, deshi naav. Kabhi hairani hoti hai ki is bharat me logon ke shabd bhasha aur kshetra ki paridhiyon ko paar karte huye kahan se kahan pahunch jaate hain. Kahin aisa to nahin, ki Orissa ka koi vyakti Sitapur ya uske aaspaas pahuncha ho, ya udhar ko koi idhar aaya ho.
saans hi nhi le paai.. poora padh gai.. nishabd hoon..kuchh der baad phir padhungi.. tabhi kuchh kah paaoongi.. uday ji ki rachna par kuchh bhi kahna mere jaise sadahran paathak ke liye soory ko diya dikhana hi hoga.. sadhuvaad.
I READ MANY STORIES OF HIS BOOK IN WHICH I MOST LIKE “DELHI KI DIWAR”.
THE STORY WAS THE BLAST ON THE CURREPT PEOPLE OF THE INDIA.
I PERSONLY KNEW AFTER WORKED WITH HIM. HE IS NOT ONLY A GREAT WRITER BUT ALSO A HONEST AND POLITE PERSON IN HIS LIFE.